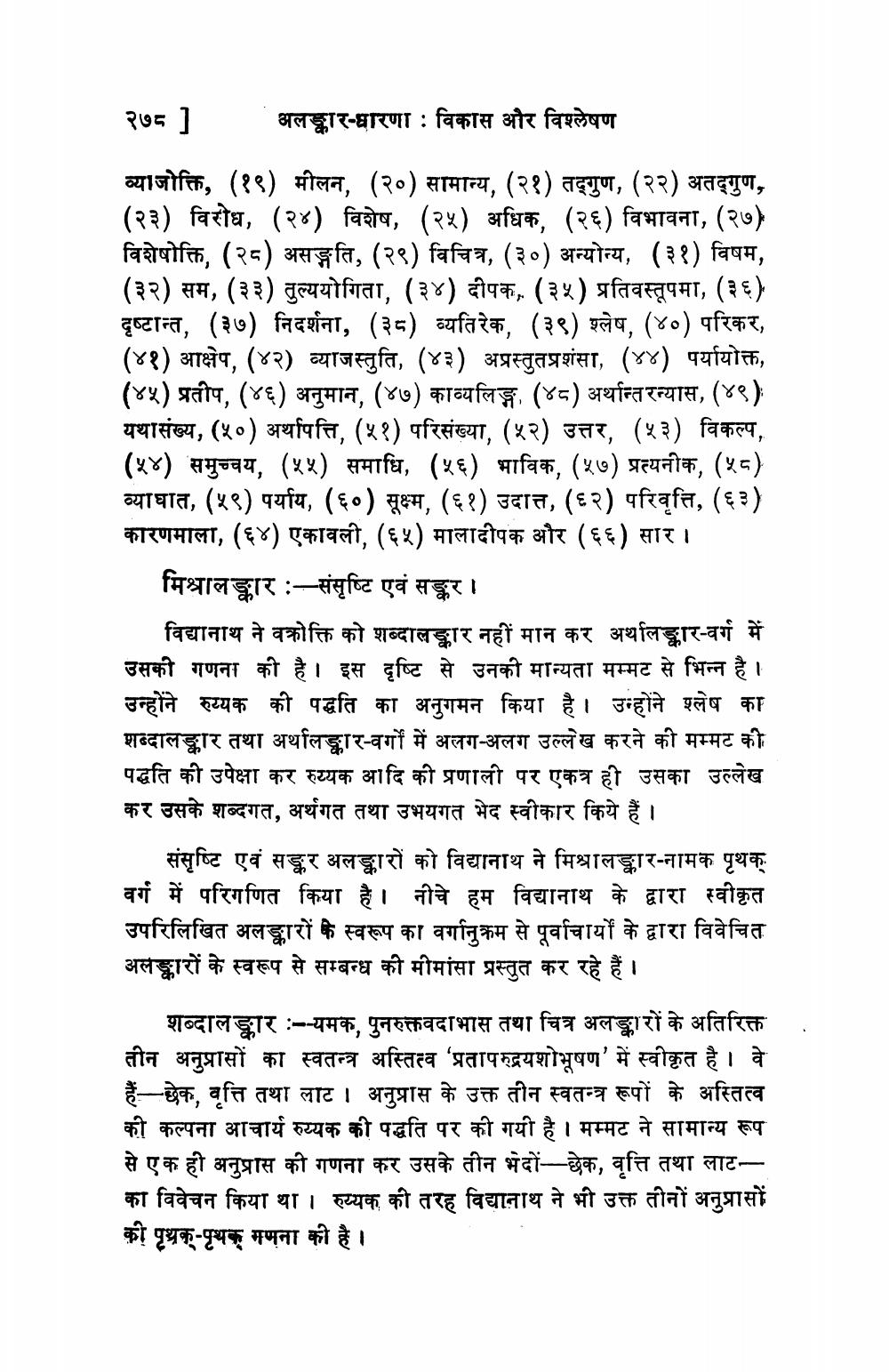________________
२७८ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
व्याजोक्ति, (१९) मीलन, (२०) सामान्य, (२१) तद्गुण, (२२) अतद्गुण, (२३) विरोध, (२४) विशेष, (२५) अधिक, (२६) विभावना, (२७) विशेषोक्ति, (२८) असङ्गति, (२९) विचित्र, (३०) अन्योन्य, (३१) विषम, (३२) सम, (३३) तुल्ययोगिता, (३४) दीपक, (३५) प्रतिवस्तूपमा, (३६) दृष्टान्त, (३७) निदर्शना, (३८) व्यतिरेक, (३९) श्लेष, (४०) परिकर, (४१) आक्षेप, (४२) व्याजस्तुति, (४३) अप्रस्तुतप्रशंसा, (४४) पर्यायोक्त, (४५) प्रतीप, (४६) अनुमान, (४७) काव्य लिङ्ग, (४८) अर्थान्तरन्यास, (४९) यथासंख्य, (५०) अर्थापत्ति, (५१) परिसंख्या, (५२) उत्तर, (५३) विकल्प, (५४) समुच्चय, (५५) समाधि, (५६) भाविक, (५७) प्रत्यनीक, (५८) व्याघात, (५९) पर्याय, (६०) सूक्ष्म, (६१) उदात्त, (६२) परिवृत्ति, (६३) कारणमाला, (६४) एकावली, (६५) मालादीपक और (६६) सार ।
मिश्रालङ्कार :-संसृष्टि एवं सङ्कर ।
विद्यानाथ ने वक्रोक्ति को शब्दालङ्कार नहीं मान कर अर्थालङ्कार-वर्ग में उसकी गणना की है। इस दृष्टि से उनकी मान्यता मम्मट से भिन्न है । उन्होंने रुय्यक की पद्धति का अनुगमन किया है। उन्होंने श्लेष का शब्दालङ्कार तथा अर्थालङ्कार-वर्गों में अलग-अलग उल्लेख करने की मम्मट की पद्धति की उपेक्षा कर रुय्यक आदि की प्रणाली पर एकत्र ही उसका उल्लेख कर उसके शब्दगत, अर्थगत तथा उभयगत भेद स्वीकार किये हैं। ___ संसृष्टि एवं सङ्कर अलङ्कारों को विद्यानाथ ने मिश्रालङ्कार-नामक पृथक वर्ग में परिगणित किया है। नीचे हम विद्यानाथ के द्वारा स्वीकृत उपरिलिखित अलङ्कारों के स्वरूप का वर्गानुक्रम से पूर्वाचार्यों के द्वारा विवेचित अलङ्कारों के स्वरूप से सम्बन्ध की मीमांसा प्रस्तुत कर रहे हैं ।
शब्दालङ्कार :--यमक, पुनरुक्तवदाभास तथा चित्र अलङ्कारों के अतिरिक्त तीन अनुप्रासों का स्वतन्त्र अस्तित्व 'प्रतापरुद्रयशोभूषण' में स्वीकृत है। वे हैं-छेक, वृत्ति तथा लाट । अनुप्रास के उक्त तीन स्वतन्त्र रूपों के अस्तित्व की कल्पना आचार्य रुय्यक की पद्धति पर की गयी है । मम्मट ने सामान्य रूप से एक ही अनुप्रास की गणना कर उसके तीन भेदों-छेक, वृत्ति तथा लाटका विवेचन किया था। रुय्यक की तरह विद्यानाथ ने भी उक्त तीनों अनुप्रासों की पृथक्-पृथक गणना की है।