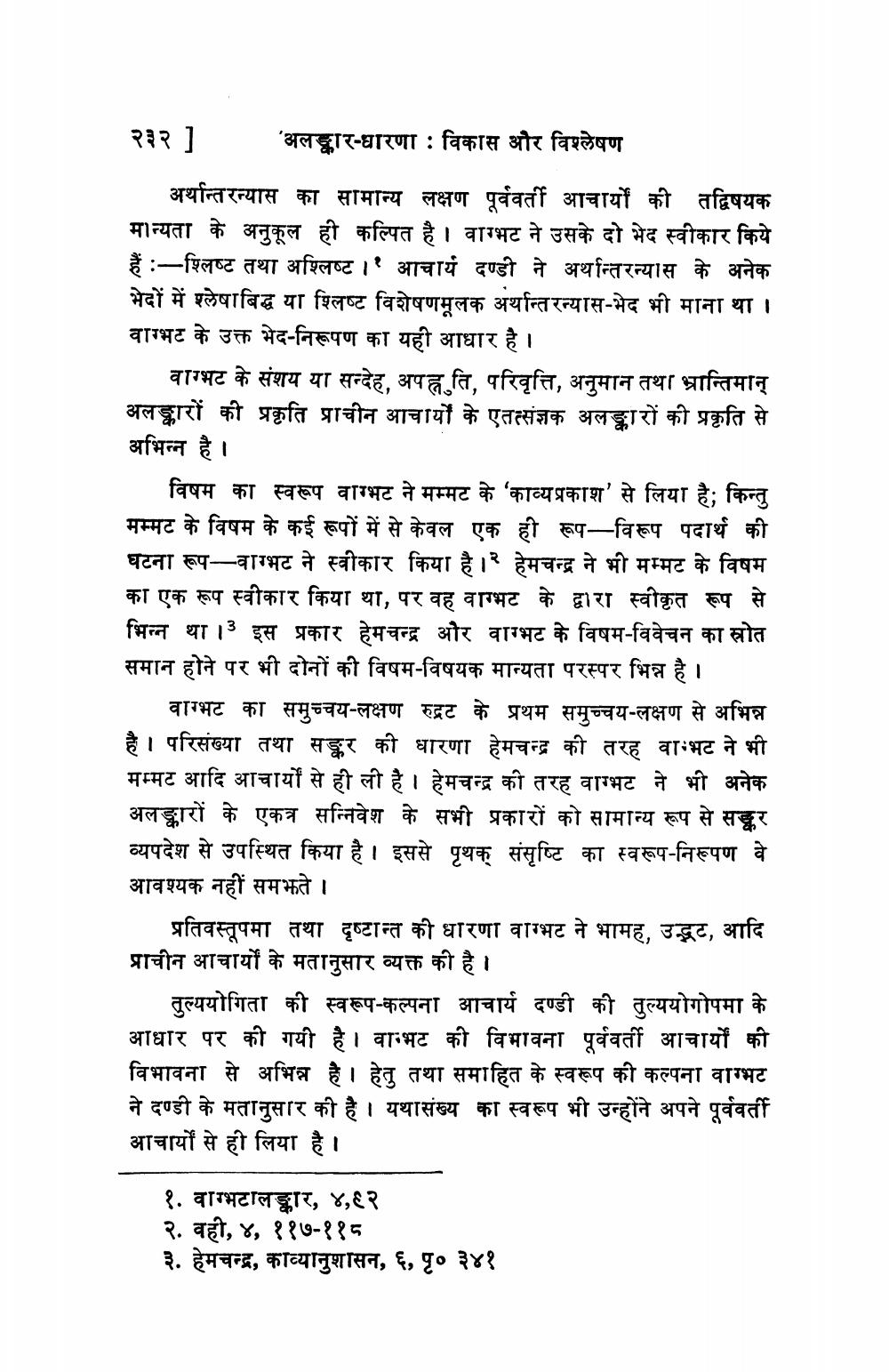________________
२३२ ]
'अलङ्कार- धारणा : विकास और विश्लेषण
अर्थान्तरन्यास का सामान्य लक्षण पूर्ववर्ती आचार्यों की तद्विषयक मान्यता के अनुकूल ही कल्पित है । वाग्भट ने उसके दो भेद स्वीकार किये हैं: - श्लिष्ट तथा अश्लिष्ट । आचार्य दण्डी ने अर्थान्तरन्यास के अनेक भेदों में श्लेषाबिद्ध या श्लिष्ट विशेषणमूलक अर्थान्तरन्यास-भेद भी माना था । वाग्भट के उक्त भेद-निरूपण का यही आधार है ।
वाग्भट के संशय या सन्देह, अपह्न ुति, परिवृत्ति, अनुमान तथा भ्रान्तिमान् अलङ्कारों की प्रकृति प्राचीन आचार्यों के एतत्संज्ञक अलङ्कारों की प्रकृति से अभिन्न है ।
विषम का स्वरूप वाग्भट ने मम्मट के 'काव्यप्रकाश' से लिया है; किन्तु मम्मट के विषम के कई रूपों में से केवल एक ही रूप - 1 - विरूप पदार्थ की घटना रूप – वाग्भट ने स्वीकार किया है । २ हेमचन्द्र ने भी मम्मट के विषम का एक रूप स्वीकार किया था, पर वह वाग्भट के द्वारा स्वीकृत रूप से भिन्न था। इस प्रकार हेमचन्द्र और वाग्भट के विषम-विवेचन का स्रोत समान होने पर भी दोनों की विषम-विषयक मान्यता परस्पर भिन्न है ।
वाग्भट का समुच्चय-लक्षण रुद्रट के प्रथम समुच्चय-लक्षण से अभिन्न है । परिसंख्या तथा सङ्कर की धारणा हेमचन्द्र की तरह वाग्भट ने भी मम्मट आदि आचार्यों से ही ली है। हेमचन्द्र की तरह वाग्भट ने भी अनेक अलङ्कारों के एकत्र सन्निवेश के सभी प्रकारों को सामान्य रूप से सङ्कर व्यपदेश से उपस्थित किया है । इससे पृथक् संसृष्टि का स्वरूप - निरूपण वे आवश्यक नहीं समझते ।
प्रतिवस्तूपमा तथा दृष्टान्त की धारणा वाग्भट ने भामह, उद्भट, आदि प्राचीन आचार्यों के मतानुसार व्यक्त की है ।
तुल्ययोगिता की स्वरूप - कल्पना आचार्य दण्डी की तुल्ययोगोपमा के आधार पर की गयी है । वाग्भट की विभावना पूर्ववर्ती आचार्यों की विभावना से अभिन्न है । हेतु तथा समाहित के स्वरूप की कल्पना वाग्भट दण्डी के मतानुसार की है । यथासंख्य का स्वरूप भी उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से ही लिया है ।
१. वाग्भटालङ्कार, ४,६२
२. वही, ४, ११७-११८
३. हेमचन्द्र, काव्यानुशासन, ६, पृ० ३४१