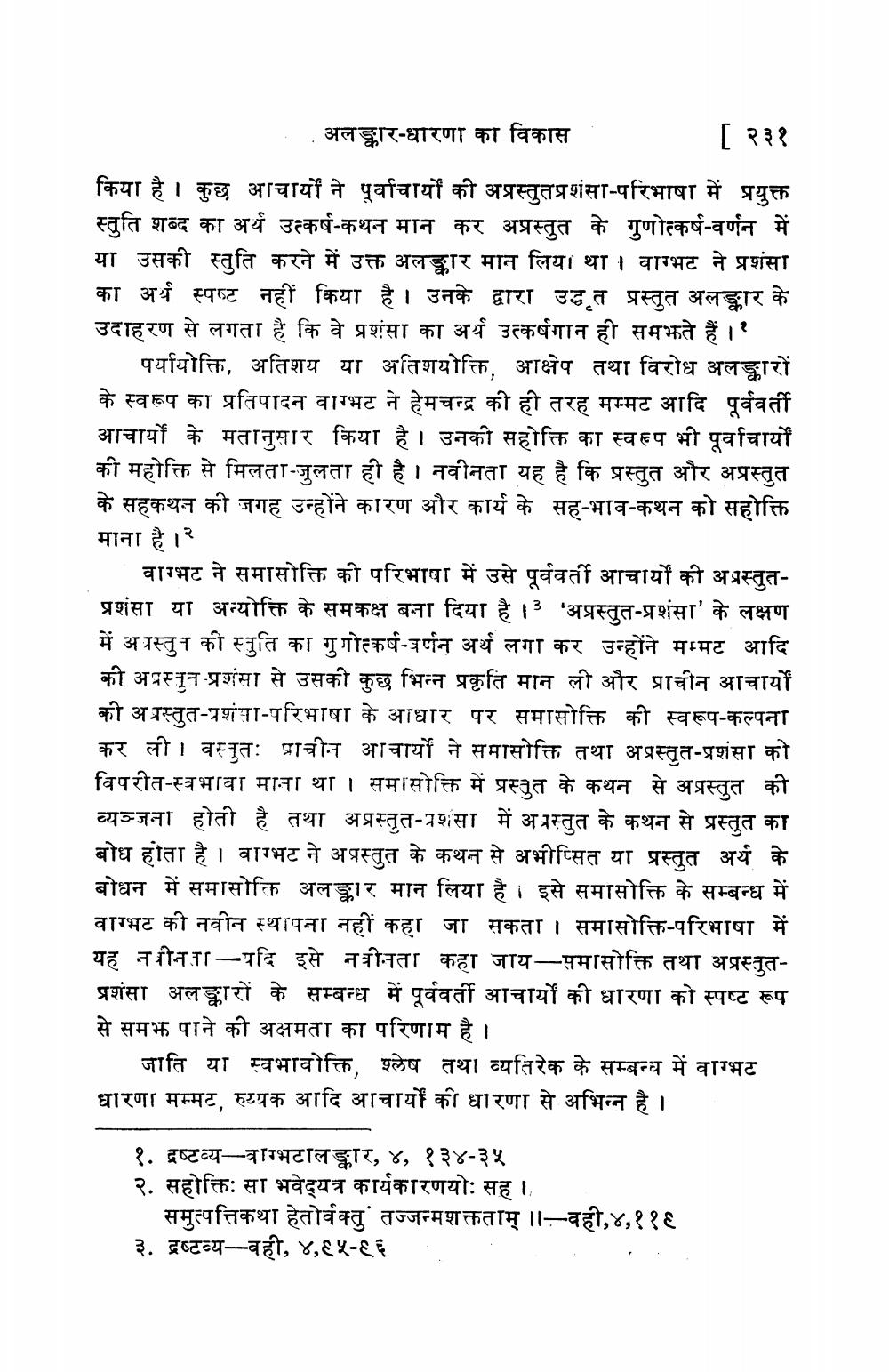________________
अलङ्कार-धारणा का विकास
[२३१
किया है। कुछ आचार्यों ने पूर्वाचार्यों की अप्रस्तुतप्रशंसा-परिभाषा में प्रयुक्त स्तुति शब्द का अर्थ उत्कर्ष-कथन मान कर अप्रस्तुत के गुणोत्कर्ष-वर्णन में या उसकी स्तुति करने में उक्त अलङ्कार मान लिया था। वाग्भट ने प्रशंसा का अर्थ स्पष्ट नहीं किया है। उनके द्वारा उद्धत प्रस्तुत अलङ्कार के उदाहरण से लगता है कि वे प्रशंसा का अर्थ उत्कर्षगान ही समझते हैं।'
पर्यायोक्ति, अतिशय या अतिशयोक्ति, आक्षेप तथा विरोध अलङ्कारों के स्वरूप का प्रतिपादन वाग्भट ने हेमचन्द्र की ही तरह मम्मट आदि पूर्ववर्ती आचार्यों के मतानुसार किया है। उनकी सहोक्ति का स्वरूप भी पूर्वाचार्यों की महोक्ति से मिलता-जुलता ही है। नवीनता यह है कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत के सहकथन की जगह उन्होंने कारण और कार्य के सह-भाव-कथन को सहोक्ति माना है। ___ वाग्भट ने समासोक्ति की परिभाषा में उसे पूर्ववर्ती आचार्यों की अप्रस्तुतप्रशंसा या अन्योक्ति के समकक्ष बना दिया है। 3 'अप्रस्तुत-प्रशंसा' के लक्षण में अपस्तुन की स्तुति का गुगोत्कर्ष-वर्णन अर्थ लगा कर उन्होंने मम्मट आदि की अप्रस्तुत प्रशंसा से उसकी कुछ भिन्न प्रकृति मान ली और प्राचीन आचार्यों की अप्रस्तुत-प्रशंसा-परिभाषा के आधार पर समासोक्ति की स्वरूप-कल्पना कर ली। वस्तुतः प्राचीन आचार्यों ने समासोक्ति तथा अप्रस्तुत-प्रशंसा को विपरीत-स्वभावा माना था । समासोक्ति में प्रस्तुत के कथन से अप्रस्तुत की व्यञ्जना होती है तथा अप्रस्तुत-प्रशंसा में अप्रस्तुत के कथन से प्रस्तुत का बोध होता है । वाग्भट ने अप्रस्तुत के कथन से अभीप्सित या प्रस्तुत अर्थ के बोधन में समासोक्ति अलङ्कार मान लिया है। इसे समासोक्ति के सम्बन्ध में वाग्भट की नवीन स्थापना नहीं कहा जा सकता। समासोक्ति-परिभाषा में यह नवीनता-यदि इसे नवीनता कहा जाय-समासोक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कारों के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती आचार्यों की धारणा को स्पष्ट रूप से समझ पाने की अक्षमता का परिणाम है।
जाति या स्वभावोक्ति, श्लेष तथा व्यतिरेक के सम्बन्ध में वाग्भट धारणा मम्मट, रुय्यक आदि आचार्यों की धारणा से अभिन्न है ।
१. द्रष्टव्य-वाग्भटालङ्कार, ४, १३४-३५ २. सहोक्तिः सा भवेद्यत्र कार्यकारणयोः सह ।
समुत्पत्तिकथा हेतोर्वक्तुतज्जन्मशक्तताम् ।। वही,४,११६ ३. द्रष्टव्य-वही, ४,६५-६६