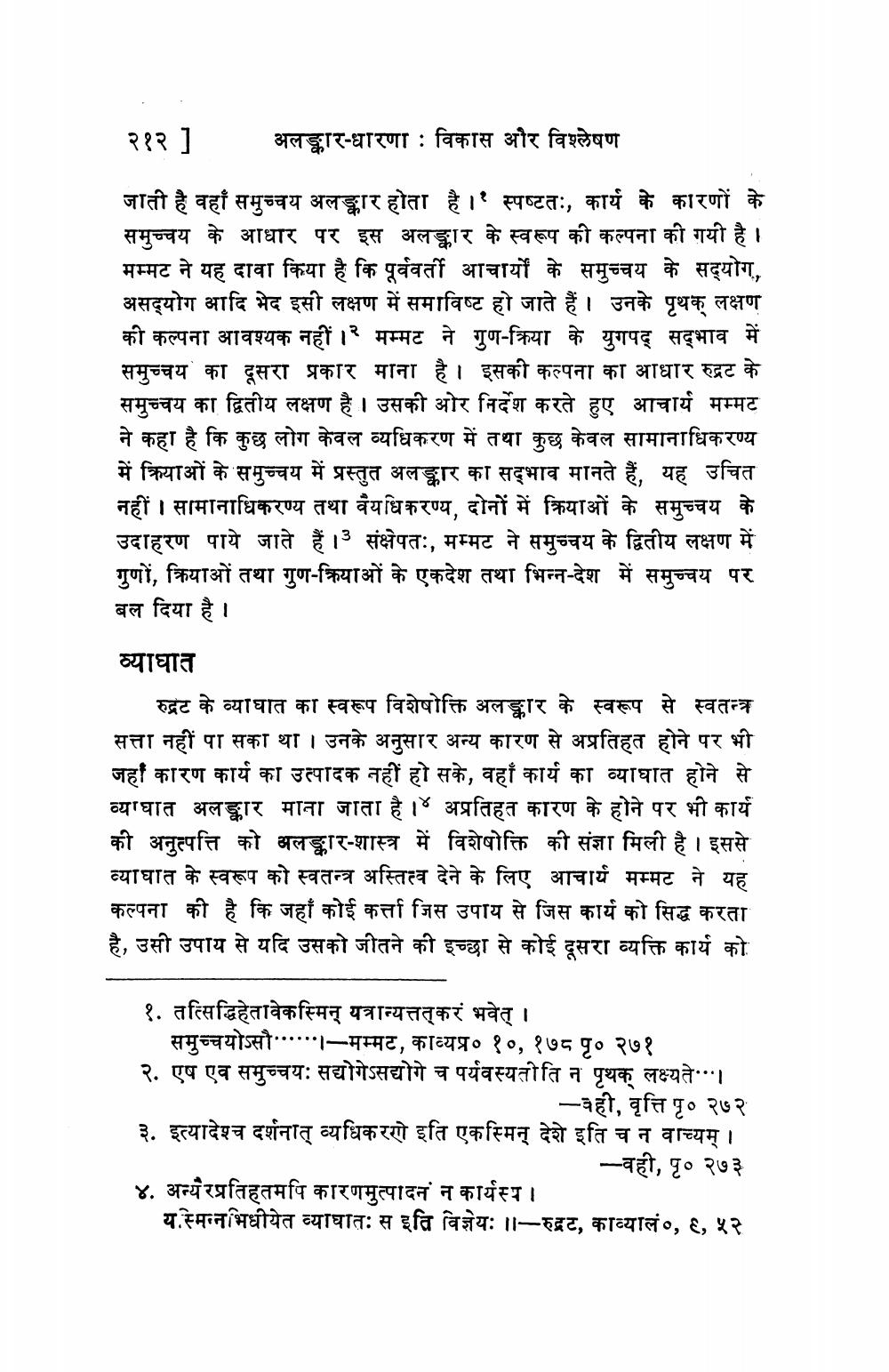________________
२१२ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
जाती है वहाँ समुच्चय अलङ्कार होता है।' स्पष्टतः, कार्य के कारणों के समुच्चय के आधार पर इस अलङ्कार के स्वरूप की कल्पना की गयी है। मम्मट ने यह दावा किया है कि पूर्ववर्ती आचार्यों के समुच्चय के सद्योग, असद्योग आदि भेद इसी लक्षण में समाविष्ट हो जाते हैं। उनके पृथक् लक्षण की कल्पना आवश्यक नहीं।२ मम्मट ने गुण-क्रिया के युगपद् सद्भाव में समुच्चय का दूसरा प्रकार माना है। इसकी कल्पना का आधार रुद्रट के समुच्चय का द्वितीय लक्षण है । उसकी ओर निर्देश करते हुए आचार्य मम्मट ने कहा है कि कुछ लोग केवल व्यधिकरण में तथा कुछ केवल सामानाधिकरण्य में क्रियाओं के समुच्चय में प्रस्तुत अलङ्कार का सद्भाव मानते हैं, यह उचित नहीं । सामानाधिकरण्य तथा वैयधिकरण्य, दोनों में क्रियाओं के समुच्चय के उदाहरण पाये जाते हैं। संक्षेपतः, मम्मट ने समुच्चय के द्वितीय लक्षण में गुणों, क्रियाओं तथा गुण-क्रियाओं के एकदेश तथा भिन्न-देश में समुच्चय पर बल दिया है।
व्याघात
रुद्रट के व्याघात का स्वरूप विशेषोक्ति अलङ्कार के स्वरूप से स्वतन्त्र सत्ता नहीं पा सका था। उनके अनुसार अन्य कारण से अप्रतिहत होने पर भी जहां कारण कार्य का उत्पादक नहीं हो सके, वहाँ कार्य का व्याघात होने से व्याघात अलङ्कार माना जाता है।४ अप्रतिहत कारण के होने पर भी कार्य की अनुत्पत्ति को अलङ्कार-शास्त्र में विशेषोक्ति की संज्ञा मिली है। इससे व्याघात के स्वरूप को स्वतन्त्र अस्तित्व देने के लिए आचार्य मम्मट ने यह कल्पना की है कि जहाँ कोई कर्ता जिस उपाय से जिस कार्य को सिद्ध करता है, उसी उपाय से यदि उसको जीतने की इच्छा से कोई दूसरा व्यक्ति कार्य को
१. तत्सिद्धिहेतावेकस्मिन् यत्रान्यत्तत्करं भवेत् ।
समुच्चयोऽसौ.....।-मम्मट, काव्यप्र० १०, १७८ पृ० २७१ २. एष एव समुच्चयः सद्योगेऽसद्योगे च पर्यवस्यतीति न पृथक् लक्ष्यते ।
-वही, वृत्ति पृ० २७२ ३. इत्यादेश्च दर्शनात् व्यधिकरणे इति एकस्मिन् देशे इति च न वाच्यम् ।
-वही, पृ० २७३ ४. अन्यैरप्रतिहतमपि कारणमुत्पादन न कार्यस्थ।
यस्मिन्नभिधीयेत व्याघातः स इति विज्ञेयः ॥-रुद्रट, काव्यालं०, ६, ५२