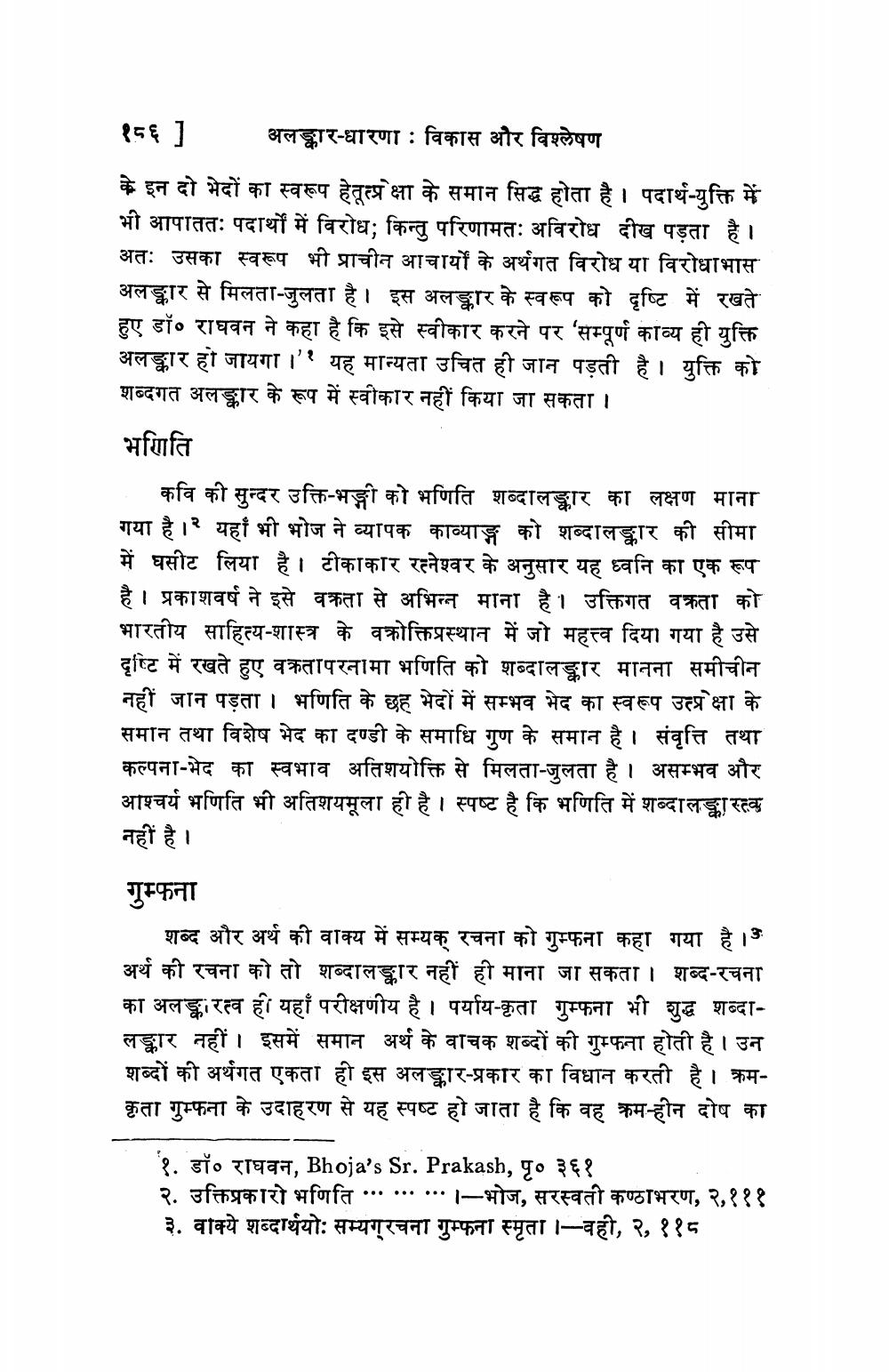________________
१८६ ] अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण के इन दो भेदों का स्वरूप हेतूत्प्रेक्षा के समान सिद्ध होता है। पदार्थ-युक्ति में भी आपाततः पदार्थों में विरोध; किन्तु परिणामतः अविरोध दीख पड़ता है। अतः उसका स्वरूप भी प्राचीन आचार्यों के अर्थगत विरोध या विरोधाभास अलङ्कार से मिलता-जुलता है। इस अलङ्कार के स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए डॉ० राघवन ने कहा है कि इसे स्वीकार करने पर 'सम्पूर्ण काव्य ही युक्ति अलङ्कार हो जायगा।'' यह मान्यता उचित ही जान पड़ती है। युक्ति को शब्दगत अलङ्कार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। भणिति
कवि की सुन्दर उक्ति-भङ्गी को भणिति शब्दालङ्कार का लक्षण माना गया है। यहाँ भी भोज ने व्यापक काव्याङ्ग को शब्दालङ्कार की सीमा में घसीट लिया है। टीकाकार रत्नेश्वर के अनुसार यह ध्वनि का एक रूप है। प्रकाशवर्ष ने इसे वक्रता से अभिन्न माना है। उक्तिगत वक्रता को भारतीय साहित्य-शास्त्र के वक्रोक्तिप्रस्थान में जो महत्त्व दिया गया है उसे दृष्टि में रखते हुए वक्रतापरनामा भणिति को शब्दालङ्कार मानना समीचीन नहीं जान पड़ता। भणिति के छह भेदों में सम्भव भेद का स्वरूप उत्प्रेक्षा के समान तथा विशेष भेद का दण्डी के समाधि गुण के समान है। संवृत्ति तथा कल्पना-भेद का स्वभाव अतिशयोक्ति से मिलता-जुलता है। असम्भव और आश्चर्य भणिति भी अतिशयमूला ही है । स्पष्ट है कि भणिति में शब्दालङ्कारत्व नहीं है।
गुम्फना
शब्द और अर्थ की वाक्य में सम्यक् रचना को गुम्फना कहा गया है। अर्थ की रचना को तो शब्दालङ्कार नहीं ही माना जा सकता। शब्द-रचना का अलङ्क रत्व ही यहाँ परीक्षणीय है। पर्याय-कृता गुम्फना भी शुद्ध शब्दालङ्कार नहीं। इसमें समान अर्थ के वाचक शब्दों की गुम्फना होती है । उन शब्दों की अर्थगत एकता ही इस अलङ्कार-प्रकार का विधान करती है। क्रमकृता गुम्फना के उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह क्रम-हीन दोष का
१. डॉ० राघवन, Bhoja's Sr. Prakash, पृ० ३६१ ।। २. उक्तिप्रकारो भणिति ... ... ... ।-भोज, सरस्वती कण्ठाभरण, २,१११ ३. वाक्ये शब्दार्थयोः सम्यग्रचना गुम्फना स्मृता। वही, २, ११८