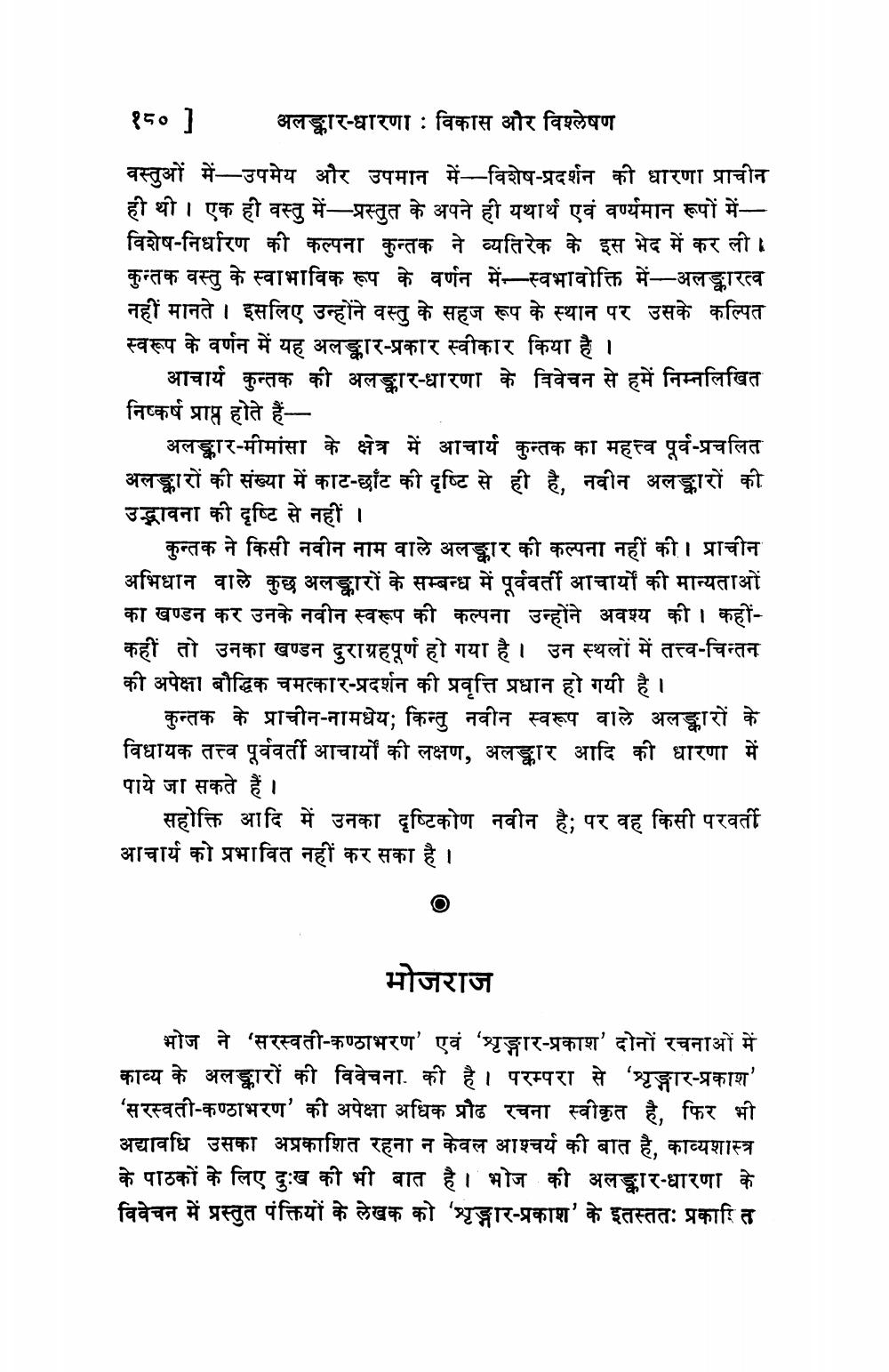________________
१८० ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
वस्तुओं में-उपमेय और उपमान में विशेष-प्रदर्शन की धारणा प्राचीन ही थी। एक ही वस्तु में प्रस्तुत के अपने ही यथार्थ एवं वर्ण्यमान रूपों मेंविशेष-निर्धारण की कल्पना कुन्तक ने व्यतिरेक के इस भेद में कर ली। कुन्तक वस्तु के स्वाभाविक रूप के वर्णन में स्वभावोक्ति में-अलङ्कारत्व नहीं मानते। इसलिए उन्होंने वस्तु के सहज रूप के स्थान पर उसके कल्पित स्वरूप के वर्णन में यह अलङ्कार-प्रकार स्वीकार किया है ।
आचार्य कुन्तक की अलङ्कार-धारणा के विवेचन से हमें निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं___ अलङ्कार-मीमांसा के क्षेत्र में आचार्य कुन्तक का महत्त्व पूर्व-प्रचलित अलङ्कारों की संख्या में काट-छाँट की दृष्टि से ही है, नवीन अलङ्कारों की उद्भावना की दृष्टि से नहीं । ___ कुन्तक ने किसी नवीन नाम वाले अलङ्कार की कल्पना नहीं की। प्राचीन अभिधान वाले कुछ अलङ्कारों के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती आचार्यों की मान्यताओं का खण्डन कर उनके नवीन स्वरूप की कल्पना उन्होंने अवश्य की। कहींकहीं तो उनका खण्डन दुराग्रहपूर्ण हो गया है। उन स्थलों में तत्त्व-चिन्तन की अपेक्षा बौद्धिक चमत्कार-प्रदर्शन की प्रवृत्ति प्रधान हो गयी है।
कुन्तक के प्राचीन-नामधेय; किन्तु नवीन स्वरूप वाले अलङ्कारों के विधायक तत्त्व पूर्ववर्ती आचार्यों की लक्षण, अलङ्कार आदि की धारणा में पाये जा सकते हैं। ____ सहोक्ति आदि में उनका दृष्टिकोण नवीन है; पर वह किसी परवर्ती आचार्य को प्रभावित नहीं कर सका है ।
भोजराज
भोज ने 'सरस्वती-कण्ठाभरण' एवं 'शृङ्गार-प्रकाश' दोनों रचनाओं में काव्य के अलङ्कारों की विवेचना. की है। परम्परा से 'शृङ्गार-प्रकाश' 'सरस्वती-कण्ठाभरण' की अपेक्षा अधिक प्रौढ रचना स्वीकृत है, फिर भी अद्यावधि उसका अप्रकाशित रहना न केवल आश्चर्य की बात है, काव्यशास्त्र के पाठकों के लिए दुःख की भी बात है। भोज की अलङ्कार-धारणा के विवेचन में प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक को 'शृङ्गार-प्रकाश' के इतस्ततः प्रकाशित