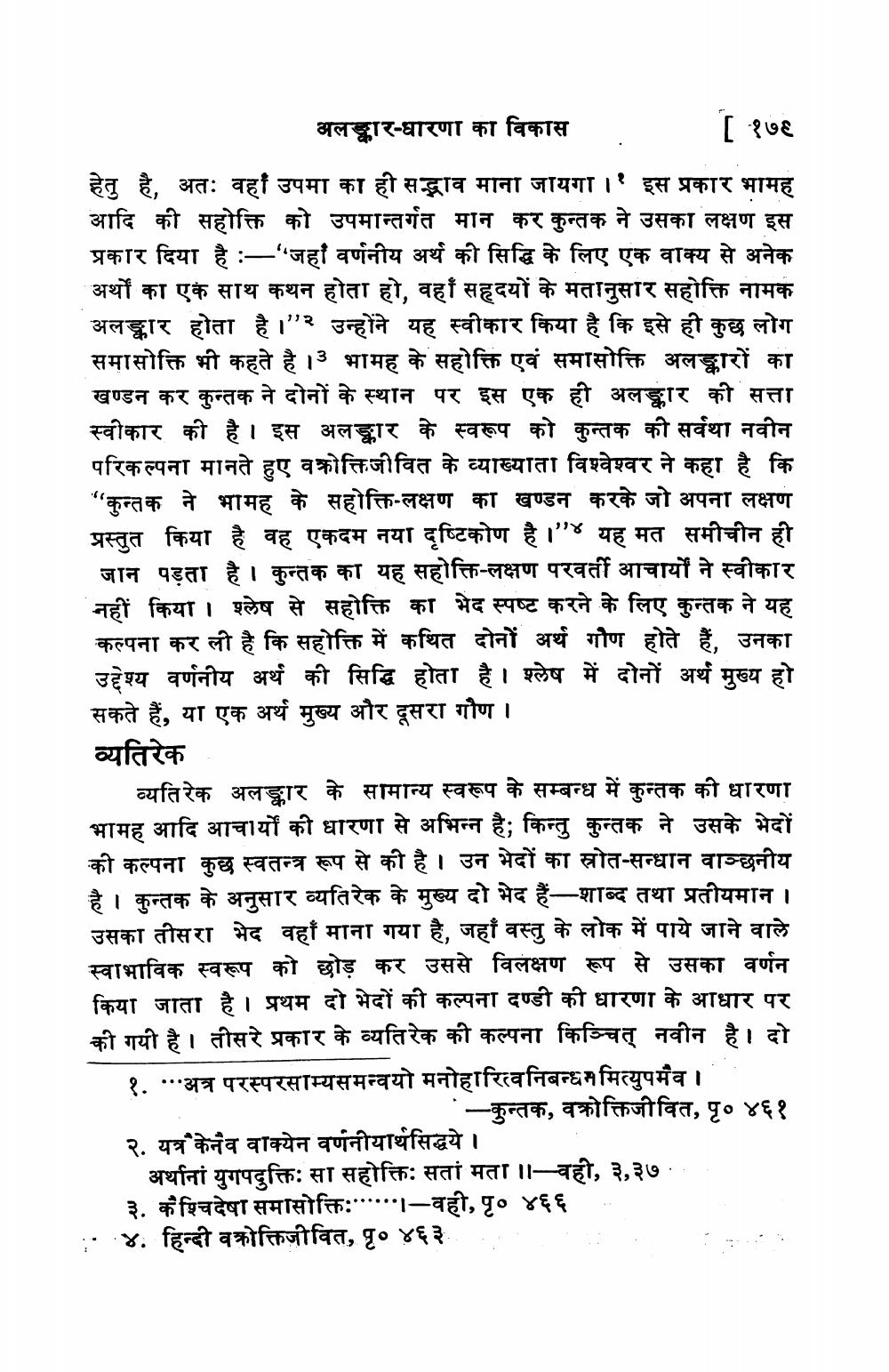________________
अलङ्कार-धारणा का विकास
[ १७९
हेतु है, अतः वहाँ उपमा का ही सद्भाव माना जायगा।' इस प्रकार भामह आदि की सहोक्ति को उपमान्तर्गत मान कर कुन्तक ने उसका लक्षण इस प्रकार दिया है :-"जहां वर्णनीय अर्थ की सिद्धि के लिए एक वाक्य से अनेक अर्थों का एक साथ कथन होता हो, वहाँ सहृदयों के मतानुसार सहोक्ति नामक अलङ्कार होता है।"२ उन्होंने यह स्वीकार किया है कि इसे ही कुछ लोग समासोक्ति भी कहते है । भामह के सहोक्ति एवं समासोक्ति अलङ्कारों का खण्डन कर कुन्तक ने दोनों के स्थान पर इस एक ही अलङ्कार की सत्ता स्वीकार की है। इस अलङ्कार के स्वरूप को कुन्तक की सर्वथा नवीन परिकल्पना मानते हुए वक्रोक्तिजीवित के व्याख्याता विश्वेश्वर ने कहा है कि "कुन्तक ने भामह के सहोक्ति-लक्षण का खण्डन करके जो अपना लक्षण प्रस्तुत किया है वह एकदम नया दृष्टिकोण है।"४ यह मत समीचीन ही जान पड़ता है। कुन्तक का यह सहोक्ति-लक्षण परवर्ती आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया। श्लेष से सहोक्ति का भेद स्पष्ट करने के लिए कुन्तक ने यह कल्पना कर ली है कि सहोक्ति में कथित दोनों अर्थ गौण होते हैं, उनका उद्देश्य वर्णनीय अर्थ की सिद्धि होता है। श्लेष में दोनों अर्थ मुख्य हो सकते हैं, या एक अर्थ मुख्य और दूसरा गौण । व्यतिरेक
व्यतिरेक अलङ्कार के सामान्य स्वरूप के सम्बन्ध में कुन्तक की धारणा भामह आदि आचार्यों की धारणा से अभिन्न है; किन्तु कुन्तक ने उसके भेदों की कल्पना कुछ स्वतन्त्र रूप से की है। उन भेदों का स्रोत-सन्धान वाञ्छनीय है । कुन्तक के अनुसार व्यतिरेक के मुख्य दो भेद हैं-शाब्द तथा प्रतीयमान । उसका तीसरा भेद वहाँ माना गया है, जहाँ वस्तु के लोक में पाये जाने वाले स्वाभाविक स्वरूप को छोड़ कर उससे विलक्षण रूप से उसका वर्णन किया जाता है। प्रथम दो भेदों की कल्पना दण्डी की धारणा के आधार पर की गयी है। तीसरे प्रकार के व्यतिरेक की कल्पना किञ्चित् नवीन है। दो १. .. अत्र परस्परसाम्यसमन्वयो मनोहारित्व निबन्धममित्युपमैव।
-कुन्तक, वक्रोक्तिजीवित, पृ० ४६१ २. यत्र केनैव वाक्येन वर्णनीयार्थसिद्धये । ___ अर्थानां युगपदुक्तिः सा सहोक्तिः सतां मता ॥ वही, ३,३७
३. कैश्चिदेषा समासोक्तिः......। वही, पृ० ४६६ .. ४. हिन्दी वक्रोक्तिजीवित, पृ० ४६३ .
. ......