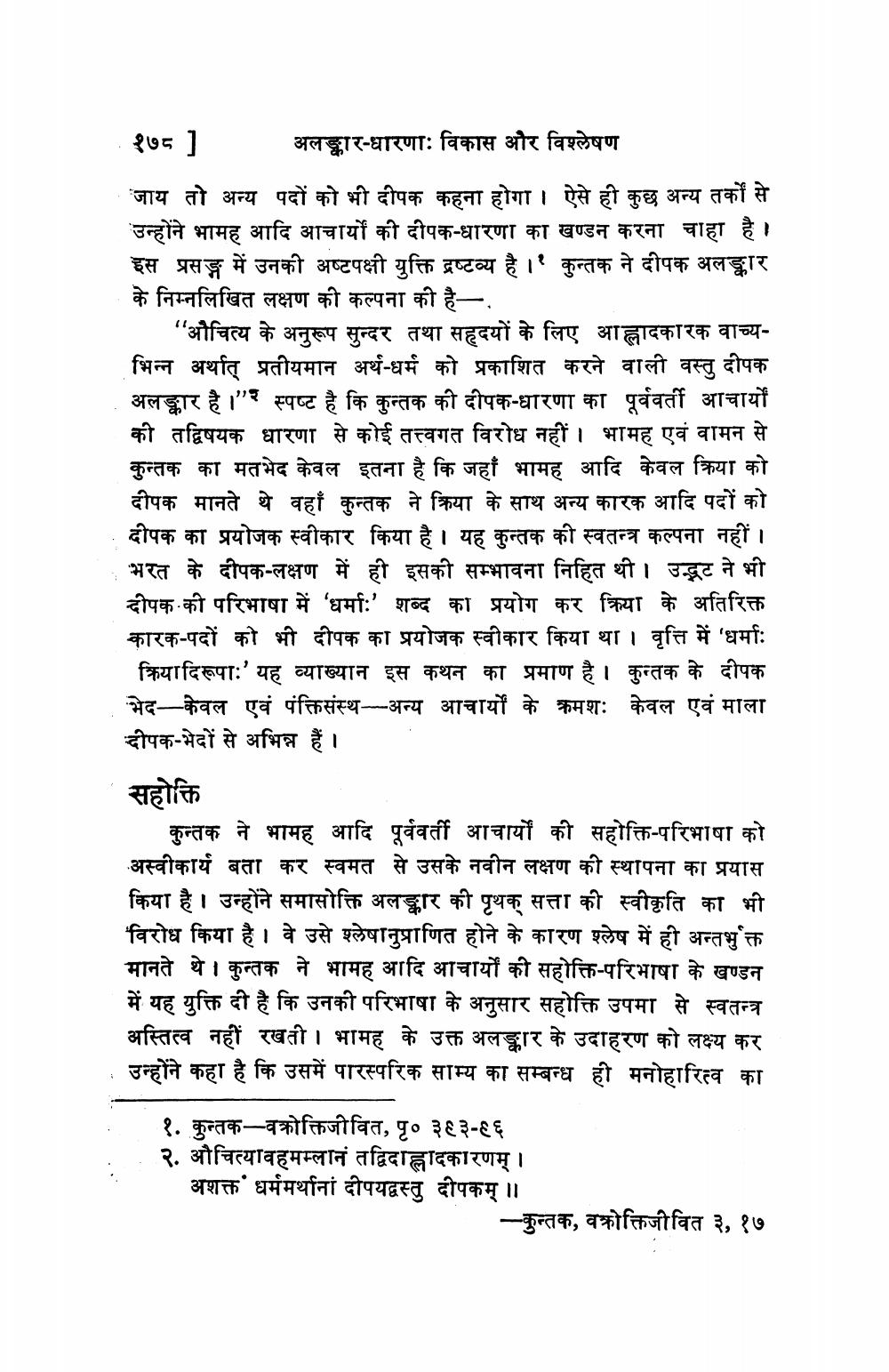________________
१७८ ] अलङ्कार-धारणाः विकास और विश्लेषण जाय तो अन्य पदों को भी दीपक कहना होगा। ऐसे ही कुछ अन्य तर्कों से उन्होंने भामह आदि आचार्यों की दीपक-धारणा का खण्डन करना चाहा है। इस प्रसङ्ग में उनकी अष्टपक्षी युक्ति द्रष्टव्य है ।' कुन्तक ने दीपक अलङ्कार के निम्नलिखित लक्षण की कल्पना की है
"औचित्य के अनुरूप सुन्दर तथा सहृदयों के लिए आह्लादकारक वाच्यभिन्न अर्थात् प्रतीयमान अर्थ-धर्म को प्रकाशित करने वाली वस्तु दीपक अलङ्कार है।"२ स्पष्ट है कि कुन्तक की दीपक-धारणा का पूर्ववर्ती आचार्यों की तद्विषयक धारणा से कोई तत्त्वगत विरोध नहीं। भामह एवं वामन से कुन्तक का मतभेद केवल इतना है कि जहाँ भामह आदि केवल क्रिया को दीपक मानते थे वहाँ कुन्तक ने क्रिया के साथ अन्य कारक आदि पदों को दीपक का प्रयोजक स्वीकार किया है। यह कुन्तक की स्वतन्त्र कल्पना नहीं। भरत के दीपक-लक्षण में ही इसकी सम्भावना निहित थी। उद्भट ने भी दीपक की परिभाषा में 'धर्माः' शब्द का प्रयोग कर क्रिया के अतिरिक्त कारक-पदों को भी दीपक का प्रयोजक स्वीकार किया था। वृत्ति में 'धर्माः क्रियादिरूपाः' यह व्याख्यान इस कथन का प्रमाण है। कुन्तक के दीपक भेद-केवल एवं पंक्तिसंस्थ-अन्य आचार्यों के क्रमशः केवल एवं माला दीपक-भेदों से अभिन्न हैं। सहोक्ति
कुन्तक ने भामह आदि पूर्ववर्ती आचार्यों की सहोक्ति-परिभाषा को अस्वीकार्य बता कर स्वमत से उसके नवीन लक्षण की स्थापना का प्रयास किया है। उन्होंने समासोक्ति अलङ्कार की पृथक् सत्ता की स्वीकृति का भी 'विरोध किया है। वे उसे श्लेषानुप्राणित होने के कारण श्लेष में ही अन्तभुक्त मानते थे। कुन्तक ने भामह आदि आचार्यों की सहोक्ति-परिभाषा के खण्डन में यह युक्ति दी है कि उनकी परिभाषा के अनुसार सहोक्ति उपमा से स्वतन्त्र
अस्तित्व नहीं रखती। भामह के उक्त अलङ्कार के उदाहरण को लक्ष्य कर . उन्होंने कहा है कि उसमें पारस्परिक साम्य का सम्बन्ध ही मनोहारित्व का . १. कुन्तक–वक्रोक्तिजीवित, पृ० ३६३-६६ .. २. औचित्यावहमम्लानं तद्विदाह्लादकारणम् । अशक्त धर्ममर्थानां दीपयवस्तु दीपकम् ॥
-कुन्तक, वक्रोक्तिजीवित ३, १७