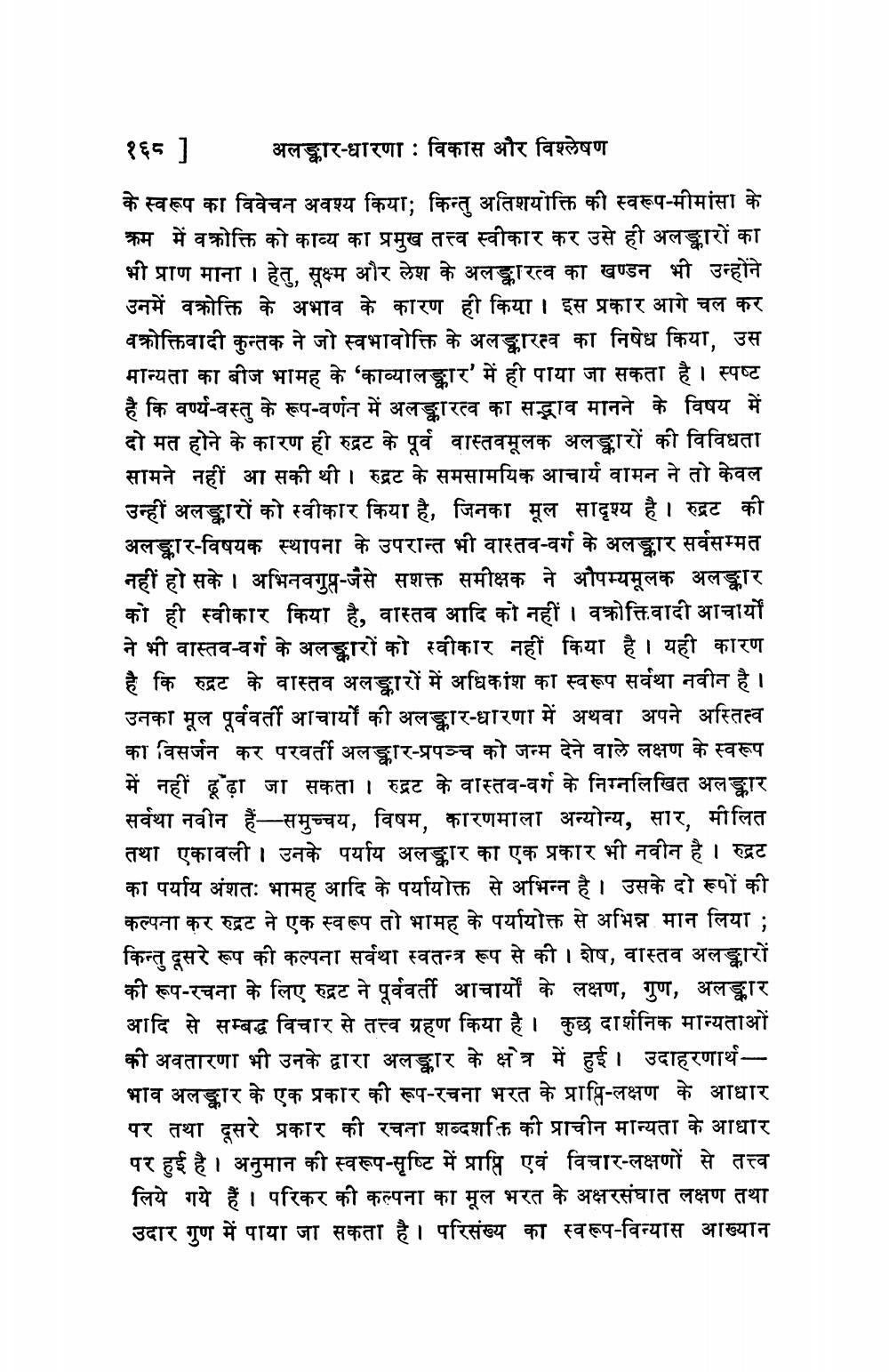________________
१६८ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
के स्वरूप का विवेचन अवश्य किया; किन्तु अतिशयोक्ति की स्वरूप-मीमांसा के क्रम में वक्रोक्ति को काव्य का प्रमुख तत्त्व स्वीकार कर उसे ही अलङ्कारों का भी प्राण माना । हेतु, सूक्ष्म और लेश के अलङ्कारत्व का खण्डन भी उन्होंने उनमें वक्रोक्ति के अभाव के कारण ही किया। इस प्रकार आगे चल कर वक्रोक्तिवादी कुन्तक ने जो स्वभावोक्ति के अलङ्कारत्व का निषेध किया, उस मान्यता का बीज भामह के 'काव्यालङ्कार' में ही पाया जा सकता है। स्पष्ट है कि वर्ण्य-वस्तु के रूप-वर्णन में अलङ्कारत्व का सद्भाव मानने के विषय में दो मत होने के कारण ही रुद्रट के पूर्व वास्तवमूलक अलङ्कारों की विविधता सामने नहीं आ सकी थी। रुद्रट के समसामयिक आचार्य वामन ने तो केवल उन्हीं अलङ्कारों को स्वीकार किया है, जिनका मूल सादृश्य है। रुद्रट की अलङ्कार-विषयक स्थापना के उपरान्त भी वास्तव-वर्ग के अलङ्कार सर्वसम्मत नहीं हो सके । अभिनवगुप्त-जैसे सशक्त समीक्षक ने औपम्यमूलक अलङ्कार को ही स्वीकार किया है, वास्तव आदि को नहीं । वक्रोक्तिवादी आचार्यों ने भी वास्तव-वर्ग के अलङ्कारों को स्वीकार नहीं किया है। यही कारण है कि रुद्रट के वास्तव अलङ्कारों में अधिकांश का स्वरूप सर्वथा नवीन है । उनका मूल पूर्ववर्ती आचार्यों की अलङ्कार-धारणा में अथवा अपने अस्तित्व का विसर्जन कर परवर्ती अलङ्कार-प्रपञ्च को जन्म देने वाले लक्षण के स्वरूप में नहीं ढूढ़ा जा सकता। रुद्रट के वास्तव-वर्ग के निम्नलिखित अलङ्कार सर्वथा नवीन हैं—समुच्चय, विषम, कारणमाला अन्योन्य, सार, मीलित तथा एकावली। उनके पर्याय अलङ्कार का एक प्रकार भी नवीन है । रुद्रट का पर्याय अंशतः भामह आदि के पर्यायोक्त से अभिन्न है। उसके दो रूपों की कल्पना कर रुद्रट ने एक स्वरूप तो भामह के पर्यायोक्त से अभिन्न मान लिया ; किन्तु दूसरे रूप की कल्पना सर्वथा स्वतन्त्र रूप से की। शेष, वास्तव अलङ्कारों की रूप-रचना के लिए रुद्रट ने पूर्ववर्ती आचार्यों के लक्षण, गुण, अलङ्कार आदि से सम्बद्ध विचार से तत्त्व ग्रहण किया है। कुछ दार्शनिक मान्यताओं की अवतारणा भी उनके द्वारा अलङ्कार के क्षेत्र में हुई। उदाहरणार्थभाव अलङ्कार के एक प्रकार की रूप-रचना भरत के प्राप्ति-लक्षण के आधार पर तथा दूसरे प्रकार की रचना शब्दशक्ति की प्राचीन मान्यता के आधार पर हुई है। अनुमान की स्वरूप-सृष्टि में प्राप्ति एवं विचार-लक्षणों से तत्त्व लिये गये हैं। परिकर की कल्पना का मूल भरत के अक्षरसंघात लक्षण तथा उदार गुण में पाया जा सकता है। परिसंख्य का स्वरूप-विन्यास आख्यान