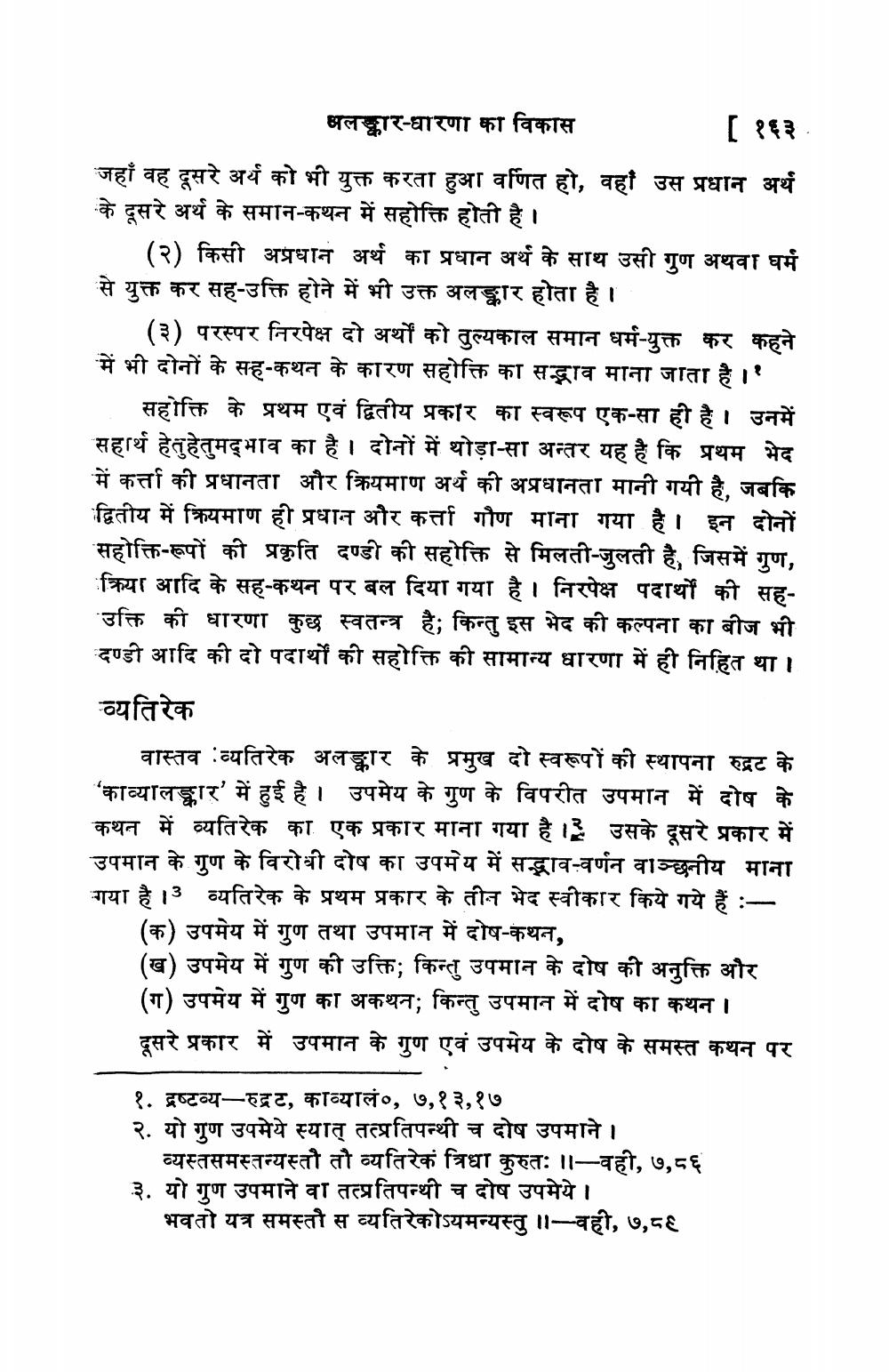________________
अलङ्कार-धारणा का विकास
[ १६३. जहाँ वह दूसरे अर्थ को भी युक्त करता हुआ वर्णित हो, वहाँ उस प्रधान अर्थ -के दूसरे अर्थ के समान - कथन में सहोक्ति होती है ।
(२) किसी अप्रधानं अर्थ का प्रधान अर्थ के साथ उसी गुण अथवा धर्म से युक्त कर सह उक्ति होने में भी उक्त अलङ्कार होता है ।
(३) परस्पर निरपेक्ष दो अर्थों को तुल्यकाल समान धर्म-युक्त कर कहने में भी दोनों के सह कथन के कारण सहोक्ति का सद्भाव माना जाता है । '
सहोक्ति के प्रथम एवं द्वितीय प्रकार का स्वरूप एक-सा ही है । उनमें सहार्थ हेतुहेतुमद्भाव का है । दोनों में थोड़ा-सा अन्तर यह है कि प्रथम भेद में कर्त्ता की प्रधानता और क्रियमाण अर्थ की अप्रधानता मानी गयी है, जबकि द्वितीय में क्रियमाण ही प्रधान और कर्त्ता गौण माना गया है । इन दोनों सहोक्ति - रूपों की प्रकृति दण्डी की सहोक्ति से मिलती-जुलती है, जिसमें गुण, क्रिया आदि के सह कथन पर बल दिया गया है । निरपेक्ष पदार्थों की सहउक्ति की धारणा कुछ स्वतन्त्र है; किन्तु इस भेद की कल्पना का बीज भी - दण्डी आदि की दो पदार्थों की सहोक्ति की सामान्य धारणा में ही निहित था ।
व्यतिरेक
वास्तव : व्यतिरेक अलङ्कार के प्रमुख दो स्वरूपों की स्थापना रुद्रट के 'काव्यालङ्कार' में हुई है । उपमेय के गुण के विपरीत उपमान में दोष के कथन में व्यतिरेक का एक प्रकार माना गया है । 2 उसके दूसरे प्रकार में उपमान के गुण के विरोधी दोष का उपमेय में सद्भाव वर्णन वाञ्छनीय माना गया है । 3 व्यतिरेक के प्रथम प्रकार के तीन भेद स्वीकार किये गये हैं
(क) उपमेय में गुण तथा उपमान में दोष-कथन,
(ख) उपमेय में गुण की उक्ति; किन्तु उपमान के दोष की अनुक्ति और (ग) उपमेय में गुण का अकथन; किन्तु उपमान में दोष का कथन ।
दूसरे प्रकार में उपमान के गुण एवं उपमेय के दोष के समस्त कथन पर
१. द्रष्टव्य - रुद्रट, काव्यालं०, ७,१३,१७
२. यो गुण उपमेये स्यात् तत्प्रतिपन्थी च दोष उपमाने ।
व्यस्तसमस्तन्यस्तौ तौ व्यतिरेकं त्रिधा कुरुतः ॥ - वही, ७, ८६
३. यो गुण उपमाने वा तत्प्रतिपन्थी च दोष उपमेये ।
भवतो यत्र समस्तौ स व्यतिरेकोऽयमन्यस्तु ॥ - वही, ७, ८६
-: