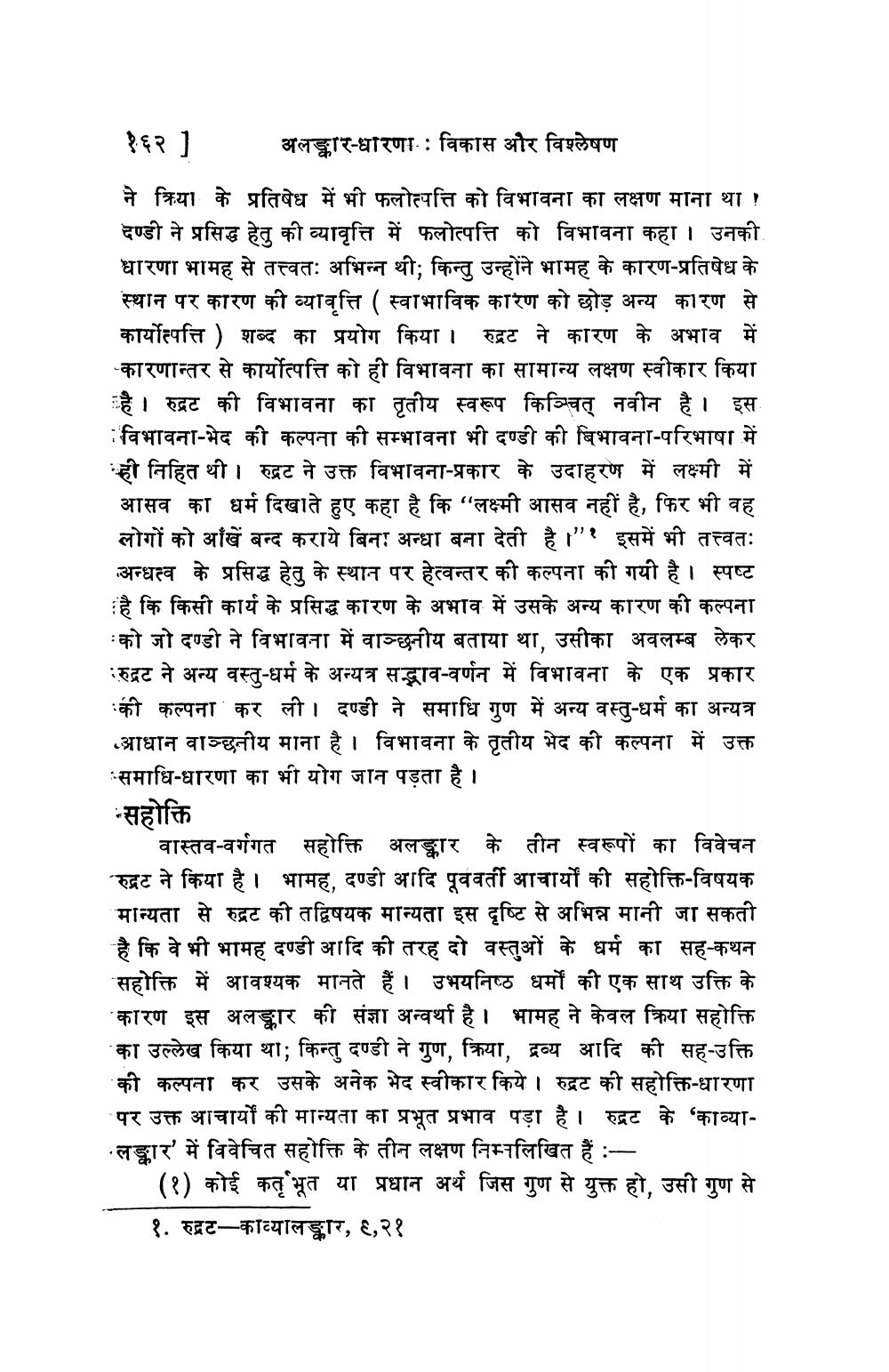________________
१६२ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
ने क्रिया के प्रतिषेध में भी फलोत्पत्ति को विभावना का लक्षण माना था। दण्डी ने प्रसिद्ध हेतु की व्यावृत्ति में फलोत्पत्ति को विभावना कहा। उनकी धारणा भामह से तत्त्वतः अभिन्न थी; किन्तु उन्होंने भामह के कारण-प्रतिषेध के स्थान पर कारण की व्यावृत्ति ( स्वाभाविक कारण को छोड़ अन्य कारण से कार्योत्पत्ति ) शब्द का प्रयोग किया। रुद्रट ने कारण के अभाव में कारणान्तर से कार्योत्पत्ति को ही विभावना का सामान्य लक्षण स्वीकार किया है। रुद्रट की विभावना का तृतीय स्वरूप किञ्चित् नवीन है। इस विभावना-भेद की कल्पना की सम्भावना भी दण्डी की बिभावना-परिभाषा में ही निहित थी। रुद्रट ने उक्त विभावना-प्रकार के उदाहरण में लक्ष्मी में आसव का धर्म दिखाते हुए कहा है कि "लक्ष्मी आसव नहीं है, फिर भी वह लोगों को आँखें बन्द कराये बिना अन्धा बना देती है।"१ इसमें भी तत्त्वतः अन्धत्व के प्रसिद्ध हेतु के स्थान पर हेत्वन्तर की कल्पना की गयी है। स्पष्ट है कि किसी कार्य के प्रसिद्ध कारण के अभाव में उसके अन्य कारण की कल्पना को जो दण्डी ने विभावना में वाञ्छनीय बताया था, उसीका अवलम्ब लेकर रुद्रट ने अन्य वस्तु-धर्म के अन्यत्र सद्भाव-वर्णन में विभावना के एक प्रकार की कल्पना कर ली। दण्डी ने समाधि गुण में अन्य वस्तु-धर्म का अन्यत्र आधान वाञ्छनीय माना है। विभावना के तृतीय भेद की कल्पना में उक्त समाधि-धारणा का भी योग जान पड़ता है। सहोक्ति
वास्तव-वर्गगत सहोक्ति अलङ्कार के तीन स्वरूपों का विवेचन रुद्रट ने किया है। भामह, दण्डी आदि पूर्ववर्ती आचार्यों की सहोक्ति-विषयक मान्यता से रुद्रट की तद्विषयक मान्यता इस दृष्टि से अभिन्न मानी जा सकती है कि वे भी भामह दण्डी आदि की तरह दो वस्तुओं के धर्म का सह-कथन सहोक्ति में आवश्यक मानते हैं। उभयनिष्ठ धर्मों की एक साथ उक्ति के कारण इस अलङ्कार की संज्ञा अन्वर्था है। भामह ने केवल क्रिया सहोक्ति का उल्लेख किया था; किन्तु दण्डी ने गुण, क्रिया, द्रव्य आदि की सह-उक्ति की कल्पना कर उसके अनेक भेद स्वीकार किये। रुद्रट की सहोक्ति-धारणा पर उक्त आचार्यों की मान्यता का प्रभूत प्रभाव पड़ा है। रुद्रट के 'काव्यालङ्कार' में विवेचित सहोक्ति के तीन लक्षण निम्नलिखित हैं :
(१) कोई कतृ भूत या प्रधान अर्थ जिस गुण से युक्त हो, उसी गुण से १. रुद्रट-काव्यालङ्कार, ६,२१