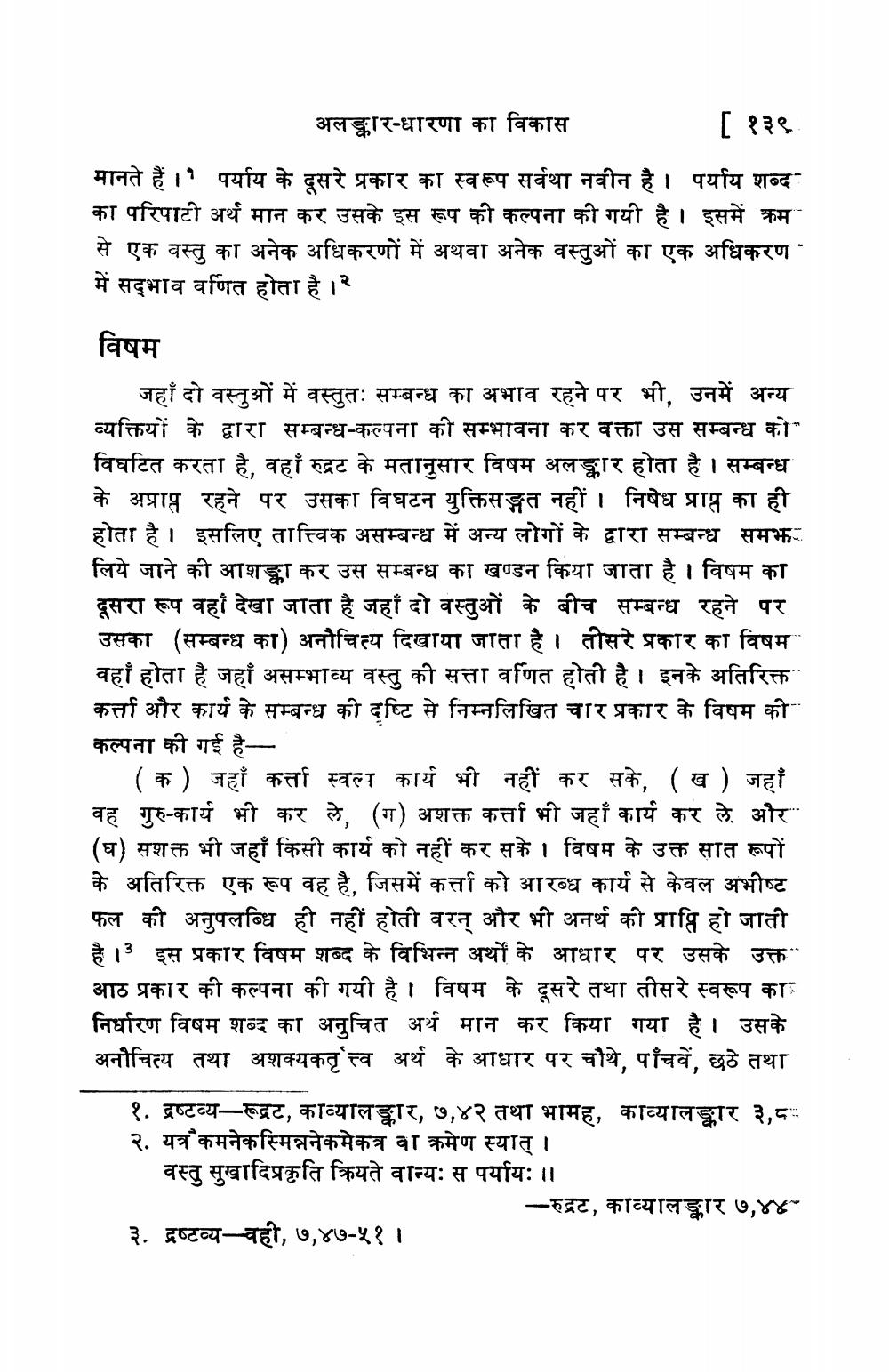________________
अलङ्कार-धारणा का विकास
[ १३९ मानते हैं। पर्याय के दूसरे प्रकार का स्वरूप सर्वथा नवीन है। पर्याय शब्द का परिपाटी अर्थ मान कर उसके इस रूप की कल्पना की गयी है। इसमें क्रम से एक वस्तु का अनेक अधिकरणों में अथवा अनेक वस्तुओं का एक अधिकरण में सद्भाव वर्णित होता है ।।
विषम
जहाँ दो वस्तुओं में वस्तुतः सम्बन्ध का अभाव रहने पर भी, उनमें अन्य व्यक्तियों के द्वारा सम्बन्ध-कल्पना की सम्भावना कर वक्ता उस सम्बन्ध को" विघटित करता है, वहाँ रुद्रट के मतानुसार विषम अलङ्कार होता है। सम्बन्ध के अप्राप्त रहने पर उसका विघटन युक्तिसङ्गत नहीं। निषेध प्राप्त का ही होता है। इसलिए तात्त्विक असम्बन्ध में अन्य लोगों के द्वारा सम्बन्ध समझ लिये जाने की आशङ्का कर उस सम्बन्ध का खण्डन किया जाता है। विषम का दूसरा रूप वहाँ देखा जाता है जहाँ दो वस्तुओं के बीच सम्बन्ध रहने पर उसका (सम्बन्ध का) अनौचित्य दिखाया जाता है। तीसरे प्रकार का विषम वहाँ होता है जहाँ असम्भाव्य वस्तु की सत्ता वणित होती है। इनके अतिरिक्त कर्ता और कार्य के सम्बन्ध की दृष्टि से निम्नलिखित चार प्रकार के विषम की कल्पना की गई है
(क) जहाँ कर्ता स्वल कार्य भी नहीं कर सके, (ख ) जहाँ वह गुरु-कार्य भी कर ले, (ग) अशक्त कर्ता भी जहाँ कार्य कर ले. और (घ) सशक्त भी जहाँ किसी कार्य को नहीं कर सके । विषम के उक्त सात रूपों के अतिरिक्त एक रूप वह है, जिसमें कर्ता को आरब्ध कार्य से केवल अभीष्ट फल की अनुपलब्धि ही नहीं होती वरन् और भी अनर्थ की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार विषम शब्द के विभिन्न अर्थों के आधार पर उसके उक्त" आठ प्रकार की कल्पना की गयी है। विषम के दूसरे तथा तीसरे स्वरूप का निर्धारण विषम शब्द का अनुचित अर्थ मान कर किया गया है। उसके अनौचित्य तथा अशक्यकर्तृत्त्व अर्थ के आधार पर चौथे, पांचवें, छठे तथा
१. द्रष्टव्य-रूद्रट, काव्यालङ्कार, ७,४२ तथा भामह, काव्यालङ्कार ३,८२. यत्र कमनेकस्मिन्ननेकमेकत्र वा क्रमेण स्यात् । वस्तु सुखादिप्रकृति क्रियते वान्यः स पर्यायः ।।
-रुद्रट, काव्यालङ्कार ७,४४० ३. द्रष्टव्य-वही, ७,४७-५१ ।