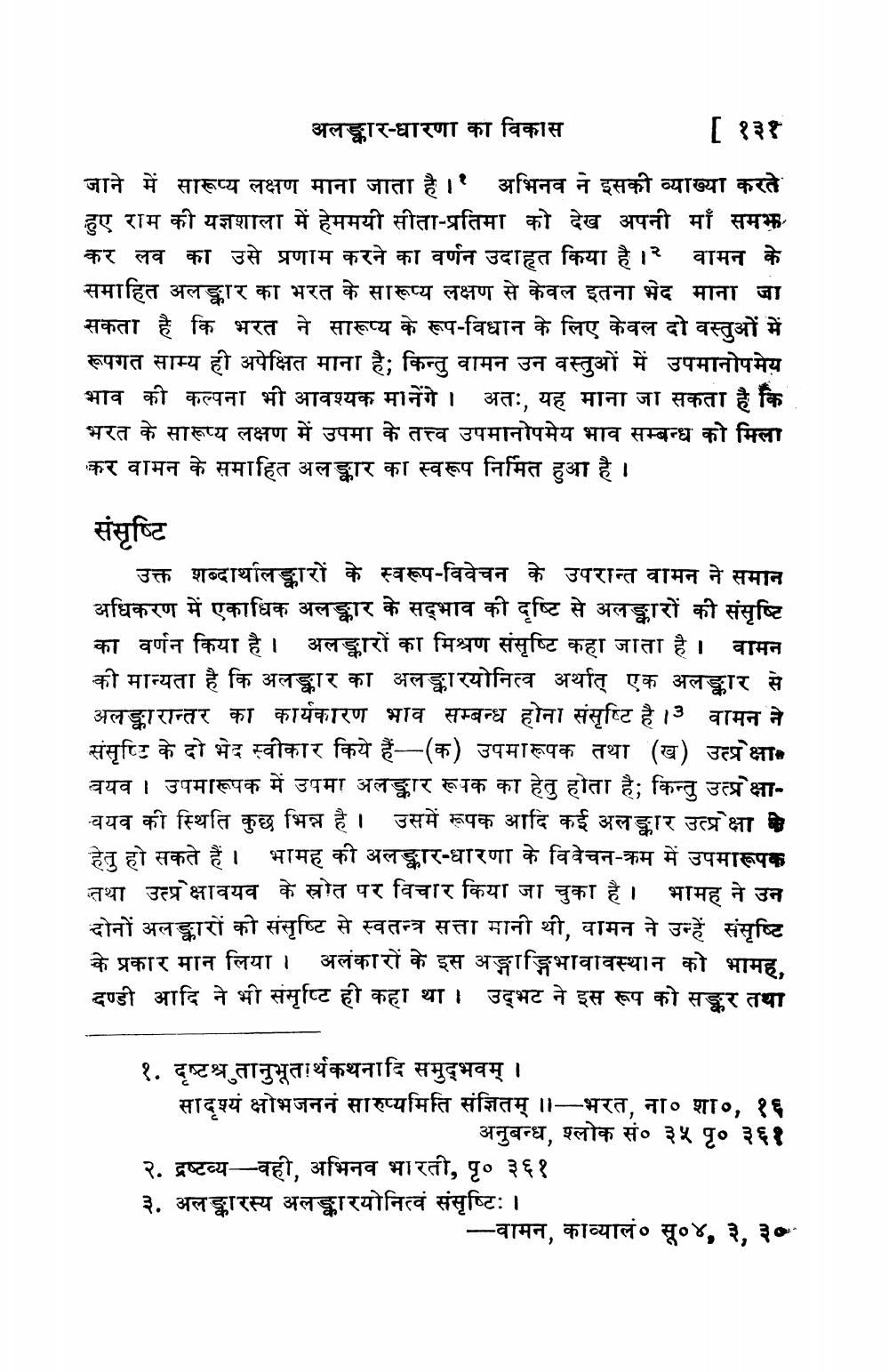________________
अलङ्कार-धारणा का विकास
[ १३१ जाने में सारूप्य लक्षण माना जाता है।' अभिनव ने इसकी व्याख्या करते हुए राम की यज्ञशाला में हेममयी सीता-प्रतिमा को देख अपनी माँ समझ कर लव का उसे प्रणाम करने का वर्णन उदाहृत किया है ।२ वामन के समाहित अलङ्कार का भरत के सारूप्य लक्षण से केवल इतना भेद माना जा सकता है कि भरत ने सारूप्य के रूप-विधान के लिए केवल दो वस्तुओं में रूपगत साम्य ही अपेक्षित माना है; किन्तु वामन उन वस्तुओं में उपमानोपमेय भाव की कल्पना भी आवश्यक मानेंगे। अतः, यह माना जा सकता है कि भरत के सारूप्य लक्षण में उपमा के तत्त्व उपमानोपमेय भाव सम्बन्ध को मिला कर वामन के समाहित अलङ्कार का स्वरूप निर्मित हुआ है ।
संसृष्टि ____ उक्त शब्दार्थालङ्कारों के स्वरूप-विवेचन के उपरान्त वामन ने समान अधिकरण में एकाधिक अलङ्कार के सद्भाव की दृष्टि से अलङ्कारों की संसृष्टि का वर्णन किया है। अलङ्कारों का मिश्रण संसृष्टि कहा जाता है। वामन की मान्यता है कि अलङ्कार का अलङ्कारयोनित्व अर्थात् एक अलङ्कार से अलङ्कारान्तर का कार्यकारण भाव सम्बन्ध होना संसृष्टि है। वामन ने संसृष्टि के दो भेद स्वीकार किये हैं—(क) उपमारूपक तथा (ख) उत्प्रेक्षा वयव । उपमारूपक में उपमा अलङ्कार रूपक का हेतु होता है; किन्तु उत्प्रेक्षावयव की स्थिति कुछ भिन्न है। उसमें रूपक आदि कई अलङ्कार उत्प्रेक्षा के हेत हो सकते हैं। भामह की अलङ्कार-धारणा के विवेचन-क्रम में उपमारूपक तथा उत्प्रेक्षावयव के स्रोत पर विचार किया जा चुका है। भामह ने उन दोनों अलङ्कारों को संसृष्टि से स्वतन्त्र सत्ता मानी थी, वामन ने उन्हें संसृष्टि के प्रकार मान लिया। अलंकारों के इस अङ्गाङ्गिभावावस्थान को भामह, दण्डी आदि ने भी संसृष्टि ही कहा था। उद्भट ने इस रूप को सङ्कर तथा
१. दृष्टश्र तानुभूतार्थकथनादि समुद्भवम् । ___ सादृश्यं क्षोभजननं सारुप्यमिति संज्ञितम् ।।-भरत, ना० शा०, १६
___ अनुबन्ध, श्लोक सं० ३५ पृ० ३६१ २. द्रष्टव्य—वही, अभिनव भारती, पृ० ३६१ ३. अलङ्कारस्य अलङ्कारयोनित्वं संसृष्टिः ।
-वामन, काव्यालं० सू०४, ३, ३०