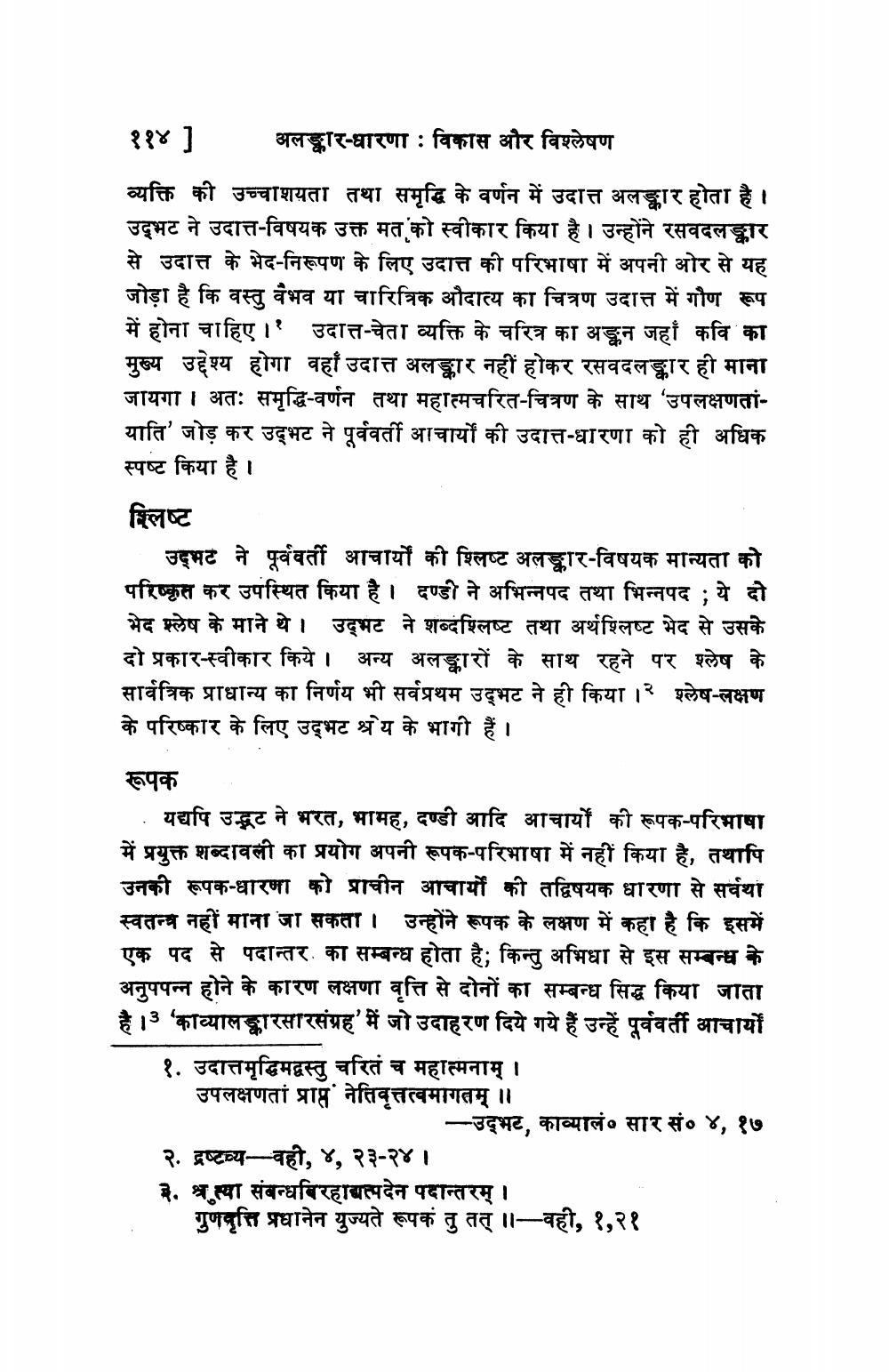________________
११४ ] अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण व्यक्ति की उच्चाशयता तथा समृद्धि के वर्णन में उदात्त अलङ्कार होता है। उद्भट ने उदात्त-विषयक उक्त मत को स्वीकार किया है। उन्होंने रसवदलङ्कार से उदात्त के भेद-निरूपण के लिए उदात्त की परिभाषा में अपनी ओर से यह जोड़ा है कि वस्तु वैभव या चारित्रिक औदात्य का चित्रण उदात्त में गौण रूप में होना चाहिए। उदात्त-चेता व्यक्ति के चरित्र का अङ्कन जहाँ कवि का मुख्य उद्देश्य होगा वहाँ उदात्त अलङ्कार नहीं होकर रसवदलङ्कार ही माना जायगा । अतः समृद्धि-वर्णन तथा महात्मचरित-चित्रण के साथ 'उपलक्षणतांयाति' जोड़ कर उद्भट ने पूर्ववर्ती आचार्यों की उदात्त-धारणा को ही अधिक स्पष्ट किया है। श्लिष्ट
उद्भट ने पूर्ववर्ती आचार्यों की श्लिष्ट अलङ्कार-विषयक मान्यता को परिष्कृत कर उपस्थित किया है। दण्डी ने अभिन्नपद तथा भिन्नपद ; ये दो भेद श्लेष के माने थे। उद्भट ने शब्दश्लिष्ट तथा अर्थश्लिष्ट भेद से उसके दो प्रकार-स्वीकार किये। अन्य अलङ्कारों के साथ रहने पर श्लेष के सार्वत्रिक प्राधान्य का निर्णय भी सर्वप्रथम उद्भट ने ही किया ।२ श्लेष-लक्षण के परिष्कार के लिए उद्भट श्रेय के भागी हैं।
रूपक
. यद्यपि उद्भट ने भरत, भामह, दण्डी आदि आचार्यों की रूपक-परिभाषा में प्रयुक्त शब्दावली का प्रयोग अपनी रूपक-परिभाषा में नहीं किया है, तथापि उनकी रूपक-धारणा को प्राचीन आचार्यों की तद्विषयक धारणा से सर्वथा स्वतन्त्र नहीं माना जा सकता। उन्होंने रूपक के लक्षण में कहा है कि इसमें एक पद से पदान्तर. का सम्बन्ध होता है; किन्तु अभिधा से इस सम्बन्ध के अनुपपन्न होने के कारण लक्षणा वृत्ति से दोनों का सम्बन्ध सिद्ध किया जाता है।3 'काव्यालङ्कारसारसंग्रह' में जो उदाहरण दिये गये हैं उन्हें पूर्ववर्ती आचार्यों १. उदात्तमृद्धिमद्वस्तु चरितं च महात्मनाम् । उपलक्षणतां प्राप्त नेतिवृत्तत्वमागतम् ॥
-उद्भट, काव्यालं. सार सं० ४, १७ २. द्रष्टव्य-वही, ४, २३-२४ । ३. त्या संबन्धबिरहाद्यपदेन पदान्तरम् ।
गुणवृत्ति प्रधानेन युज्यते रूपकं तु तत् ॥-वही, १,२१