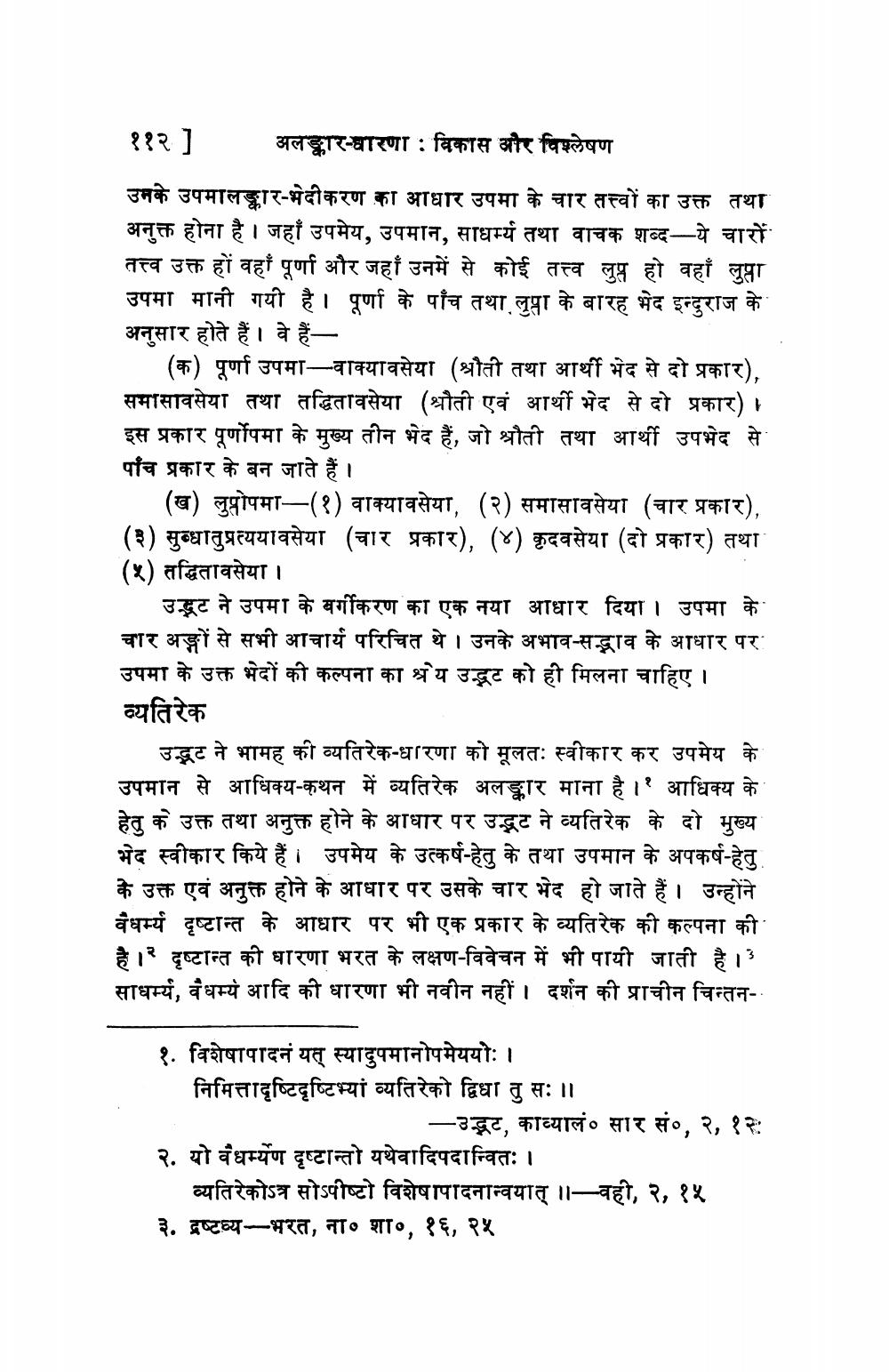________________
११२ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
उनके उपमालङ्कार-भेदीकरण का आधार उपमा के चार तत्त्वों का उक्त तथा अनुक्त होना है । जहाँ उपमेय, उपमान, साधर्म्य तथा वाचक शब्द – ये चारों तत्त्व उक्त हों वहाँ पूर्णा और जहाँ उनमें से कोई तत्त्व लुप्त हो वहाँ लुप्त उपमा मानी गयी है । पूर्णा के पाँच तथा लुप्ता के बारह भेद इन्दुराज के अनुसार होते हैं । वे हैं—
(क) पूर्णा उपमा - वाक्यावसेया ( श्रौती तथा आर्थी भेद से दो प्रकार), समासावसेया तथा तद्धितावसेया ( श्रौती एवं आर्थी भेद से दो प्रकार ) । इस प्रकार पूर्णोपमा के मुख्य तीन भेद हैं, जो श्रौती तथा आर्थी उपभेद से पाँच प्रकार के बन जाते हैं ।
(ख) लुप्तोपमा - ( १ ) वाक्यावसेया, (२) समासावसेया ( चार प्रकार ), (३) सुब्धातुप्रत्ययावसेया ( चार प्रकार ), (४) कृदवसेया ( दो प्रकार ) तथा (५) तद्धितावसेया ।
उद्भट ने उपमा के वर्गीकरण का एक नया आधार दिया । उपमा के चार अङ्गों से सभी आचार्य परिचित थे । उनके अभाव -सद्भाव के आधार पर उपमा के उक्त भेदों की कल्पना का श्रेय उद्भट को ही मिलना चाहिए । व्यतिरेक
उद्भट ने भामह की व्यतिरेक-धारणा को मूलतः स्वीकार कर उपमेय के उपमान से आधिक्य - कथन में व्यतिरेक अलङ्कार माना है ।' आधिक्य के हेतु के उक्त तथा अनुक्त होने के आधार पर उद्भट ने व्यतिरेक के दो मुख्य भेद स्वीकार किये हैं । उपमेय के उत्कर्ष - हेतु के तथा उपमान के अपकर्ष - हेतु. के उक्त एवं अनुक्त होने के आधार पर उसके चार भेद हो जाते हैं । उन्होंने वैधर्म्य दृष्टान्त के आधार पर भी एक प्रकार के व्यतिरेक की कल्पना की है । दृष्टान्त की धारणा भरत के लक्षण - विवेचन में भी पायी जाती है । 3 साधर्म्य, वैधर्म्य आदि की धारणा भी नवीन नहीं । दर्शन की प्राचीन चिन्तन-
१. विशेषापादनं यत् स्यादुपमानोपमेययोः । निमित्त दृष्टिदृष्टिभ्यां व्यतिरेको द्विधा तु सः ॥
- उद्भट, काव्यालं० सार सं०, २, १२:
२. यो वैधर्म्येण दृष्टान्तो यथेवादिपदान्वितः ।
व्यतिरेकोऽत्र सोऽपीष्टो विशेषापादनान्वयात् ॥ - वही, २, १५
३. द्रष्टव्य - भरत, ना० शा०, १६, २५