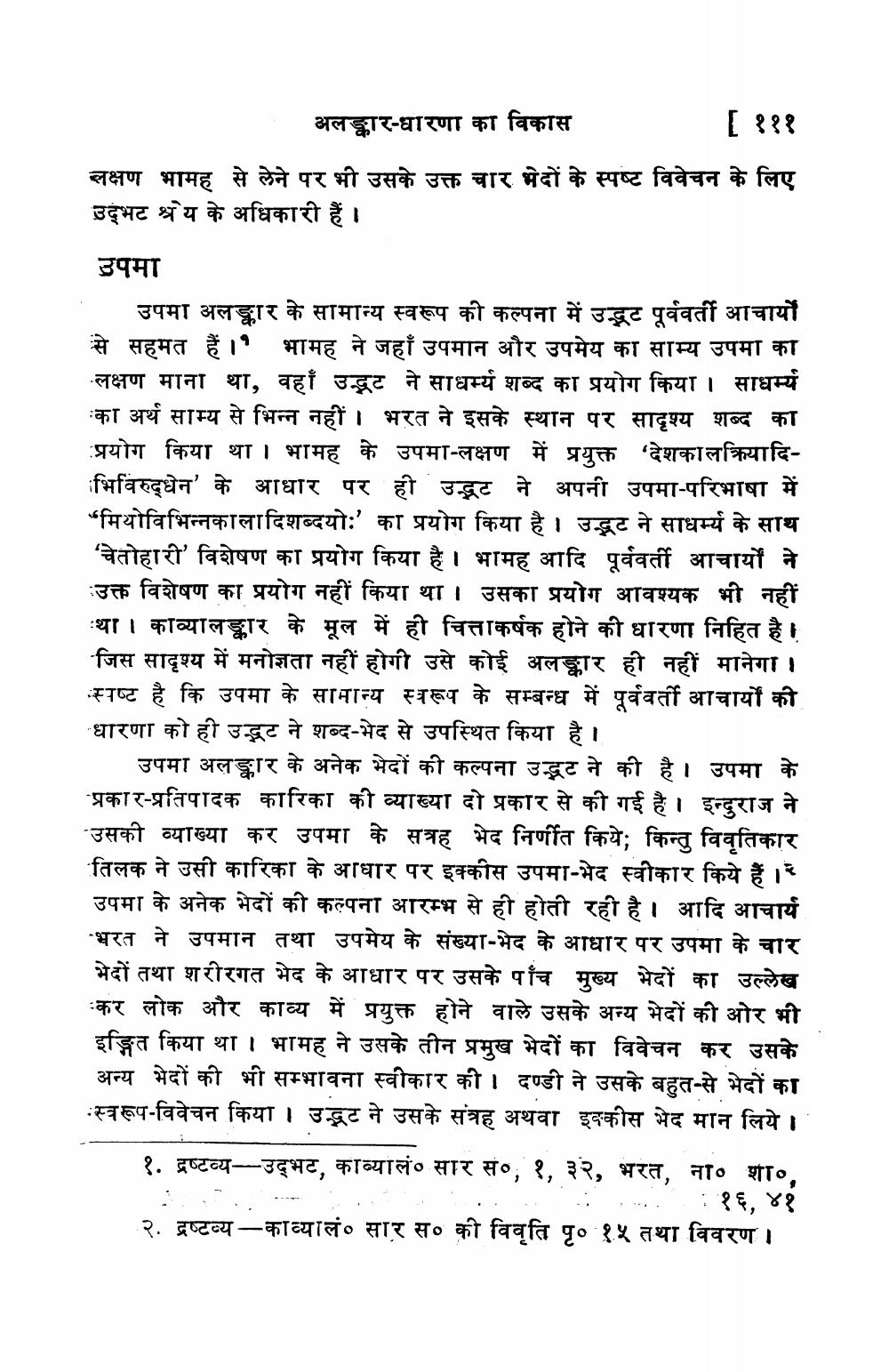________________
अलङ्कार-धारणा का विकास
[ १११
लक्षण भामह से लेने पर भी उसके उक्त चार भेदों के स्पष्ट विवेचन के लिए उद्भट श्रेय के अधिकारी हैं ।
उपमा
उपमा अलङ्कार के सामान्य स्वरूप की कल्पना में उद्भट पूर्ववर्ती आचार्यों से सहमत हैं।' भामह ने जहाँ उपमान और उपमेय का साम्य उपमा का लक्षण माना था, वहाँ उद्भट ने साधर्म्य शब्द का प्रयोग किया। साधर्म्य का अर्थ साम्य से भिन्न नहीं। भरत ने इसके स्थान पर सादृश्य शब्द का प्रयोग किया था। भामह के उपमा-लक्षण में प्रयुक्त 'देशकालक्रियादिभिविरुद्धन' के आधार पर ही उद्भट ने अपनी उपमा-परिभाषा में “मियोविभिन्नकालादिशब्दयोः' का प्रयोग किया है। उद्भट ने साधर्म्य के साथ 'चेतोहारी' विशेषण का प्रयोग किया है। भामह आदि पूर्ववर्ती आचार्यों ने उक्त विशेषण का प्रयोग नहीं किया था। उसका प्रयोग आवश्यक भी नहीं था। काव्यालङ्कार के मूल में ही चित्ताकर्षक होने की धारणा निहित है। 'जिस सादृश्य में मनोज्ञता नहीं होगी उसे कोई अलङ्कार ही नहीं मानेगा। स्पष्ट है कि उपमा के सामान्य स्वरूप के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती आचार्यों की धारणा को ही उद्भट ने शब्द-भेद से उपस्थित किया है।
उपमा अलङ्कार के अनेक भेदों की कल्पना उद्भट ने की है। उपमा के प्रकार-प्रतिपादक कारिका की व्याख्या दो प्रकार से की गई है। इन्दुराज ने उसकी व्याख्या कर उपमा के सत्रह भेद निर्णीत किये; किन्तु विवृतिकार तिलक ने उसी कारिका के आधार पर इक्कीस उपमा-भेद स्वीकार किये हैं। उपमा के अनेक भेदों की कल्पना आरम्भ से ही होती रही है। आदि आचार्य भरत ने उपमान तथा उपमेय के संख्या-भेद के आधार पर उपमा के चार भेदों तथा शरीरगत भेद के आधार पर उसके पाँच मुख्य भेदों का उल्लेख कर लोक और काव्य में प्रयुक्त होने वाले उसके अन्य भेदों की ओर भी इङ्गित किया था। भामह ने उसके तीन प्रमुख भेदों का विवेचन कर उसके अन्य भेदों की भी सम्भावना स्वीकार की। दण्डी ने उसके बहुत-से भेदों का स्वरूप-विवेचन किया। उद्भट ने उसके संत्रह अथवा इक्कीस भेद मान लिये।
१. द्रष्टव्य-उद्भट, काव्यालं० सार स०, १, ३२, भरत, ना० शा०,
२. द्रष्टव्य – काव्यालं० सार स० की विवृति पृ० १५ तथा विवरण।