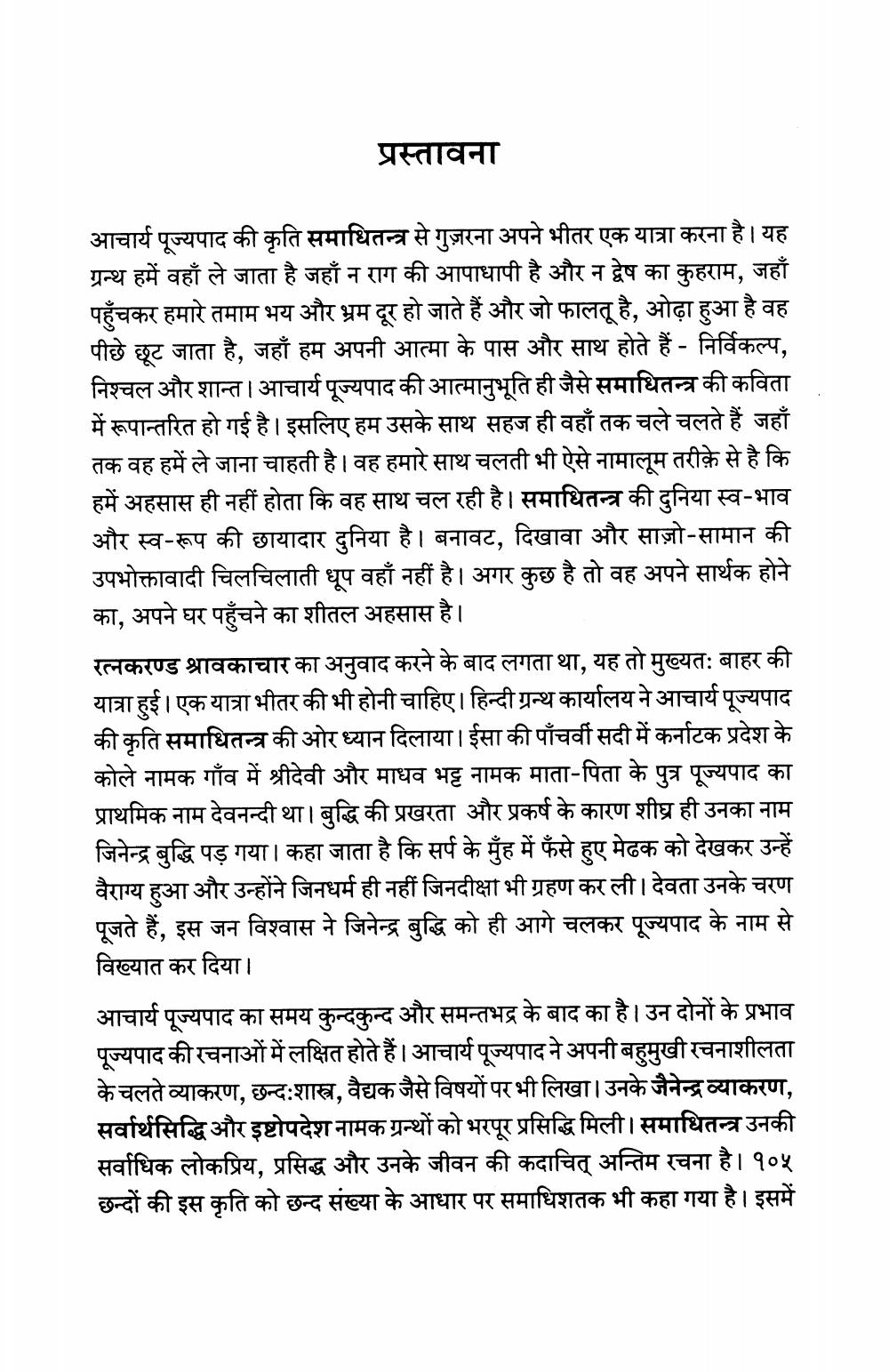________________
प्रस्तावना
आचार्य पूज्यपाद की कृति समाधितन्त्र से गुज़रना अपने भीतर एक यात्रा करना है। यह ग्रन्थ हमें वहाँ ले जाता है जहाँ न राग की आपाधापी है और न द्वेष का कुहराम, जहाँ पहुँचकर हमारे तमाम भय और भ्रम दूर हो जाते हैं और जो फालतू है, ओढ़ा हुआ है वह पीछे छूट जाता है, जहाँ हम अपनी आत्मा के पास और साथ होते हैं - निर्विकल्प, निश्चल और शान्त । आचार्य पूज्यपाद की आत्मानुभूति ही जैसे समाधितन्त्र की कविता में रूपान्तरित हो गई है। इसलिए हम उसके साथ सहज ही वहाँ तक चले चलते हैं जहाँ तक वह हमें ले जाना चाहती है। वह हमारे साथ चलती भी ऐसे नामालूम तरीके से है कि हमें अहसास ही नहीं होता कि वह साथ चल रही है। समाधितन्त्र की दुनिया स्व-भाव
और स्व-रूप की छायादार दुनिया है। बनावट, दिखावा और साजो-सामान की उपभोक्तावादी चिलचिलाती धूप वहाँ नहीं है। अगर कुछ है तो वह अपने सार्थक होने का, अपने घर पहुँचने का शीतल अहसास है। रत्नकरण्ड श्रावकाचार का अनुवाद करने के बाद लगता था, यह तो मुख्यत: बाहर की यात्रा हुई। एक यात्रा भीतर की भी होनी चाहिए। हिन्दी ग्रन्थ कार्यालय ने आचार्य पूज्यपाद की कृति समाधितन्त्र की ओर ध्यान दिलाया। ईसा की पाँचवीं सदी में कर्नाटक प्रदेश के कोले नामक गाँव में श्रीदेवी और माधव भट्ट नामक माता-पिता के पुत्र पूज्यपाद का प्राथमिक नाम देवनन्दी था। बुद्धि की प्रखरता और प्रकर्ष के कारण शीघ्र ही उनका नाम जिनेन्द्र बुद्धि पड़ गया। कहा जाता है कि सर्प के मुँह में फँसे हुए मेढक को देखकर उन्हें वैराग्य हुआ और उन्होंने जिनधर्म ही नहीं जिनदीक्षा भी ग्रहण कर ली। देवता उनके चरण पूजते हैं, इस जन विश्वास ने जिनेन्द्र बुद्धि को ही आगे चलकर पूज्यपाद के नाम से विख्यात कर दिया।
आचार्य पूज्यपाद का समय कुन्दकुन्द और समन्तभद्र के बाद का है। उन दोनों के प्रभाव पूज्यपाद की रचनाओं में लक्षित होते हैं। आचार्य पूज्यपाद ने अपनी बहुमुखी रचनाशीलता के चलते व्याकरण, छन्दःशास्त्र, वैद्यक जैसे विषयों पर भी लिखा। उनके जैनेन्द्र व्याकरण, सर्वार्थसिद्धि और इष्टोपदेश नामक ग्रन्थों को भरपूर प्रसिद्धि मिली। समाधितन्त्र उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय, प्रसिद्ध और उनके जीवन की कदाचित् अन्तिम रचना है। १०५ छन्दों की इस कृति को छन्द संख्या के आधार पर समाधिशतक भी कहा गया है। इसमें