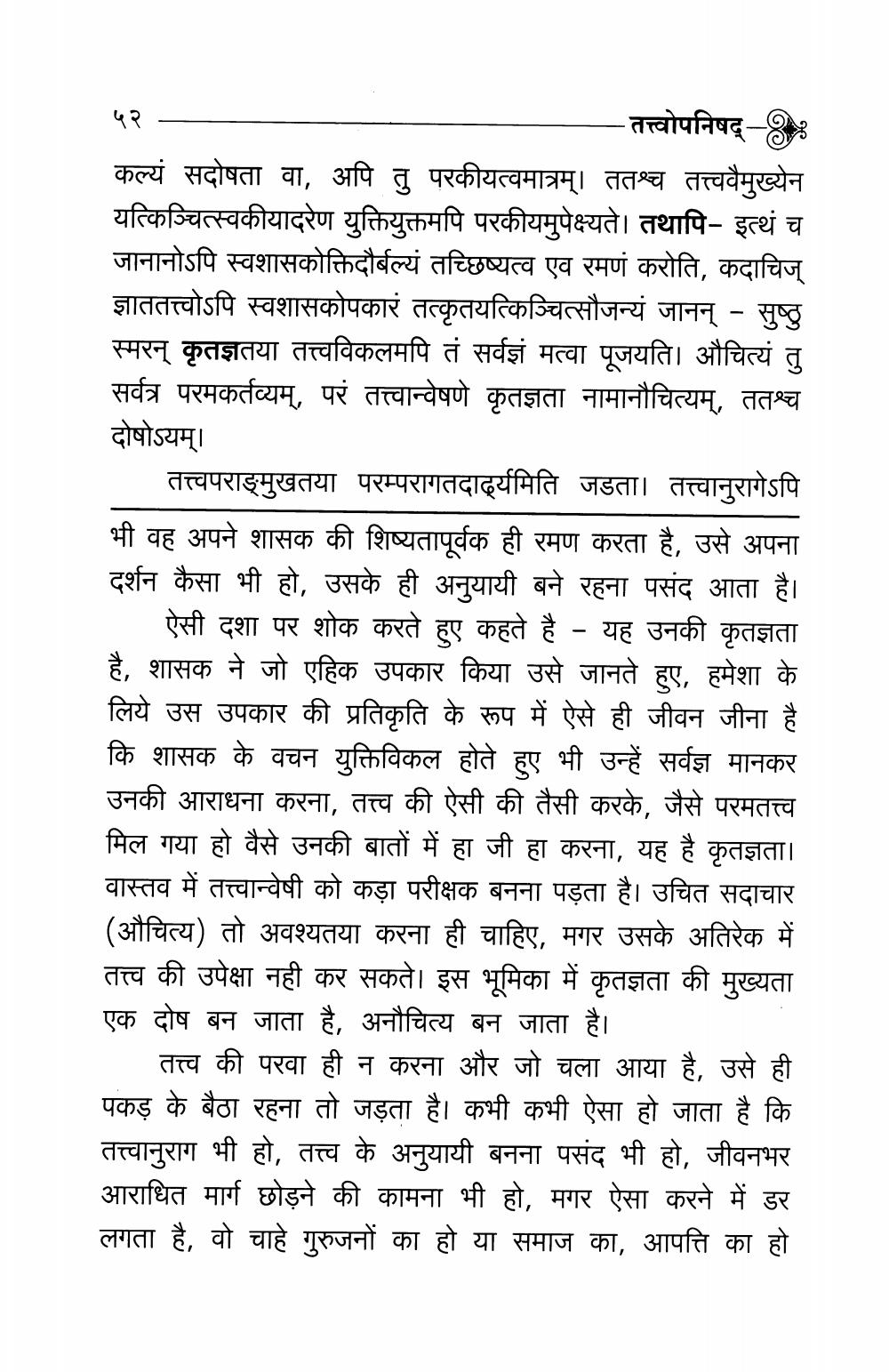________________
५२
-तत्त्वोपनिषद्कल्यं सदोषता वा, अपि तु परकीयत्वमात्रम्। ततश्च तत्त्ववैमुख्येन यत्किञ्चित्स्वकीयादरेण युक्तियुक्तमपि परकीयमुपेक्ष्यते। तथापि- इत्थं च जानानोऽपि स्वशासकोक्तिदौर्बल्यं तच्छिष्यत्व एव रमणं करोति, कदाचिज् ज्ञाततत्त्वोऽपि स्वशासकोपकारं तत्कृतयत्किञ्चित्सौजन्यं जानन् - सुष्ठु स्मरन् कृतज्ञतया तत्त्वविकलमपि तं सर्वज्ञं मत्वा पूजयति। औचित्यं तु सर्वत्र परमकर्तव्यम्, परं तत्त्वान्वेषणे कृतज्ञता नामानौचित्यम्, ततश्च दोषोऽयम्। ___ तत्त्वपराङ्मुखतया परम्परागतदायमिति जडता। तत्त्वानुरागेऽपि भी वह अपने शासक की शिष्यतापूर्वक ही रमण करता है, उसे अपना दर्शन कैसा भी हो, उसके ही अनुयायी बने रहना पसंद आता है। __ऐसी दशा पर शोक करते हुए कहते है - यह उनकी कृतज्ञता है, शासक ने जो एहिक उपकार किया उसे जानते हुए, हमेशा के लिये उस उपकार की प्रतिकृति के रूप में ऐसे ही जीवन जीना है कि शासक के वचन युक्तिविकल होते हुए भी उन्हें सर्वज्ञ मानकर उनकी आराधना करना, तत्त्व की ऐसी की तैसी करके, जैसे परमतत्त्व मिल गया हो वैसे उनकी बातों में हा जी हा करना, यह है कृतज्ञता। वास्तव में तत्त्वान्वेषी को कड़ा परीक्षक बनना पड़ता है। उचित सदाचार (औचित्य) तो अवश्यतया करना ही चाहिए, मगर उसके अतिरेक में तत्त्व की उपेक्षा नही कर सकते। इस भूमिका में कृतज्ञता की मुख्यता एक दोष बन जाता है, अनौचित्य बन जाता है।
तत्त्व की परवा ही न करना और जो चला आया है, उसे ही पकड़ के बैठा रहना तो जड़ता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तत्त्वानुराग भी हो, तत्त्व के अनुयायी बनना पसंद भी हो, जीवनभर आराधित मार्ग छोड़ने की कामना भी हो, मगर ऐसा करने में डर लगता है, वो चाहे गुरुजनों का हो या समाज का, आपत्ति का हो