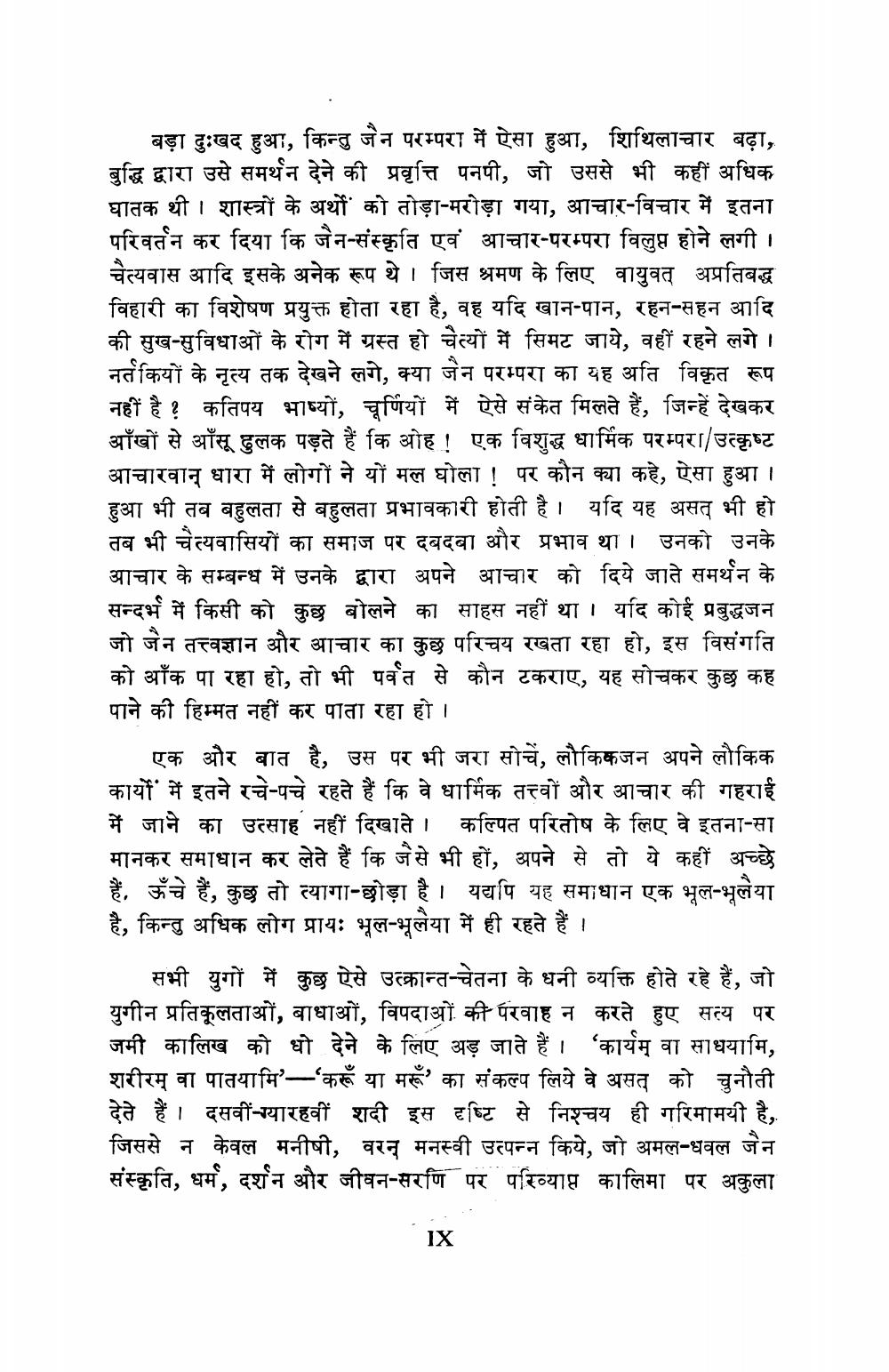________________
बड़ा दुःखद हुआ, किन्तु जैन परम्परा में ऐसा हुआ, शिथिलाचार बढ़ा, बुद्धि द्वारा उसे समर्थन देने की प्रवृत्ति पनपी, जो उससे भी कहीं अधिक घातक थी। शास्त्रों के अर्थों को तोड़ा-मरोड़ा गया, आचार-विचार में इतना परिवर्तन कर दिया कि जेन-संस्कृति एवं आचार-परम्परा विलुप्त होने लगी। चैत्यवास आदि इसके अनेक रूप थे। जिस श्रमण के लिए वायुवत् अप्रतिबद्ध विहारी का विशेषण प्रयुक्त होता रहा है, वह यदि खान-पान, रहन-सहन आदि की सुख-सुविधाओं के रोग में ग्रस्त हो चैत्यों में सिमट जाये, वहीं रहने लगे। नर्तकियों के नृत्य तक देखने लगे, क्या जैन परम्परा का यह अति विकृत रूप नहीं है ? कतिपय भाष्यों, चूर्णियों में ऐसे संकेत मिलते हैं, जिन्हें देखकर आँखों से आँसू हुलक पड़ते हैं कि ओह ! एक विशुद्ध धार्मिक परम्पररा/उत्कृष्ट आचारवान धारा में लोगों ने यो मल घोला ! पर कौन क्या कहे, ऐसा हुआ । हुआ भी तब बहुलता से बहुलता प्रभावकारी होती है। यदि यह असत् भी हो तब भी चैत्यवासियों का समाज पर दबदबा और प्रभाव था । उनको उनके आचार के सम्बन्ध में उनके द्वारा अपने आचार को दिये जाते समर्थन के सन्दर्भ में किसी को कुछ बोलने का साहस नहीं था। यदि कोई प्रबुद्धजन जो जैन तत्त्वज्ञान और आचार का कुछ परिचय रखता रहा हो, इस विसंगति को आँक पा रहा हो, तो भी पर्वत से कौन टकराए, यह सोचकर कुछ कह पाने की हिम्मत नहीं कर पाता रहा हो ।
एक और बात है, उस पर भी जरा सोचें, लौकिकजन अपने लौकिक कार्यों में इतने रचे-पचे रहते हैं कि वे धार्मिक तत्त्वों और आचार की गहराई में जाने का उत्साह नहीं दिखाते। कल्पित परितोष के लिए वे इतना-सा मानकर समाधान कर लेते हैं कि जैसे भी हों, अपने से तो ये कहीं अच्छे हैं, ऊँचे हैं, कुछ तो त्यागा-छोड़ा है। यद्यपि यह समाधान एक भूल-भूलेया है, किन्तु अधिक लोग प्रायः भूल-भूलेया में ही रहते हैं।
सभी युगों में कुछ ऐसे उत्क्रान्त-चेतना के धनी व्यक्ति होते रहे हैं, जो युगीन प्रतिकूलताओं, बाधाओं, विपदाओं की परवाह न करते हुए सत्य पर जमी कालिख को धो देने के लिए अड़ जाते हैं। 'कार्यम् वा साधयामि, शरीरम् वा पातयामि'-'करूँ या मरूँ' का संकल्प लिये वे असत् को चुनौती देते हैं। दसवीं-ग्यारहवीं शदी इस दृष्टि से निश्चय ही गरिमामयी है, जिससे न केवल मनीषी, वरन मनस्वी उत्पन्न किये, जो अमल-धवल जैन संस्कृति, धर्म, दर्शन और जीवन-सरणि पर परिव्याप्त कालिमा पर अकुला
IX