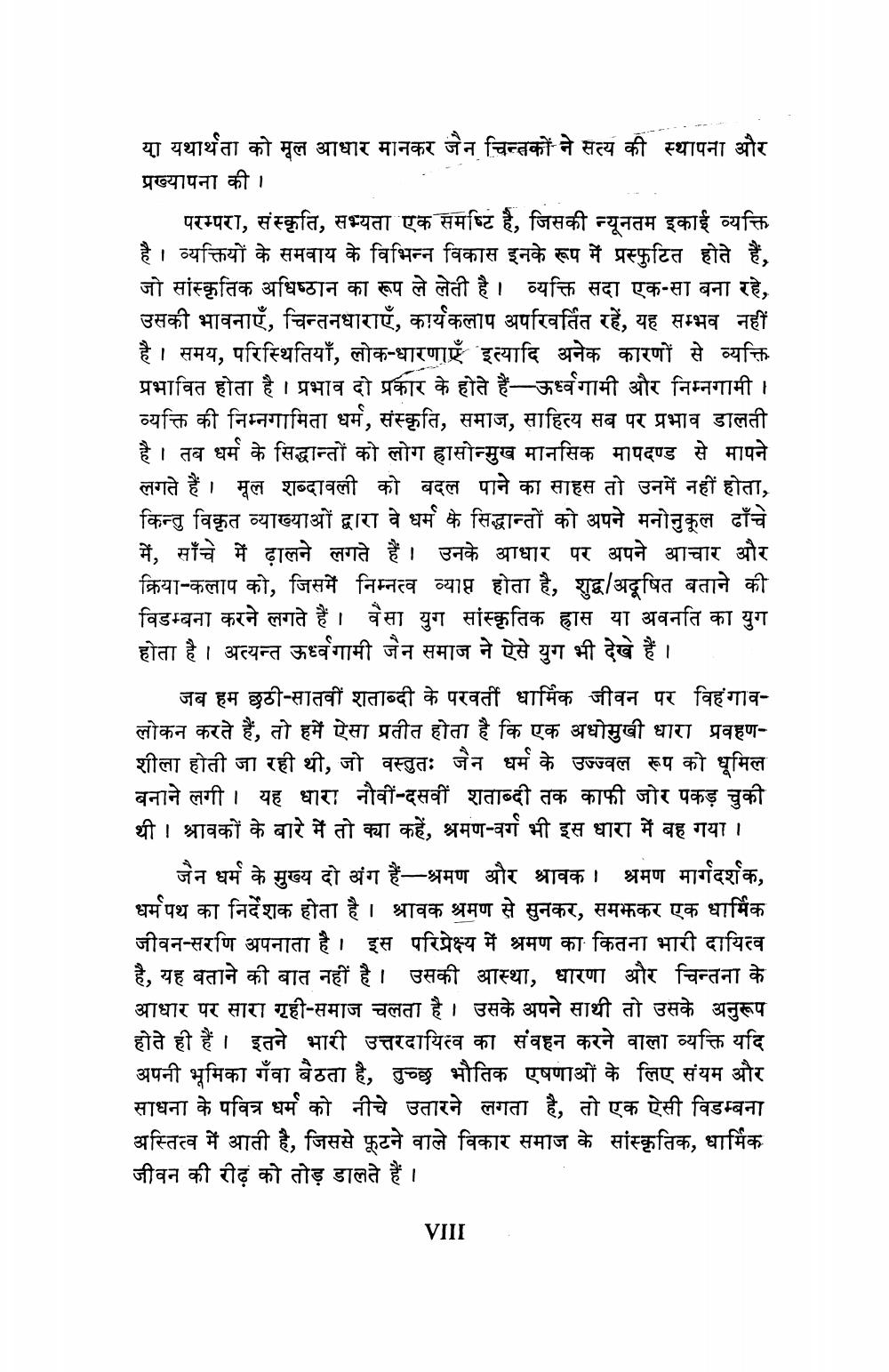________________
या यथार्थता को मूल आधार मानकर जैन चिन्तकों ने सत्य की स्थापना और प्रख्यापना की ।
परम्परा, संस्कृति, सभ्यता एक समष्टि है, जिसकी न्यूनतम इकाई व्यक्ति है । व्यक्तियों के समवाय के विभिन्न विकास इनके रूप में प्रस्फुटित होते हैं, जो सांस्कृतिक अधिष्ठान का रूप ले लेती है । व्यक्ति सदा एक-सा बना रहे, उसकी भावनाएँ, चिन्तनधाराएँ, कार्यकलाप अपरिवर्तित रहें, यह सम्भव नहीं है । समय, परिस्थितियाँ, लोक-धारणाएँ इत्यादि अनेक कारणों से व्यक्ति प्रभावित होता है । प्रभाव दो प्रकार के होते हैं— ऊर्ध्वगामी और निम्नगामी । व्यक्ति की निम्नगामिता धर्म, संस्कृति, समाज, साहित्य सब पर प्रभाव डालती है | तब धर्म के सिद्धान्तों को लोग हासोन्मुख मानसिक मापदण्ड से मापने लगते हैं । मूल शब्दावली को बदल पाने का साहस तो उनमें नहीं होता, किन्तु विकृत व्याख्याओं द्वारा वे धर्म के सिद्धान्तों को अपने मनोनुकूल ढाँचे में, साँचे में ढ़ालने लगते हैं । उनके आधार पर अपने आचार और क्रिया-कलाप को, जिसमें निम्नत्व व्याप्त होता है, शुद्ध / अदूषित बताने की विडम्बना करने लगते हैं । वैसा युग सांस्कृतिक ह्रास या अवनति का युग होता है | अत्यन्त ऊर्ध्वगामी जैन समाज ने ऐसे युग भी देखे हैं ।
जब हम छठी-सातवीं शताब्दी के परवर्ती धार्मिक जीवन पर विहंगावलोकन करते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक अधोमुखी धारा प्रवहण - शीला होती जा रही थी, जो वस्तुतः जैन धर्म के उज्ज्वल रूप को धूमिल बनाने लगी । यह धारा नौवीं दसवीं शताब्दी तक काफी जोर पकड़ चुकी थी । श्रावकों के बारे में तो क्या कहें, श्रमण-वर्ग भी इस धारा में बह गया ।
जैन धर्म के मुख्य दो अंग हैं- श्रमण और श्रावक । श्रमण मार्गदर्शक, धर्मपथ का निर्देशक होता है । श्रावक श्रमण से सुनकर, समझकर एक धार्मिक जीवन-सरणि अपनाता है । इस परिप्रेक्ष्य में श्रमण का कितना भारी दायित्व है, यह बताने की बात नहीं है । उसकी आस्था, धारणा और चिन्तना के आधार पर सारा गृही-समाज चलता है। उसके अपने साथी तो उसके अनुरूप होते ही हैं । इतने भारी उत्तरदायित्व का संवहन करने वाला व्यक्ति यदि अपनी भूमिका गँवा बैठता है, तुच्छ भौतिक एषणाओं के लिए संयम और साधना के पवित्र धर्म को नीचे उतारने लगता है, तो एक ऐसी विडम्बना अस्तित्व में आती है, जिससे फूटने वाले विकार समाज के सांस्कृतिक, धार्मिक जीवन की रीढ़ को तोड़ डालते हैं ।
VIII