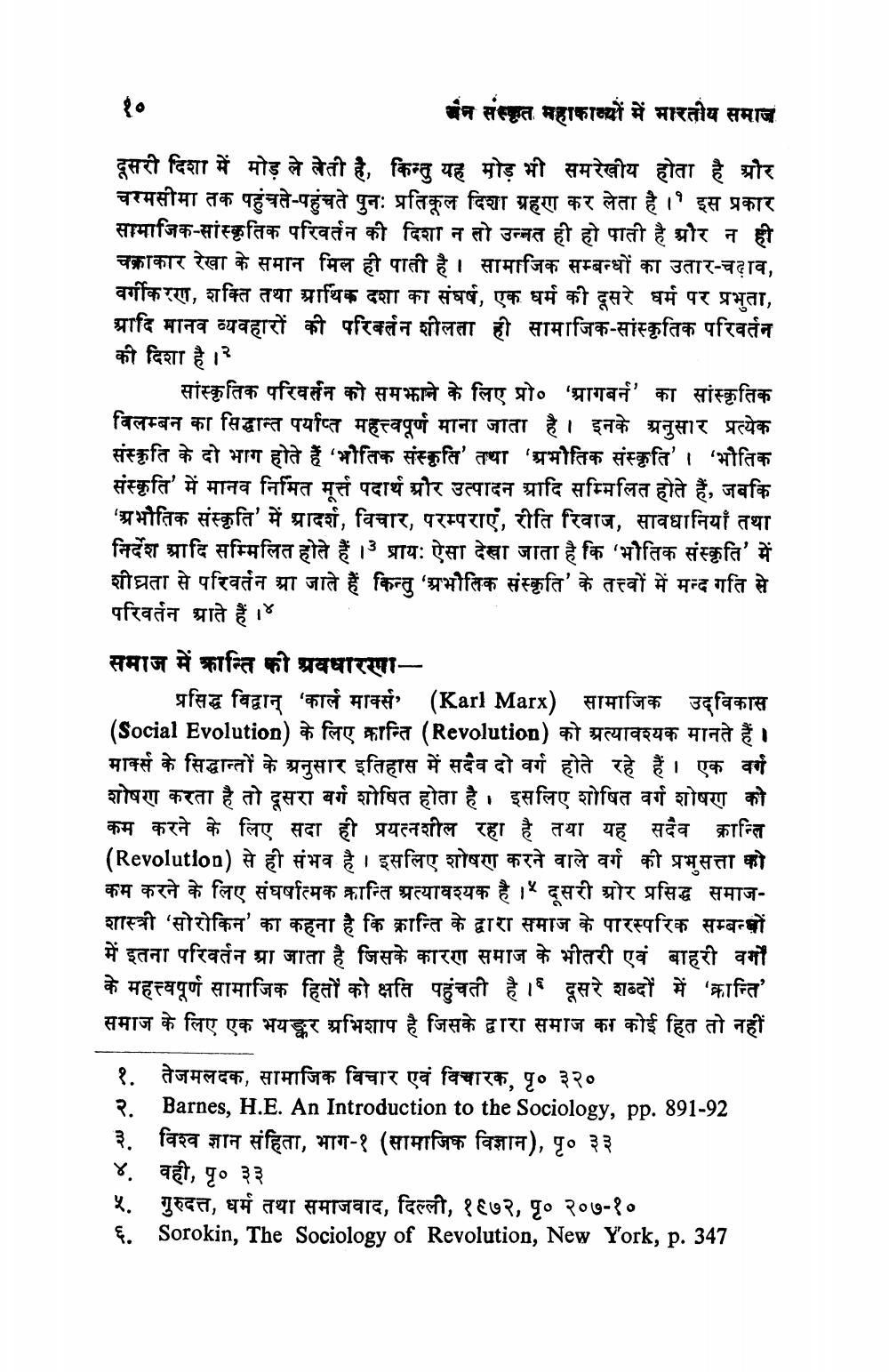________________
बन संस्कृत महाकाव्यों में भारतीय समाज
दूसरी दिशा में मोड़ ले लेती है, किन्तु यह मोड़ भी समरेखीय होता है और चरमसीमा तक पहुंचते-पहुंचते पुनः प्रतिकूल दिशा ग्रहण कर लेता है । इस प्रकार सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा न तो उन्नत ही हो पाती है और न ही चक्राकार रेखा के समान मिल ही पाती है। सामाजिक सम्बन्धों का उतार-चढ़ाव, वर्गीकरण, शक्ति तथा आर्थिक दशा का संघर्ष, एक धर्म की दूसरे धर्म पर प्रभुता, आदि मानव व्यवहारों की परिवर्तन शीलता ही सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा है ।।
सांस्कृतिक परिवर्तन को समझाने के लिए प्रो० 'पागबर्न' का सांस्कृतिक विलम्बन का सिद्धान्त पर्याप्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इनके अनुसार प्रत्येक संस्कृति के दो भाग होते हैं 'भौतिक संस्कृति' तथा 'अभौतिक संस्कृति' । 'भौतिक संस्कृति' में मानव निर्मित मूर्त पदार्थ और उत्पादन आदि सम्मिलित होते हैं, जबकि 'अभौतिक संस्कृति' में प्रादर्श, विचार, परम्पराएं, रीति रिवाज, सावधानियाँ तथा निर्देश आदि सम्मिलित होते हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि 'भौतिक संस्कृति' में शीघ्रता से परिवर्तन आ जाते हैं किन्तु 'अभौतिक संस्कृति' के तत्त्वों में मन्द गति से परिवर्तन पाते हैं । समाज में क्रान्ति की अवधारणा
प्रसिद्ध विद्वान् 'कार्ल मार्क्स' (Karl Marx) सामाजिक उद्विकास (Social Evolution) के लिए क्रान्ति (Revolution) को अत्यावश्यक मानते हैं। मार्क्स के सिद्धान्तों के अनुसार इतिहास में सदैव दो वर्ग होते रहे हैं। एक वर्ग शोषण करता है तो दूसरा बर्ग शोषित होता है। इसलिए शोषित वर्ग शोषण को कम करने के लिए सदा ही प्रयत्नशील रहा है तया यह सदैव क्रान्ति (Revolution) से ही संभव है। इसलिए शोषण करने वाले वर्ग की प्रभुसत्ता को कम करने के लिए संघर्षात्मक क्रान्ति अत्यावश्यक है। दूसरी ओर प्रसिद्ध समाजशास्त्री 'सोरोकिन' का कहना है कि क्रान्ति के द्वारा समाज के पारस्परिक सम्बन्धों में इतना परिवर्तन आ जाता है जिसके कारण समाज के भीतरी एवं बाहरी वर्गों के महत्त्वपूर्ण सामाजिक हितों को क्षति पहुंचती है। दूसरे शब्दों में 'क्रान्ति' समाज के लिए एक भयङ्कर अभिशाप है जिसके द्वारा समाज का कोई हित तो नहीं १. तेजमलदक, सामाजिक विचार एवं विचारक, पृ० ३२० २. Barnes, H.E. An Introduction to the Sociology, pp. 891-92 ३. विश्व ज्ञान संहिता, भाग-१ (सामाजिक विज्ञान), पृ० ३३ ४. वही, पृ० ३३ ५. गुरुदत्त, धर्म तथा समाजवाद, दिल्ली, १६७२, पृ० २०७-१० ६. Sorokin, The Sociology of Revolution, New York, p. 347