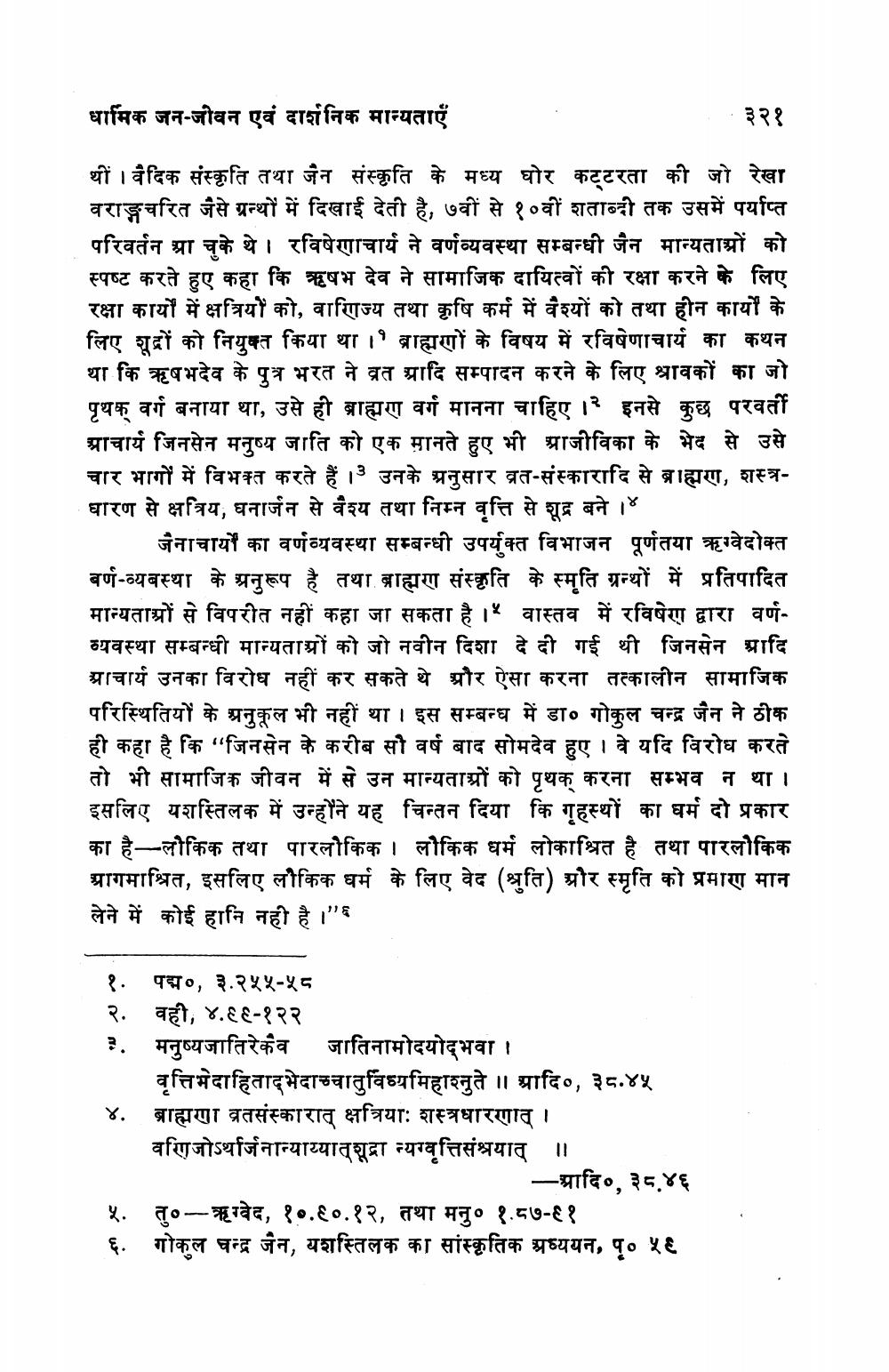________________
धार्मिक जन-जीवन एवं दार्शनिक मान्यताएं
. ३२१
थीं । वैदिक संस्कृति तथा जैन संस्कृति के मध्य घोर कट्टरता की जो रेखा वराङ्गचरित जैसे ग्रन्थों में दिखाई देती है, ७वीं से १०वीं शताब्दी तक उसमें पर्याप्त परिवर्तन आ चुके थे। रविषेणाचार्य ने वर्णव्यवस्था सम्बन्धी जैन मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि ऋषभ देव ने सामाजिक दायित्वों की रक्षा करने के लिए रक्षा कार्यों में क्षत्रियों को, वाणिज्य तथा कृषि कर्म में वैश्यों को तथा हीन कार्यों के लिए शूद्रों को नियुक्त किया था ।' ब्राह्मणों के विषय में रविषेणाचार्य का कथन था कि ऋषभदेव के पुत्र भरत ने व्रत आदि सम्पादन करने के लिए श्रावकों का जो पृथक् वर्ग बनाया था, उसे ही ब्राह्मण वर्ग मानना चाहिए ।२ इनसे कुछ परवर्ती आचार्य जिनसेन मनुष्य जाति को एक मानते हुए भी आजीविका के भेद से उसे चार भागों में विभक्त करते हैं। उनके अनुसार व्रत-संस्कारादि से ब्राह्मण, शस्त्रधारण से क्षत्रिय, धनार्जन से वैश्य तथा निम्न वृत्ति से शूद्र बने ।४
जैनाचार्यों का वर्णव्यवस्था सम्बन्धी उपर्युक्त विभाजन पूर्णतया ऋग्वेदोक्त वर्ण-व्यवस्था के अनुरूप है तथा ब्राह्मण संस्कृति के स्मृति ग्रन्थों में प्रतिपादित मान्यताओं से विपरीत नहीं कहा जा सकता है । वास्तव में रविषेण द्वारा वर्णव्यवस्था सम्बन्धी मान्यतामों को जो नवीन दिशा दे दी गई थी जिनसेन आदि प्राचार्य उनका विरोध नहीं कर सकते थे और ऐसा करना तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल भी नहीं था । इस सम्बन्ध में डा० गोकुल चन्द्र जैन ने ठीक ही कहा है कि "जिनसेन के करीब सौ वर्ष बाद सोमदेव हुए। वे यदि विरोध करते तो भी सामाजिक जीवन में से उन मान्यताओं को पृथक करना सम्भव न था। इसलिए यशस्तिलक में उन्होंने यह चिन्तन दिया कि गृहस्थों का धर्म दो प्रकार का है-लौकिक तथा पारलौकिक । लौकिक धर्म लोकाश्रित है तथा पारलौकिक आगमाश्रित, इसलिए लौकिक धर्म के लिए वेद (श्रुति) और स्मृति को प्रमाण मान लेने में कोई हानि नही है।"६
१. पद्म०, ३.२५५-५८ २. वही, ४.६६-१२२ ३. मनुष्यजातिरेकैव जातिनामोदयोद्भवा ।
वत्तिभेदाहिताभेदाच्चातुर्विध्यमिहाश्नुते ॥ आदि०, ३८.४५ ४. ब्राह्मणा व्रतसंस्कारात् क्षत्रियाः शस्त्रधारणात् ।।
वरिणजोऽर्थार्जनान्याय्यात्शूद्रा न्यग्वृत्तिसंश्रयात् ॥
-आदि०,३८.४६
५. तु०-ऋग्वेद, १०.६०.१२, तथा मनु० १.८७-६१ ६. गोकुल चन्द्र जैन, यशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ५६