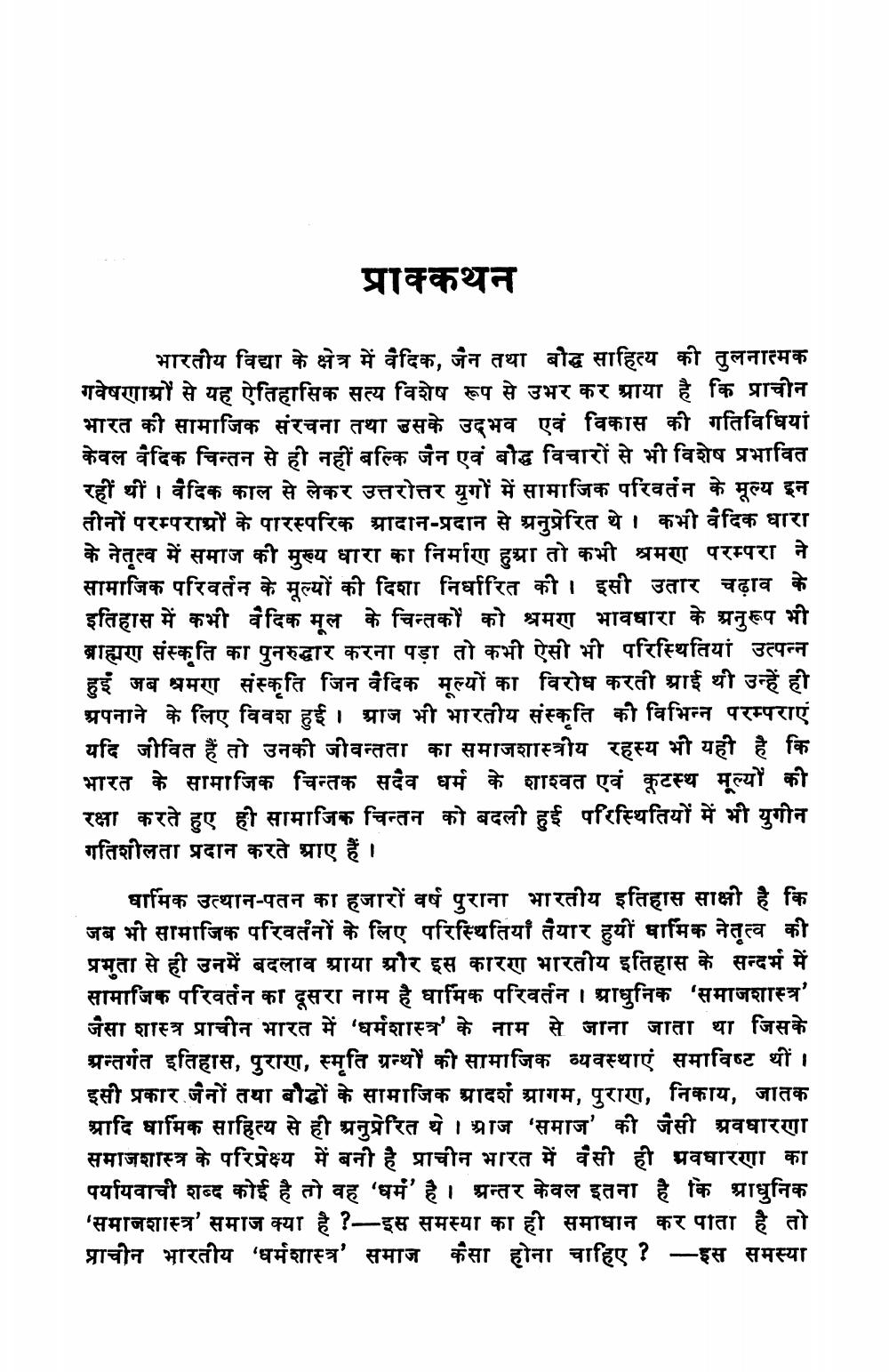________________
प्राक्कथन
भारतीय विद्या के क्षेत्र में वैदिक, जैन तथा बौद्ध साहित्य की तुलनात्मक गवेषणाओं से यह ऐतिहासिक सत्य विशेष रूप से उभर कर पाया है कि प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना तथा उसके उद्भव एवं विकास की गतिविधियां केवल वैदिक चिन्तन से ही नहीं बल्कि जैन एवं बौद्ध विचारों से भी विशेष प्रभावित रहीं थीं। वैदिक काल से लेकर उत्तरोत्तर युगों में सामाजिक परिवर्तन के मूल्य इन तीनों परम्परामों के पारस्परिक आदान-प्रदान से अनुप्रेरित थे। कभी वैदिक धारा के नेतृत्व में समाज की मुख्य धारा का निर्माण हुआ तो कभी श्रमण परम्परा ने सामाजिक परिवर्तन के मूल्यों की दिशा निर्धारित की। इसी उतार चढ़ाव के इतिहास में कभी वैदिक मूल के चिन्तकों को श्रमण भावधारा के अनुरूप भी ब्राह्मण संस्कृति का पुनरुद्धार करना पड़ा तो कभी ऐसी भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जब श्रमण संस्कृति जिन वैदिक मूल्यों का विरोध करती आई थी उन्हें ही अपनाने के लिए विवश हुई। आज भी भारतीय संस्कृति की विभिन्न परम्पराएं यदि जीवित हैं तो उनको जीवन्तता का समाजशास्त्रीय रहस्य भी यही है कि भारत के सामाजिक चिन्तक सदैव धर्म के शाश्वत एवं कूटस्थ मूल्यों की रक्षा करते हुए ही सामाजिक चिन्तन को बदली हुई परिस्थितियों में भी युगीन गतिशीलता प्रदान करते आए हैं।
धार्मिक उत्थान-पतन का हजारों वर्ष पुराना भारतीय इतिहास साक्षी है कि जब भी सामाजिक परिवर्तनों के लिए परिस्थितियां तैयार हुयीं धार्मिक नेतृत्व की प्रभुता से ही उनमें बदलाव आया और इस कारण भारतीय इतिहास के सन्दर्भ में सामाजिक परिवर्तन का दूसरा नाम है धार्मिक परिवर्तन । आधुनिक 'समाजशास्त्र' जैसा शास्त्र प्राचीन भारत में 'धर्मशास्त्र' के नाम से जाना जाता था जिसके अन्तर्गत इतिहास, पुराण, स्मृति ग्रन्थों की सामाजिक व्यवस्थाएं समाविष्ट थीं। इसी प्रकार जैनों तथा बौद्धों के सामाजिक प्रादर्श आगम, पुराण, निकाय, जातक आदि धार्मिक साहित्य से ही अनुप्रेरित थे । प्राज 'समाज' की जैसी अवधारणा समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में बनी है प्राचीन भारत में वैसी ही अवधारणा का पर्यायवाची शब्द कोई है तो वह 'धर्म' है। अन्तर केवल इतना है कि प्राधुनिक 'समानशास्त्र' समाज क्या है ?-इस समस्या का ही समाधान कर पाता है तो प्राचीन भारतीय 'धर्मशास्त्र' समाज कैसा होना चाहिए ? -इस समस्या