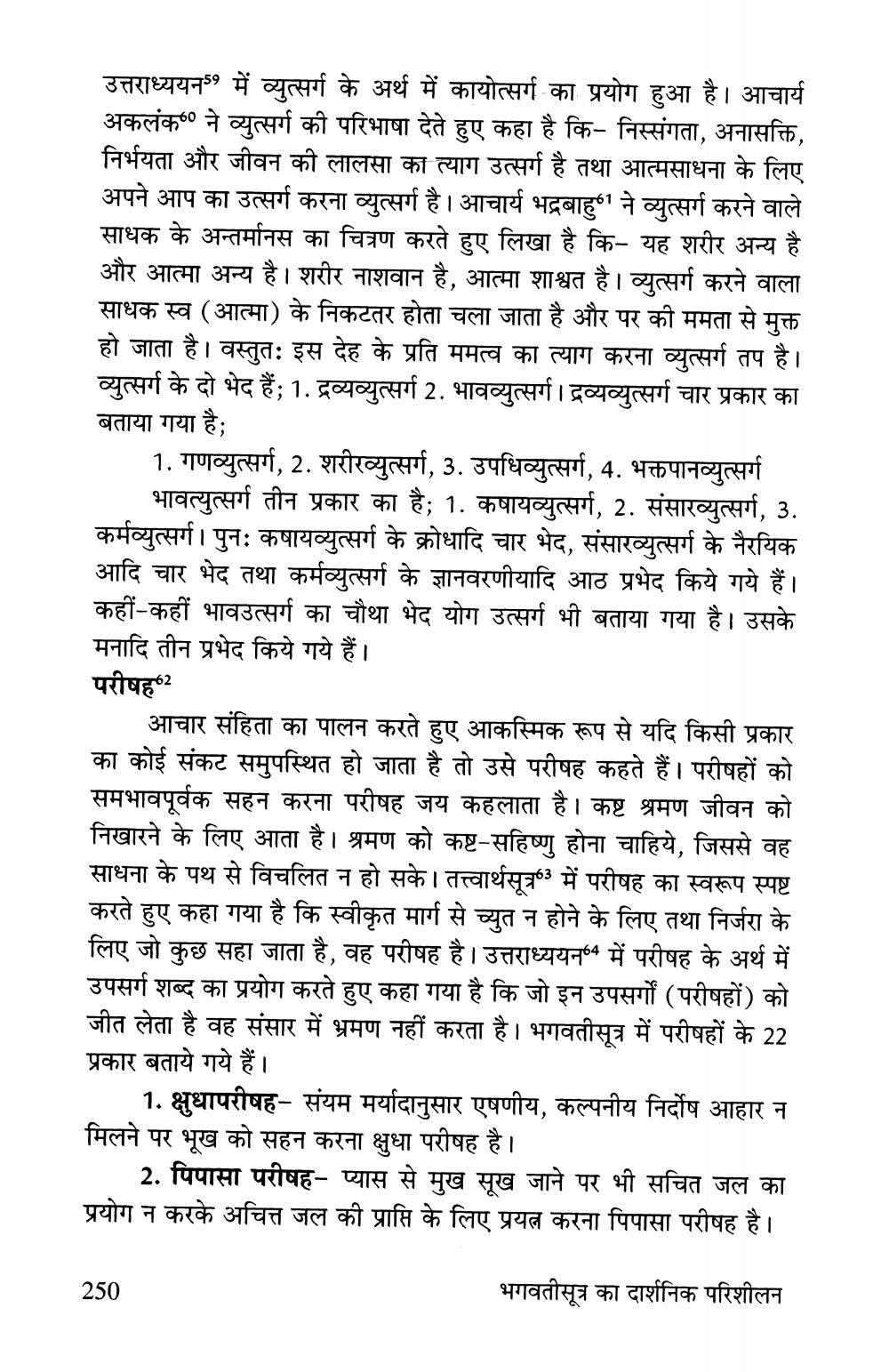________________
उत्तराध्ययन में व्युत्सर्ग के अर्थ में कायोत्सर्ग का प्रयोग हुआ है। आचार्य अकलंक ने व्युत्सर्ग की परिभाषा देते हुए कहा है कि- निस्संगता, अनासक्ति, निर्भयता और जीवन की लालसा का त्याग उत्सर्ग है तथा आत्मसाधना के लिए अपने आप का उत्सर्ग करना व्युत्सर्ग है। आचार्य भद्रबाहु1 ने व्युत्सर्ग करने वाले साधक के अन्तर्मानस का चित्रण करते हुए लिखा है कि- यह शरीर अन्य है
और आत्मा अन्य है। शरीर नाशवान है, आत्मा शाश्वत है। व्युत्सर्ग करने वाला साधक स्व (आत्मा) के निकटतर होता चला जाता है और पर की ममता से मुक्त हो जाता है। वस्तुतः इस देह के प्रति ममत्व का त्याग करना व्युत्सर्ग तप है। व्युत्सर्ग के दो भेद हैं; 1. द्रव्यव्युत्सर्ग 2. भावव्युत्सर्ग। द्रव्यव्युत्सर्ग चार प्रकार का बताया गया है;
1. गणव्युत्सर्ग, 2. शरीरव्युत्सर्ग, 3. उपधिव्युत्सर्ग, 4. भक्तपानव्युत्सर्ग
भावत्युत्सर्ग तीन प्रकार का है; 1. कषायव्युत्सर्ग, 2. संसारव्युत्सर्ग, 3. कर्मव्युत्सर्ग। पुनः कषायव्युत्सर्ग के क्रोधादि चार भेद, संसारव्युत्सर्ग के नैरयिक आदि चार भेद तथा कर्मव्युत्सर्ग के ज्ञानवरणीयादि आठ प्रभेद किये गये हैं। कहीं-कहीं भावउत्सर्ग का चौथा भेद योग उत्सर्ग भी बताया गया है। उसके मनादि तीन प्रभेद किये गये हैं। परीषहर
आचार संहिता का पालन करते हुए आकस्मिक रूप से यदि किसी प्रकार का कोई संकट समुपस्थित हो जाता है तो उसे परीषह कहते हैं। परीषहों को समभावपूर्वक सहन करना परीषह जय कहलाता है। कष्ट श्रमण जीवन को निखारने के लिए आता है। श्रमण को कष्ट-सहिष्णु होना चाहिये, जिससे वह साधना के पथ से विचलित न हो सके। तत्त्वार्थसूत्र में परीषह का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि स्वीकृत मार्ग से च्युत न होने के लिए तथा निर्जरा के लिए जो कुछ सहा जाता है, वह परीषह है। उत्तराध्ययन4 में परीषह के अर्थ में उपसर्ग शब्द का प्रयोग करते हुए कहा गया है कि जो इन उपसर्गों (परीषहों) को जीत लेता है वह संसार में भ्रमण नहीं करता है। भगवतीसूत्र में परीषहों के 22 प्रकार बताये गये हैं।
1. क्षुधापरीषह- संयम मर्यादानुसार एषणीय, कल्पनीय निर्दोष आहार न मिलने पर भूख को सहन करना क्षुधा परीषह है।
2. पिपासा परीषह- प्यास से मुख सूख जाने पर भी सचित जल का प्रयोग न करके अचित्त जल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना पिपासा परीषह है।
250
भगवतीसूत्र का दार्शनिक परिशीलन