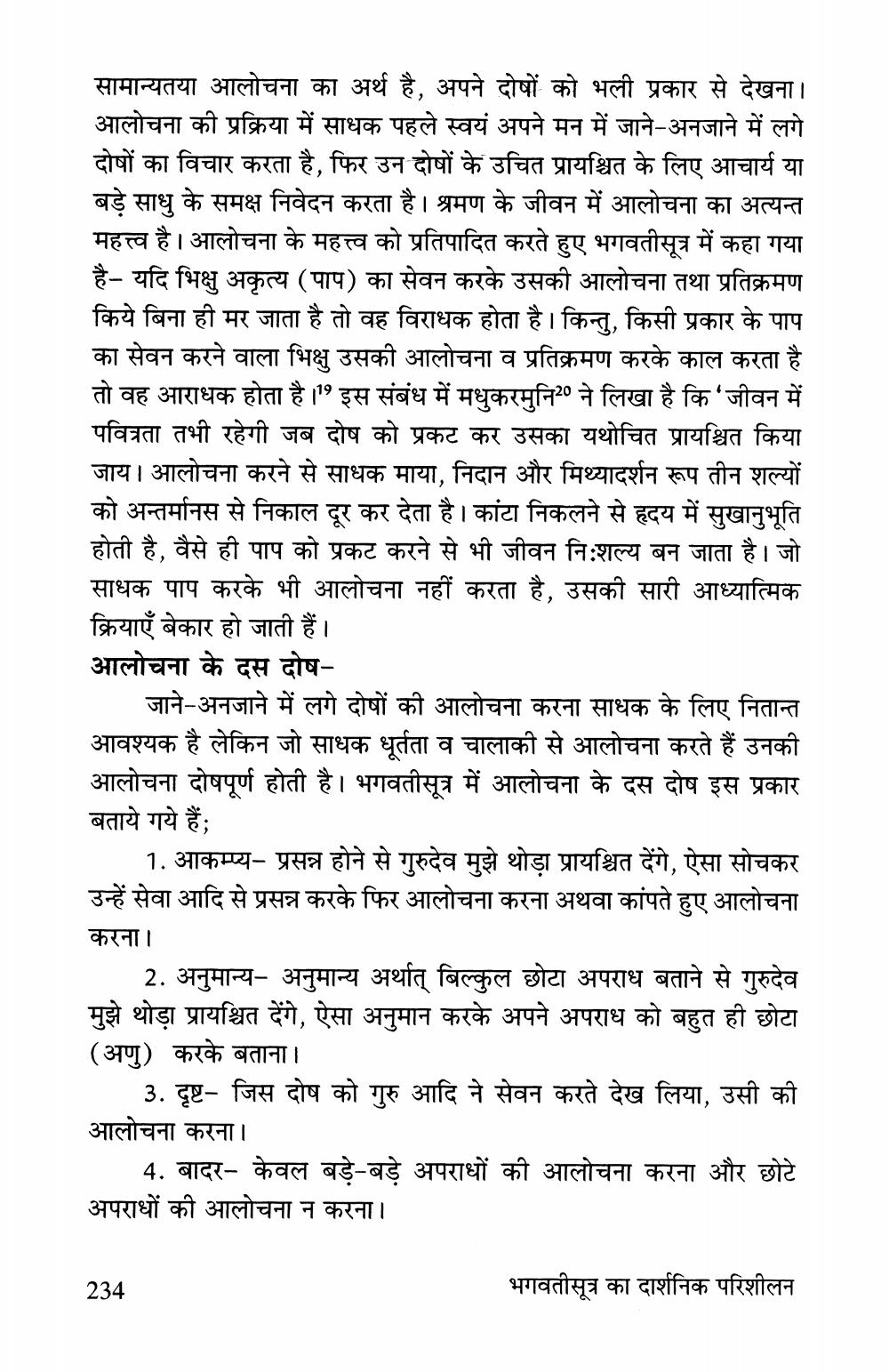________________
सामान्यतया आलोचना का अर्थ है, अपने दोषों को भली प्रकार से देखना। आलोचना की प्रक्रिया में साधक पहले स्वयं अपने मन में जाने-अनजाने में लगे दोषों का विचार करता है, फिर उन दोषों के उचित प्रायश्चित के लिए आचार्य या बड़े साधु के समक्ष निवेदन करता है। श्रमण के जीवन में आलोचना का अत्यन्त महत्त्व है। आलोचना के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए भगवतीसूत्र में कहा गया है- यदि भिक्षु अकृत्य (पाप) का सेवन करके उसकी आलोचना तथा प्रतिक्रमण किये बिना ही मर जाता है तो वह विराधक होता है। किन्तु, किसी प्रकार के पाप का सेवन करने वाला भिक्षु उसकी आलोचना व प्रतिक्रमण करके काल करता है तो वह आराधक होता है। इस संबंध में मधुकरमुनि ने लिखा है कि जीवन में पवित्रता तभी रहेगी जब दोष को प्रकट कर उसका यथोचित प्रायश्चित किया जाय। आलोचना करने से साधक माया, निदान और मिथ्यादर्शन रूप तीन शल्यों को अन्तर्मानस से निकाल दूर कर देता है। कांटा निकलने से हृदय में सुखानुभूति होती है, वैसे ही पाप को प्रकट करने से भी जीवन निःशल्य बन जाता है। जो साधक पाप करके भी आलोचना नहीं करता है, उसकी सारी आध्यात्मिक क्रियाएँ बेकार हो जाती हैं। आलोचना के दस दोष
जाने-अनजाने में लगे दोषों की आलोचना करना साधक के लिए नितान्त आवश्यक है लेकिन जो साधक धूर्तता व चालाकी से आलोचना करते हैं उनकी आलोचना दोषपूर्ण होती है। भगवतीसूत्र में आलोचना के दस दोष इस प्रकार बताये गये हैं;
1. आकम्प्य- प्रसन्न होने से गुरुदेव मुझे थोड़ा प्रायश्चित देंगे, ऐसा सोचकर उन्हें सेवा आदि से प्रसन्न करके फिर आलोचना करना अथवा कांपते हुए आलोचना करना।
2. अनुमान्य- अनुमान्य अर्थात् बिल्कुल छोटा अपराध बताने से गुरुदेव मुझे थोड़ा प्रायश्चित देंगे, ऐसा अनुमान करके अपने अपराध को बहुत ही छोटा (अणु) करके बताना।
3. दृष्ट- जिस दोष को गुरु आदि ने सेवन करते देख लिया, उसी की आलोचना करना। ___4. बादर- केवल बड़े-बड़े अपराधों की आलोचना करना और छोटे अपराधों की आलोचना न करना।
234
भगवतीसूत्र का दार्शनिक परिशीलन