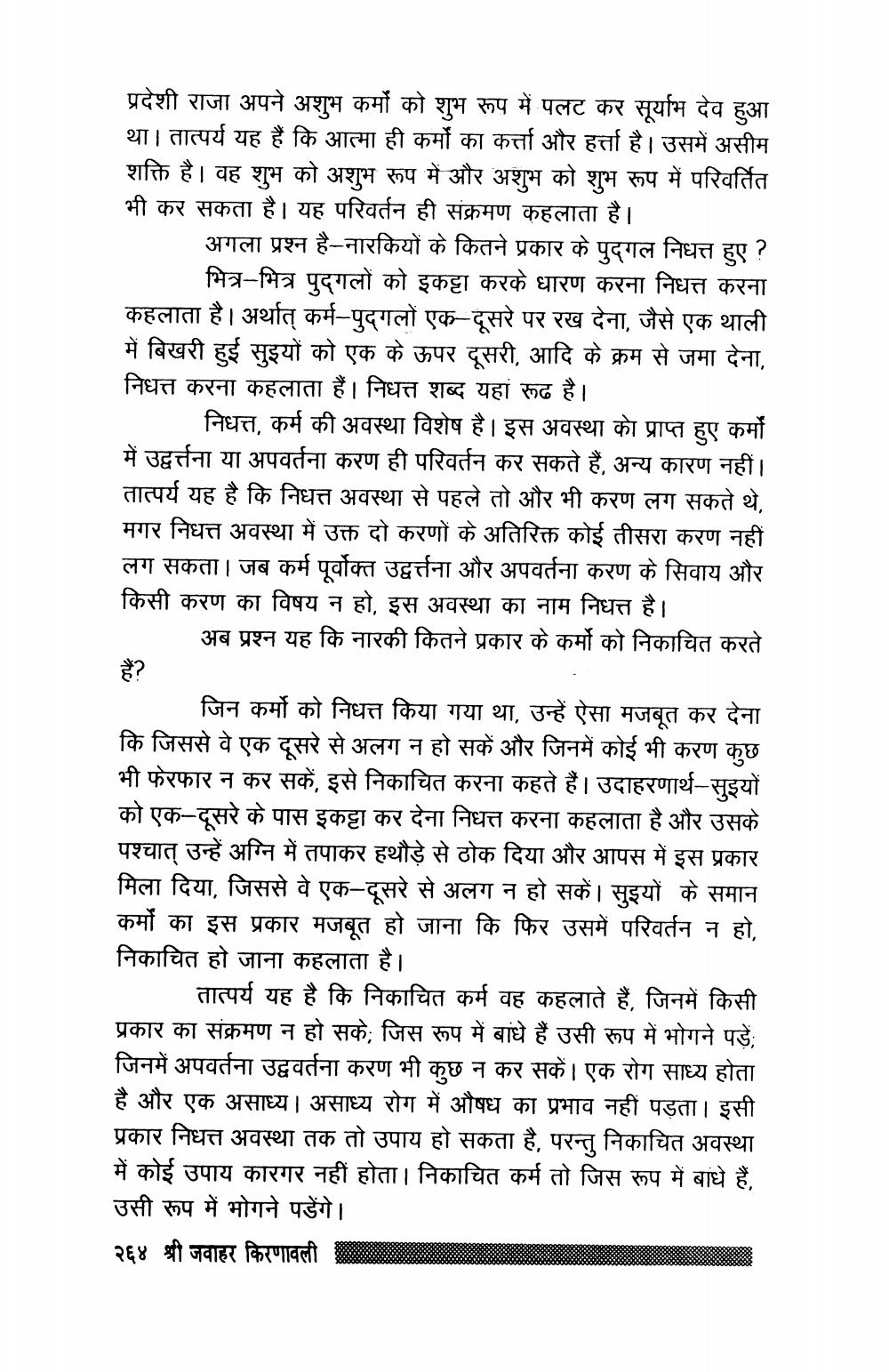________________
प्रदेशी राजा अपने अशुभ कर्मों को शुभ रूप में पलट कर सूर्याभ देव हुआ था। तात्पर्य यह हैं कि आत्मा ही कर्मों का कर्त्ता और हर्त्ता है । उसमें असीम शक्ति है। वह शुभ को अशुभ रूप में और अशुभ को शुभ रूप में परिवर्तित भी कर सकता है । यह परिवर्तन ही संक्रमण कहलाता है ।
अगला प्रश्न है - नारकियों के कितने प्रकार के पुद्गल निधत्त हुए ? भित्र-भित्र पुद्गलों को इकट्टा करके धारण करना निधत्त करना कहलाता है। अर्थात् कर्म - पुद्गलों एक-दूसरे पर रख देना, जैसे एक थाली में बिखरी हुई सुइयों को एक के ऊपर दूसरी, आदि के क्रम से जमा देना, निधत्त करना कहलाता हैं । निधत्त शब्द यहां रूढ है ।
निधत्त, कर्म की अवस्था विशेष है। इस अवस्था को प्राप्त हुए कर्मों उद्वर्त्तना या अपवर्तना करण ही परिवर्तन कर सकते हैं, अन्य कारण नहीं । तात्पर्य यह है कि निधत्त अवस्था से पहले तो और भी करण लग सकते थे, मगर निधत्त अवस्था में उक्त दो करणों के अतिरिक्त कोई तीसरा करण नहीं लग सकता। जब कर्म पूर्वोक्त उद्वर्त्तना और अपवर्तना करण के सिवाय और किसी करण का विषय न हो, इस अवस्था का नाम निधत्त है ।
अब प्रश्न यह कि नारकी कितने प्रकार के कर्मों को निकाचित करते
हैं?
जिन कर्मो को निधत्त किया गया था, उन्हें ऐसा मजबूत कर देना कि जिससे वे एक दूसरे से अलग न हो सकें और जिनमें कोई भी करण कुछ भी फेरफार न कर सकें, इसे निकाचित करना कहते हैं। उदाहरणार्थ- सुइयों को एक-दूसरे के पास इकट्टा कर देना निधत्त करना कहलाता है और उसके पश्चात् उन्हें अग्नि में तपाकर हथौड़े से ठोक दिया और आपस में इस प्रकार मिला दिया, जिससे वे एक-दूसरे से अलग न हो सकें। सुइयों के समान कर्मों का इस प्रकार मजबूत हो जाना कि फिर उसमें परिवर्तन न हो, निकाचित हो जाना कहलाता है।
तात्पर्य यह है कि निकाचित कर्म वह कहलाते हैं, जिनमें किसी प्रकार का संक्रमण न हो सके; जिस रूप में बांधे हैं उसी रूप में भोगने पड़े; जिनमें अपवर्तना उद्ववर्तना करण भी कुछ न कर सकें। एक रोग साध्य होता है और एक असाध्य । असाध्य रोग में औषध का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार निधत्त अवस्था तक तो उपाय हो सकता है, परन्तु निकाचित अवस्था में कोई उपाय कारगर नहीं होता । निकाचित कर्म तो जिस रूप में बांधे हैं, उसी रूप में भोगने पडेंगे।
२६४ श्री जवाहर किरणावली