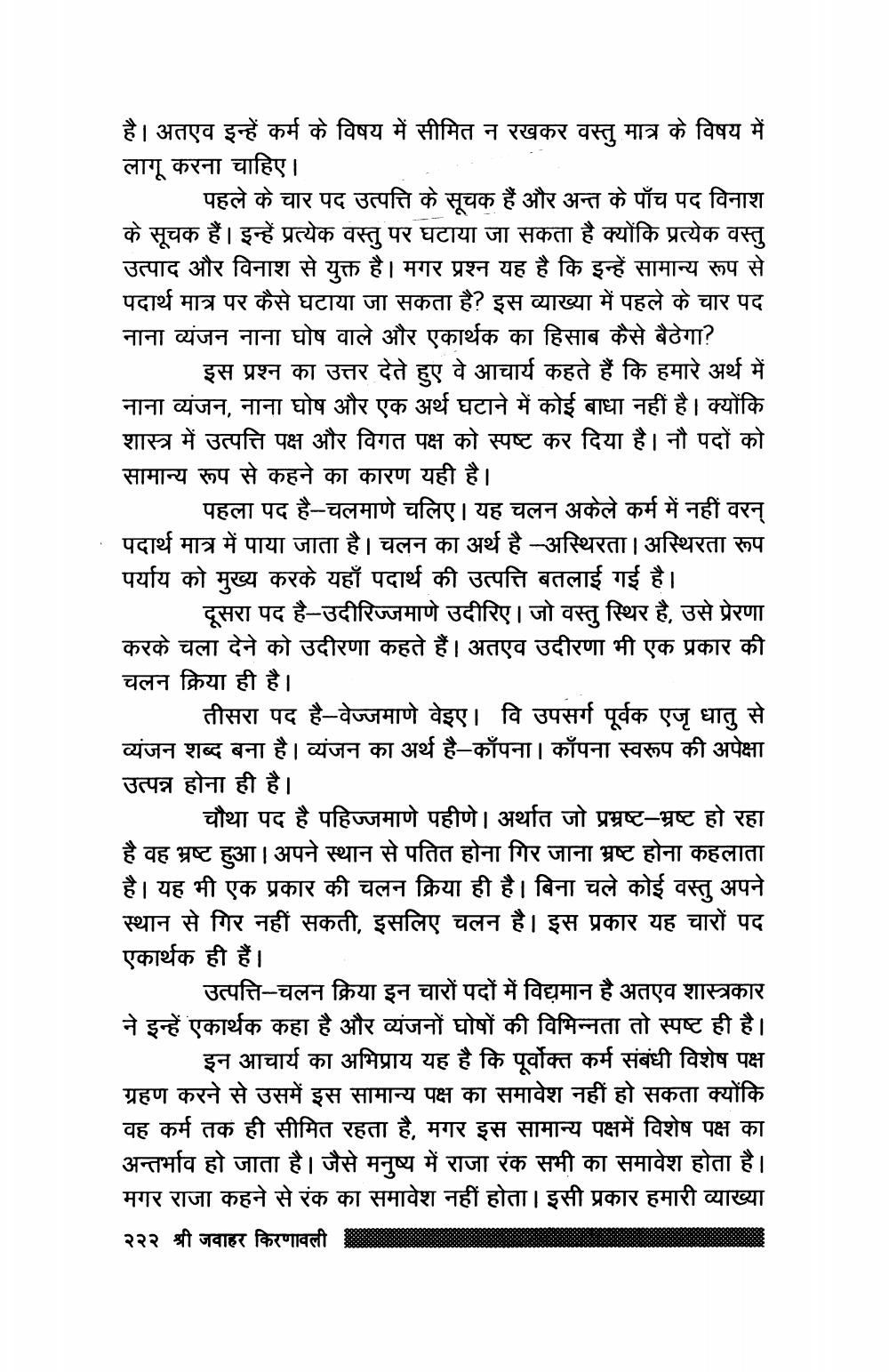________________
है। अतएव इन्हें कर्म के विषय में सीमित न रखकर वस्तु मात्र के विषय में लागू करना चाहिए।
पहले के चार पद उत्पत्ति के सूचक हैं और अन्त के पाँच पद विनाश के सूचक हैं। इन्हें प्रत्येक वस्तु पर घटाया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक वस्तु उत्पाद और विनाश से युक्त है। मगर प्रश्न यह है कि इन्हें सामान्य रूप से पदार्थ मात्र पर कैसे घटाया जा सकता है? इस व्याख्या में पहले के चार पद नाना व्यंजन नाना घोष वाले और एकार्थक का हिसाब कैसे बैठेगा?
_इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वे आचार्य कहते हैं कि हमारे अर्थ में नाना व्यंजन, नाना घोष और एक अर्थ घटाने में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि शास्त्र में उत्पत्ति पक्ष और विगत पक्ष को स्पष्ट कर दिया है। नौ पदों को सामान्य रूप से कहने का कारण यही है।
पहला पद है-चलमाणे चलिए। यह चलन अकेले कर्म में नहीं वरन् पदार्थ मात्र में पाया जाता है। चलन का अर्थ है -अस्थिरता। अस्थिरता रूप पर्याय को मुख्य करके यहाँ पदार्थ की उत्पत्ति बतलाई गई है।
दूसरा पद है-उदीरिज्जमाणे उदीरिए। जो वस्तु स्थिर है, उसे प्रेरणा करके चला देने को उदीरणा कहते हैं। अतएव उदीरणा भी एक प्रकार की चलन क्रिया ही है।
तीसरा पद है-वेज्जमाणे वेइए। वि उपसर्ग पूर्वक एकृ धातु से व्यंजन शब्द बना है। व्यंजन का अर्थ है-कॉपना। कॉपना स्वरूप की अपेक्षा उत्पन्न होना ही है।
चौथा पद है पहिज्जमाणे पहीणे। अर्थात जो प्रभ्रष्ट-भ्रष्ट हो रहा है वह भ्रष्ट हुआ। अपने स्थान से पतित होना गिर जाना भ्रष्ट होना कहलाता है। यह भी एक प्रकार की चलन क्रिया ही है। बिना चले कोई वस्तु अपने स्थान से गिर नहीं सकती, इसलिए चलन है। इस प्रकार यह चारों पद एकार्थक ही हैं।
उत्पत्ति-चलन क्रिया इन चारों पदों में विद्यमान है अतएव शास्त्रकार ने इन्हें एकार्थक कहा है और व्यंजनों घोषों की विभिन्नता तो स्पष्ट ही है।
इन आचार्य का अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त कर्म संबंधी विशेष पक्ष ग्रहण करने से उसमें इस सामान्य पक्ष का समावेश नहीं हो सकता क्योंकि वह कर्म तक ही सीमित रहता है, मगर इस सामान्य पक्षमें विशेष पक्ष का अन्तर्भाव हो जाता है। जैसे मनुष्य में राजा रंक सभी का समावेश होता है। मगर राजा कहने से रंक का समावेश नहीं होता। इसी प्रकार हमारी व्याख्या २२२ श्री जवाहर किरणावली