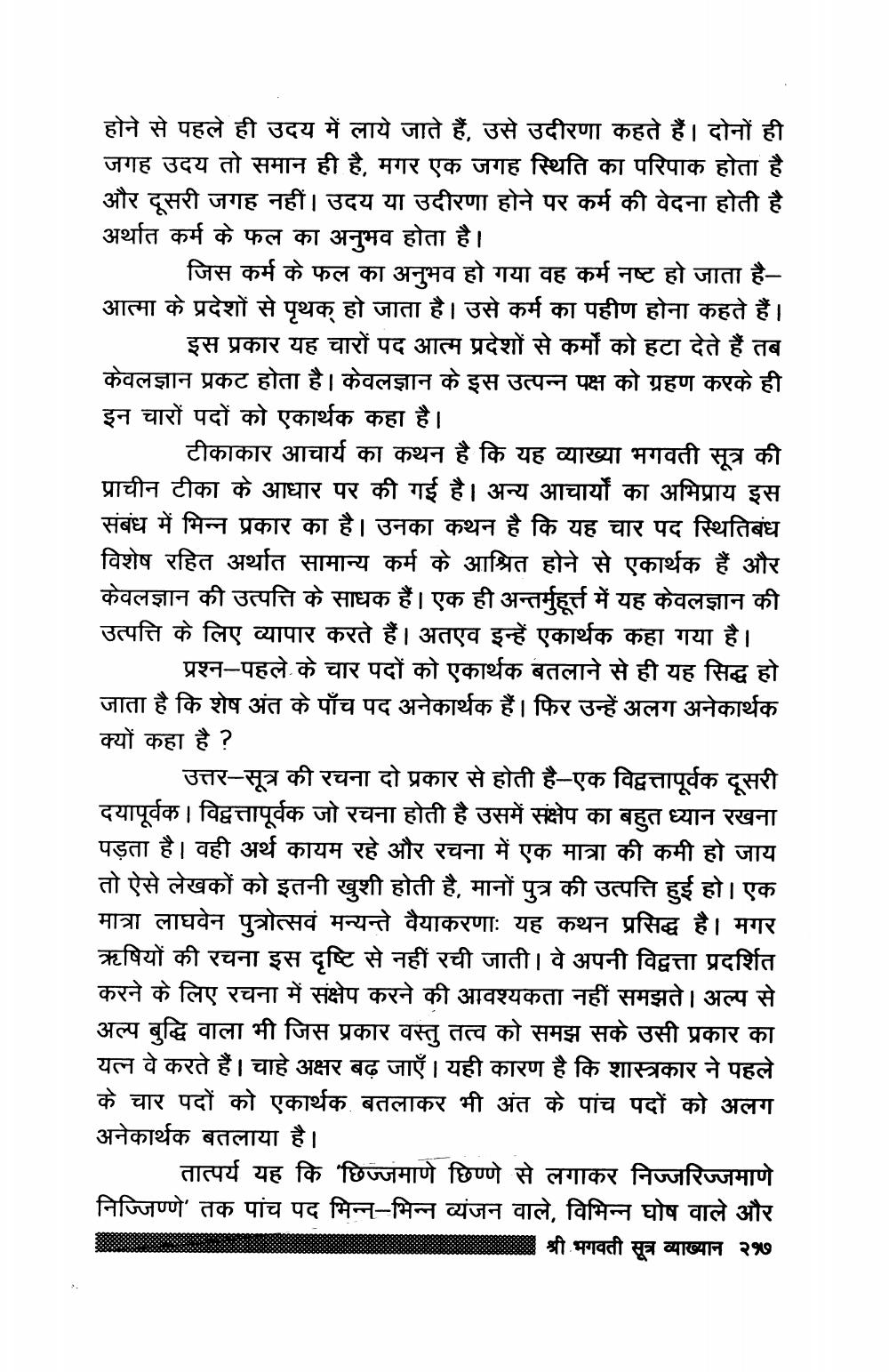________________
होने से पहले ही उदय में लाये जाते हैं, उसे उदीरणा कहते हैं। दोनों ही जगह उदय तो समान ही है, मगर एक जगह स्थिति का परिपाक होता है और दूसरी जगह नहीं। उदय या उदीरणा होने पर कर्म की वेदना होती है अर्थात कर्म के फल का अनुभव होता है।
जिस कर्म के फल का अनुभव हो गया वह कर्म नष्ट हो जाता हैआत्मा के प्रदेशों से पृथक् हो जाता है। उसे कर्म का पहीण होना कहते हैं।
___ इस प्रकार यह चारों पद आत्म प्रदेशों से कर्मों को हटा देते हैं तब केवलज्ञान प्रकट होता है। केवलज्ञान के इस उत्पन्न पक्ष को ग्रहण करके ही इन चारों पदों को एकार्थक कहा है।
टीकाकार आचार्य का कथन है कि यह व्याख्या भगवती सूत्र की प्राचीन टीका के आधार पर की गई है। अन्य आचार्यों का अभिप्राय इस संबंध में भिन्न प्रकार का है। उनका कथन है कि यह चार पद स्थितिबंध विशेष रहित अर्थात सामान्य कर्म के आश्रित होने से एकार्थक हैं और केवलज्ञान की उत्पत्ति के साधक हैं। एक ही अन्तर्मुहूर्त में यह केवलज्ञान की उत्पत्ति के लिए व्यापार करते हैं। अतएव इन्हें एकार्थक कहा गया है।
प्रश्न-पहले के चार पदों को एकार्थक बतलाने से ही यह सिद्ध हो जाता है कि शेष अंत के पाँच पद अनेकार्थक हैं। फिर उन्हें अलग अनेकार्थक क्यों कहा है ?
उत्तर-सूत्र की रचना दो प्रकार से होती है-एक विद्वत्तापूर्वक दूसरी दयापूर्वक । विद्वत्तापूर्वक जो रचना होती है उसमें संक्षेप का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वही अर्थ कायम रहे और रचना में एक मात्रा की कमी हो जाय तो ऐसे लेखकों को इतनी खुशी होती है, मानों पुत्र की उत्पत्ति हुई हो। एक मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः यह कथन प्रसिद्ध है। मगर ऋषियों की रचना इस दृष्टि से नहीं रची जाती। वे अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए रचना में संक्षेप करने की आवश्यकता नहीं समझते। अल्प से अल्प बुद्धि वाला भी जिस प्रकार वस्तु तत्व को समझ सके उसी प्रकार का यत्न वे करते हैं। चाहे अक्षर बढ़ जाएँ। यही कारण है कि शास्त्रकार ने पहले के चार पदों को एकार्थक बतलाकर भी अंत के पांच पदों को अलग अनेकार्थक बतलाया है।
तात्पर्य यह कि 'छिज्जमाणे छिण्णे से लगाकर निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे' तक पांच पद भिन्न-भिन्न व्यंजन वाले, विभिन्न घोष वाले और
-श्री भगवती सूत्र व्याख्यान २१७