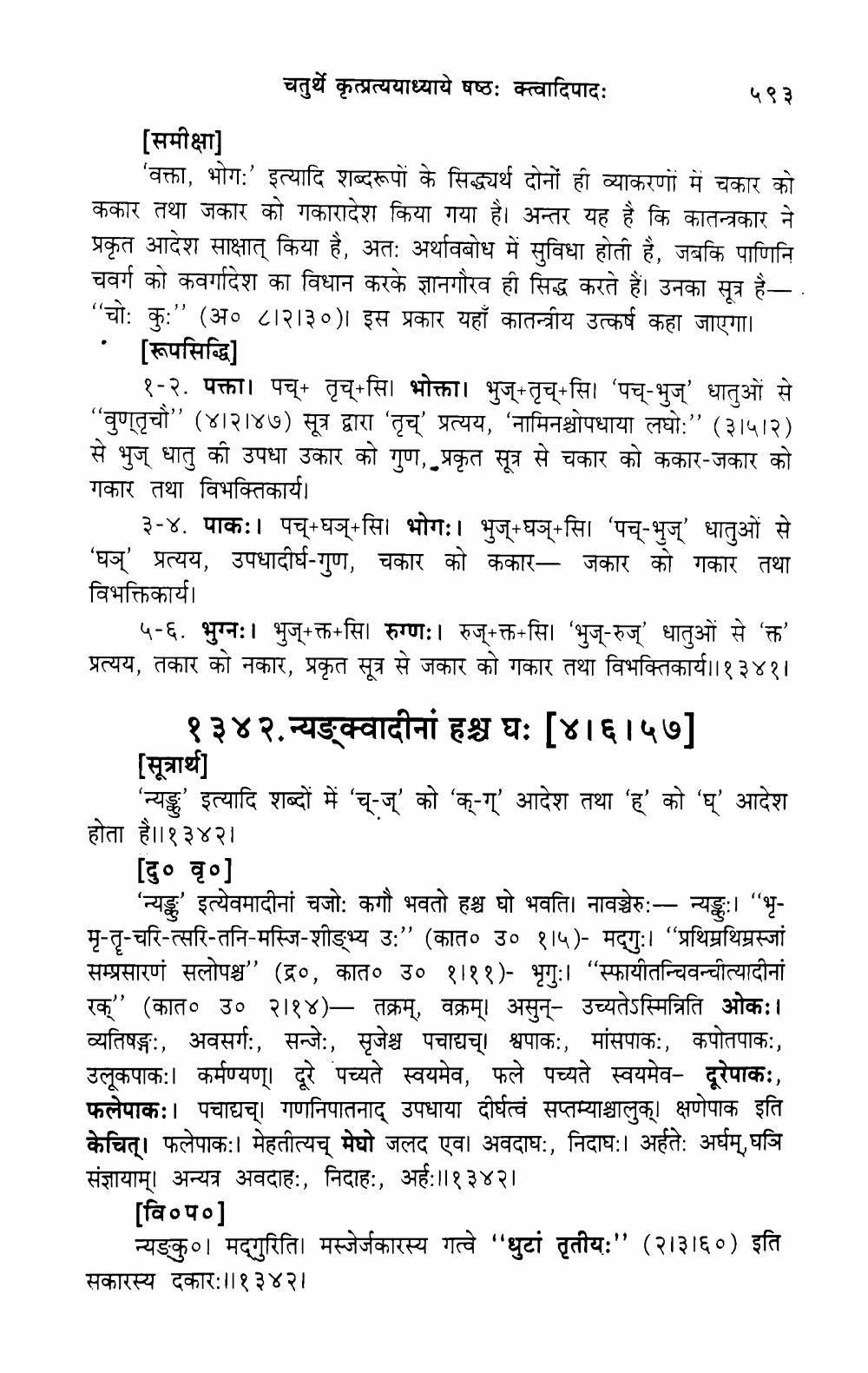________________
चतुर्थे कृत्प्रत्ययाध्याये षष्ठः क्त्वादिपादः
५९३ [समीक्षा]
'वक्ता, भोग:' इत्यादि शब्दरूपों के सिद्धयर्थ दोनों ही व्याकरणों में चकार को ककार तथा जकार को गकारादेश किया गया है। अन्तर यह है कि कातन्त्रकार ने प्रकृत आदेश साक्षात् किया है, अत: अर्थावबोध में सुविधा होती है, जबकि पाणिनि चवर्ग को कवर्गादेश का विधान करके ज्ञानगौरव ही सिद्ध करते हैं। उनका सूत्र है"चोः कुः'' (अ० ८।२।३०)। इस प्रकार यहाँ कातन्त्रीय उत्कर्ष कहा जाएगा। - [रूपसिद्धि]
१-२. पक्ता। पच्+ तृच्+सि। भोक्ता। भुज् तृच्+सि। ‘पच्-भुज्' धातुओं से “वुण्तृचो'' (४।२।४७) सूत्र द्वारा 'तृच्' प्रत्यय, 'नामिनश्चोपधाया लघो:'' (३।५।२) से भुज् धातु की उपधा उकार को गुण, प्रकृत सूत्र से चकार को ककार-जकार को गकार तथा विभक्तिकार्य।
३-४. पाकः। पच्+घञ्+सि। भोगः। भुज्+घञ्+सि। ‘पच्-भुज्' धातुओं से 'घञ्' प्रत्यय, उपधादीर्घ-गुण, चकार को ककार- जकार को गकार तथा विभक्तिकार्य।
५-६. भुग्नः। भुज्+क्त+सि। रुग्णः । रुज्+क्तसि। 'भुज्-रुज्' धातुओं से 'क्त' प्रत्यय, तकार को नकार, प्रकृत सूत्र से जकार को गकार तथा विभक्तिकार्य।।१३४१।
१३४२.न्यङ्कवादीनां हश्च घः [४।६।५७] [सूत्रार्थ
'न्यङ्घ' इत्यादि शब्दों में ‘च्-ज्' को 'क्-ग्' आदेश तथा 'ह्' को 'घ्' आदेश होता है।।१३४२।
[दु० वृ०]
'न्यङ्घ' इत्येवमादीनां चजोः कगौ भवतो हश्च घो भवति। नावञ्चेरु:- न्यङ्घः। “भृमृ-तृ-चरि-त्सरि-तनि-मस्जि-शीङ्भ्य उ:' (कात० उ० १।५)- मद्गुः। “प्रथिम्रथिम्रस्जां सम्प्रसारणं सलोपश्च' (द्र०, कात० उ० १।११)- भृगुः। “स्फायीतन्चिवन्चीत्यादीनां रक्” (कात० उ० २।१४)- तक्रम्, वक्रम्। असुन्- उच्यतेऽस्मिन्निति ओकः। व्यतिषङ्गः, अवसर्गः, सन्जेः, सृजेश्च पचाद्यच्। श्वपाकः, मांसपाकः, कपोतपाकः, उलूकपाकः। कर्मण्यण। दूरे पच्यते स्वयमेव, फले पच्यते स्वयमेव- दूरेपाकः, फलेपाकः। पचाद्यच्। गणनिपातनाद् उपधाया दीर्घत्वं सप्तम्याश्चालुक्। क्षणेपाक इति केचित्। फलेपाकः। मेहतीत्यच् मेघो जलद एव। अवदाघ:, निदाघः। अर्हतेः अर्घम्,घबि संज्ञायाम्। अन्यत्र अवदाह:, निदाहः, अर्हः।।१३४२।
[वि०प०]
न्यकु०। मद्गुरिति। मस्जेर्जकारस्य गत्वे "धुटां तृतीयः' (२।३।६०) इति सकारस्य दकारः।।१३४२।