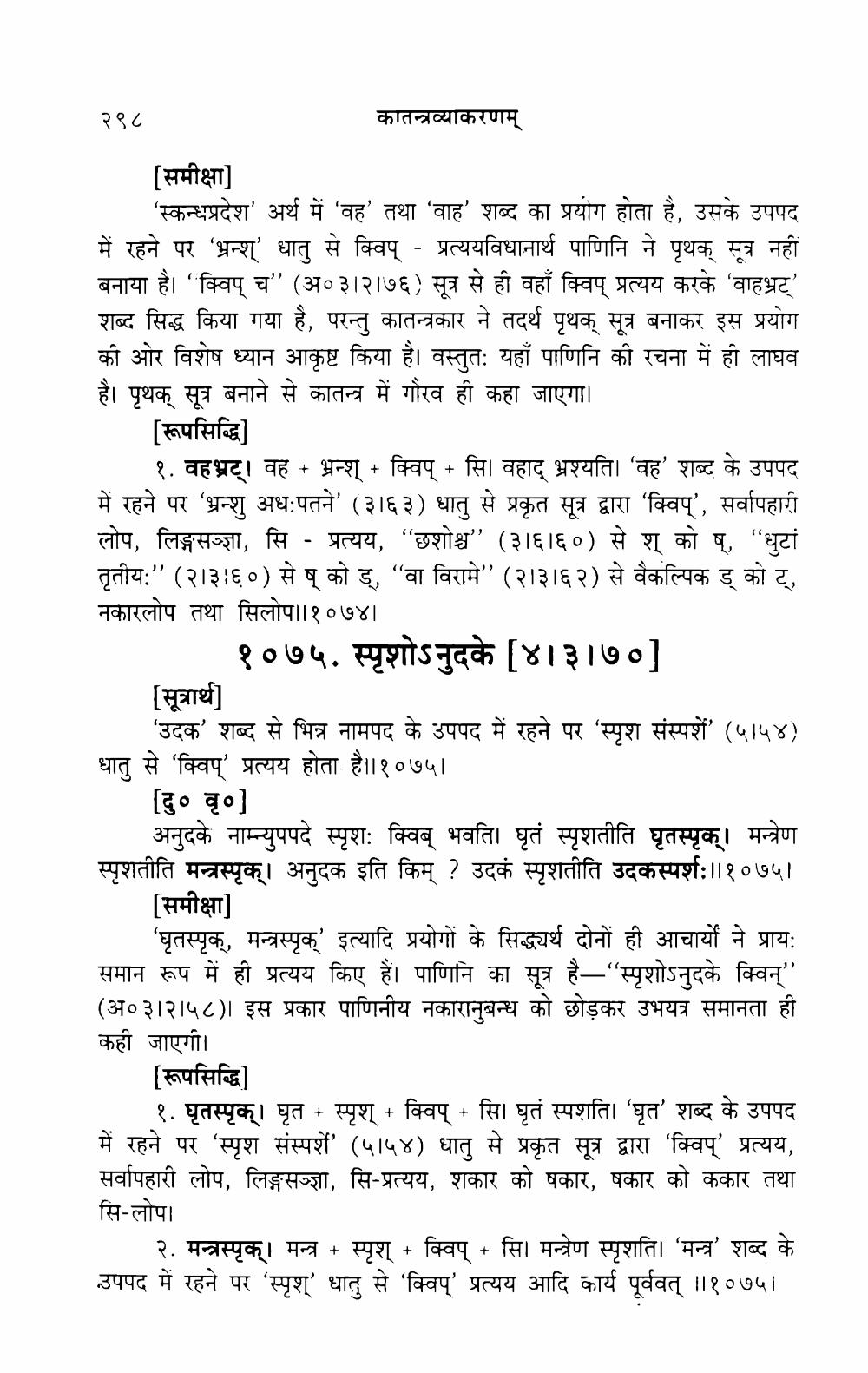________________
२९८
कातन्त्रव्याकरणम्
[समीक्षा]
'स्कन्धप्रदेश' अर्थ में 'वह' तथा 'वाह' शब्द का प्रयोग होता है, उसके उपपद में रहने पर 'भ्रन्श्' धातु से क्विप् प्रत्ययविधानार्थ पाणिनि ने पृथक् सूत्र नहीं बनाया है। ंक्विप् च’” (अ०३।२।७६) सूत्र से ही वहाँ क्विप् प्रत्यय करके 'वाहभ्रट्' शब्द सिद्ध किया गया है, परन्तु कातन्त्रकार ने तदर्थ पृथक् सूत्र बनाकर इस प्रयोग की ओर विशेष ध्यान आकृष्ट किया है। वस्तुतः यहाँ पाणिनि की रचना में ही लाघव है | पृथक् सूत्र बनाने से कातन्त्र में गौरव ही कहा जाएगा।
[रूपसिद्धि]
-
१. वह भ्रट् । वह + भ्रन्श् + क्विप् + सि। वहाद् भ्रश्यति । 'वह' शब्द के उपपद में रहने पर 'भ्रन्शु अध: पतने' ( ३।६३) धातु से प्रकृत सूत्र द्वारा 'क्विप्', सर्वापहारी लोप, लिङ्गसञ्ज्ञा, सि प्रत्यय, “छशोश्च” (३।६।६० ) से श् को घ्, “धुटां तृतीय:” (२।३:६०) से ष् को ड्, “वा विरामे” (२।३।६२) से वैकल्पिक ड् को ट्, नकारलोप तथा सिलोप।। १०७४ ।
१०७५. स्पृशोऽनुदके [४।३।७०]
[सूत्रार्थ]
'उदक' शब्द से भिन्न नामपद के उपपद में रहने पर 'स्पृश संस्पर्श' (५/५४) धातु से 'क्विप्' प्रत्यय होता है ।। १०७५ ।
[दु० वृ० ]
अनुदके नाम्न्युपपदे स्पृशः क्विब् भवति । घृतं स्पृशतीति घृतस्पृक्। मन्त्रेण स्पृशतीति मन्त्रस्पृक् । अनुदक इति किम् ? उदकं स्पृशतीति उदकस्पर्शः ।। १०७५ । [समीक्षा]
'घृतस्पृक्, मन्त्रस्पृक्' इत्यादि प्रयोगों के सिद्ध्यर्थ दोनों ही आचार्यों ने प्रायः समान रूप में ही प्रत्यय किए हैं। पाणिनि का सूत्र है - "स्पृशोऽनुदके क्विन्" (अ०३।२।५८)। इस प्रकार पाणिनीय नकारानुबन्ध को छोड़कर उभयत्र समानता ही कही जाएगी।
[रूपसिद्धि]
१. घृतस्पृक् । घृत + स्पृश् + क्विप् + सि। घृतं स्पशति । 'घृत' शब्द के उपपद में रहने पर 'स्पृश संस्पर्श' (५/५४) धातु से प्रकृत सूत्र द्वारा 'क्विप्' प्रत्यय, सर्वापहारी लोप, लिङ्गसञ्ज्ञा, सि-प्रत्यय, शकार को षकार, षकार को ककार तथा सि-लोप।
२. मन्त्रस्पृक् । मन्त्र + स्पृश् + क्विप् + सि। मन्त्रेण स्पृशति । 'मन्त्र' शब्द के उपपद में रहने पर ‘स्पृश्' धातु से 'क्विप्' प्रत्यय आदि कार्य पूर्ववत् ॥ १०७५ |