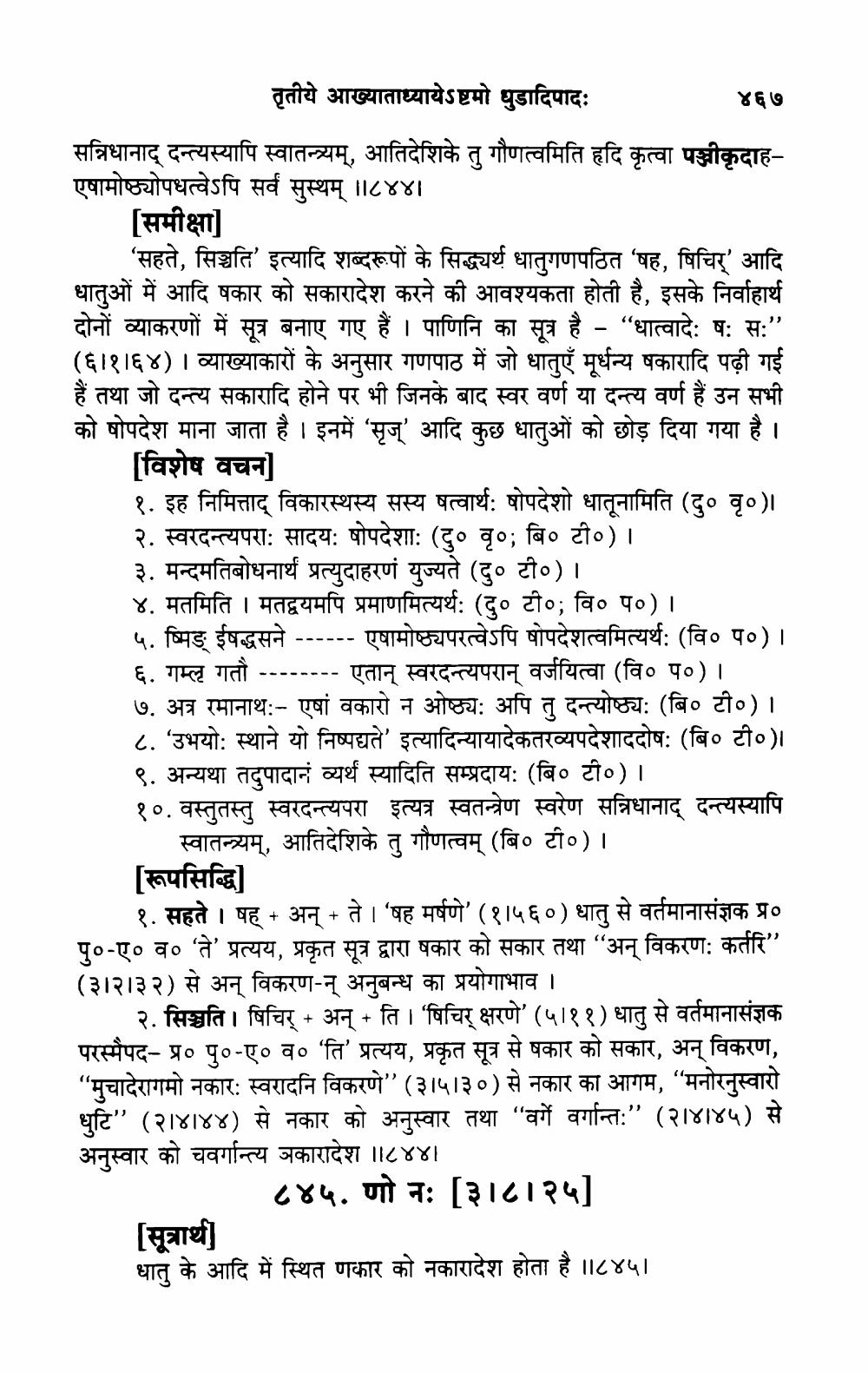________________
४६७
तृतीये आख्याताध्यायेऽष्टमो घुडादिपादः ४६७ सन्निधानाद् दन्त्यस्यापि स्वातन्त्र्यम्, आतिदेशिके तु गौणत्वमिति हदि कृत्वा पञ्जीकृदाहएषामोष्ठ्योपधत्वेऽपि सर्वं सुस्थम् ।।८४४।
[समीक्षा
'सहते, सिञ्चति' इत्यादि शब्दरूपों के सिद्ध्यर्थ धातुगणपठित ‘षह, षिचिर्' आदि धातुओं में आदि षकार को सकारादेश करने की आवश्यकता होती है, इसके निर्वाहार्थ दोनों व्याकरणों में सूत्र बनाए गए हैं । पाणिनि का सूत्र है - "धात्वादेः षः सः" (६।१।६४) । व्याख्याकारों के अनुसार गणपाठ में जो धातुएँ मूर्धन्य षकारादि पढ़ी गई हैं तथा जो दन्त्य सकारादि होने पर भी जिनके बाद स्वर वर्ण या दन्त्य वर्ण हैं उन सभी को षोपदेश माना जाता है । इनमें 'सृज्' आदि कुछ धातुओं को छोड़ दिया गया है ।
[विशेष वचन] १. इह निमित्ताद् विकारस्थस्य सस्य षत्वार्थ: षोपदेशो धातूनामिति (दु० वृ०)। २. स्वरदन्त्यपरा: सादय: षोपदेशा: (दु० वृ०; बि० टी०) । ३. मन्दमतिबोधनार्थं प्रत्युदाहरणं युज्यते (दु० टी०)। ४. मतमिति । मतद्वयमपि प्रमाणमित्यर्थः (दु० टी०; वि० प०)। ५. मिङ् ईषद्धसने ------ एषामोष्ठ्यपरत्वेऽपि षोपदेशत्वमित्यर्थः (वि०प०)। ६. गम्ल गतौ -------- एतान् स्वरदन्त्यपरान् वर्जयित्वा (वि० प०) । ७. अत्र रमानाथ:- एषां वकारो न ओष्ठ्य: अपि तु दन्त्योष्ठय: (बि० टी०)। ८. 'उभयोः स्थाने यो निष्पद्यते' इत्यादिन्यायादेकतरव्यपदेशाददोष: (बि० टी०)। ९. अन्यथा तदुपादानं व्यर्थं स्यादिति सम्प्रदाय: (बि० टी०)। १०. वस्तुतस्तु स्वरदन्त्यपरा इत्यत्र स्वतन्त्रेण स्वरेण सनिधानाद् दन्त्यस्यापि
स्वातन्त्र्यम्, आतिदेशिके तु गौणत्वम् (बि० टी०) । [रूपसिद्धि]
१. सहते । षह् + अन् + ते । 'षह मर्षणे' (१।५६०) धातु से वर्तमानासंज्ञक प्र० पु०-ए० व० 'ते' प्रत्यय, प्रकृत सूत्र द्वारा षकार को सकार तथा “अन् विकरणः कर्तरि" (३।२।३२) से अन् विकरण-न् अनुबन्ध का प्रयोगाभाव ।
२. सिञ्चति। षिचिर् + अन् + ति । 'षिचिर् क्षरणे' (५।११) धातु से वर्तमानासंज्ञक परस्मैपद-प्र० पु०-ए० व० 'ति' प्रत्यय, प्रकृत सूत्र से षकार को सकार, अन् विकरण, "मुचादेरागमो नकारः स्वरादनि विकरणे'' (३।५।३०) से नकार का आगम, “मनोरनुस्वारो धुटि' (२।४।४४) से नकार को अनुस्वार तथा “वर्गे वर्गान्त:' (२।४।४५) से अनुस्वार को चवर्गान्त्य अकारादेश ।।८४४।
८४५. णो नः [३।८।२५] [सूत्रार्थ धातु के आदि में स्थित णकार को नकारादेश होता है ।।८४५।