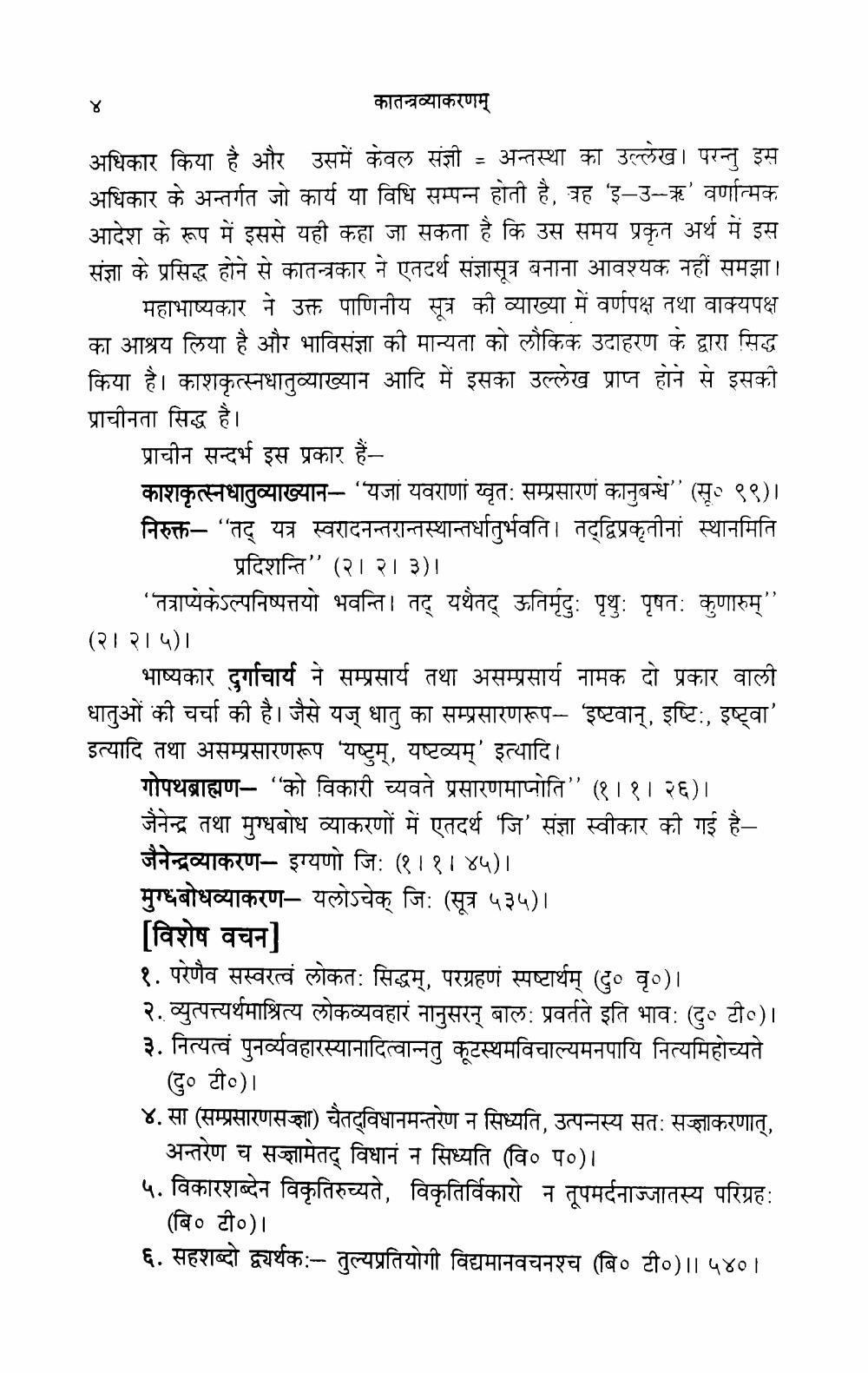________________
कातन्त्रव्याकरणम्
अधिकार किया है और उसमें केवल संज्ञी = अन्तस्था का उल्लेख | परन्तु इस अधिकार के अन्तर्गत जो कार्य या विधि सम्पन्न होती है, वह 'इ - उ ऋ' वर्णात्मक आदेश के रूप में इससे यही कहा जा सकता है कि उस समय प्रकृत अर्थ में इस संज्ञा के प्रसिद्ध होने से कातन्त्रकार ने एतदर्थ संज्ञासूत्र बनाना आवश्यक नहीं समझा। महाभाष्यकार ने उक्त पाणिनीय सूत्र की व्याख्या में वर्णपक्ष तथा वाक्यपक्ष का आश्रय लिया है और भाविसंज्ञा की मान्यता को लौकिक उदाहरण के द्वारा सिद्ध किया है। काशकृत्स्नधातुव्याख्यान आदि में इसका उल्लेख प्राप्त होने से इसकी प्राचीनता सिद्ध है।
प्राचीन सन्दर्भ इस प्रकार हैं
४
काशकृत्स्नधातुव्याख्यान - "यजां यवराणां य्वृतः सम्प्रसारणं कानुबन्धे" (सू० ९९ ) । निरुक्त— “तद् यत्र स्वरादनन्तरान्तस्थान्तर्धातुर्भवति । तद्विप्रकृतीनां स्थानमिति प्रदिशन्ति” (२ । २ । ३)।
“तत्राप्येकेऽल्पनिष्पत्तयो भवन्ति । तद् यथैतद् ऊतिर्मृदुः पृथुः पृषत: कुणारुम्” (२ । २। ५) ।
भाष्यकार दुर्गाचार्य ने सम्प्रसार्य तथा असम्प्रसार्य नामक दो प्रकार वाली धातुओं की चर्चा की है। जैसे यज् धातु का सम्प्रसारणरूप - 'इष्टवान्, इष्टि:, इष्ट्वा' इत्यादि तथा असम्प्रसारणरूप 'यष्टुम्, यष्टव्यम्' इत्यादि ।
गोपथब्राह्मण– “को विकारी च्यवते प्रसारणमाप्नोति” (१ । १ । २६) ।
जैनेन्द्र तथा मुग्धबोध व्याकरणों में एतदर्थ 'जि' संज्ञा स्वीकार की गई है— जैनेन्द्रव्याकरण- इग्यणो जि: ( १ । १ । ४५) ।
मुग्धबोधव्याकरण - यलोऽचेक् जि: ( सूत्र ५३५) ।
[विशेष वचन ]
१. परेणैव सस्वरत्वं लोकतः सिद्धम्, परग्रहणं स्पष्टार्थम् (दु० वृ० ) ।
२. व्युत्पत्त्यर्थमाश्रित्य लोकव्यवहारं नानुसरन् बाल: प्रवर्तते इति भाव: (दु० टी० ) । ३. नित्यत्वं पुनर्व्यवहारस्यानादित्वान्नतु कूटस्थमविचाल्यमनपायि नित्यमिहोच्यते (दु० टी०) ।
४. सा (सम्प्रसारणसञ्ज्ञ) चैतद्विधानमन्तरेण न सिध्यति, उत्पन्नस्य सतः सञ्ज्ञाकरणात्, अन्तरेण च सञ्ज्ञामेतद् विधानं न सिध्यति (वि० प०)।
५. विकारशब्देन विकृतिरुच्यते, विकृतिर्विकारो न तूपमर्दनाज्जातस्य परिग्रहः (बि० टी० ) ।
६. सहशब्दो द्व्यर्थक :- तुल्यप्रतियोगी विद्यमानवचनश्च (बि० टी० ) । । ५४० ।