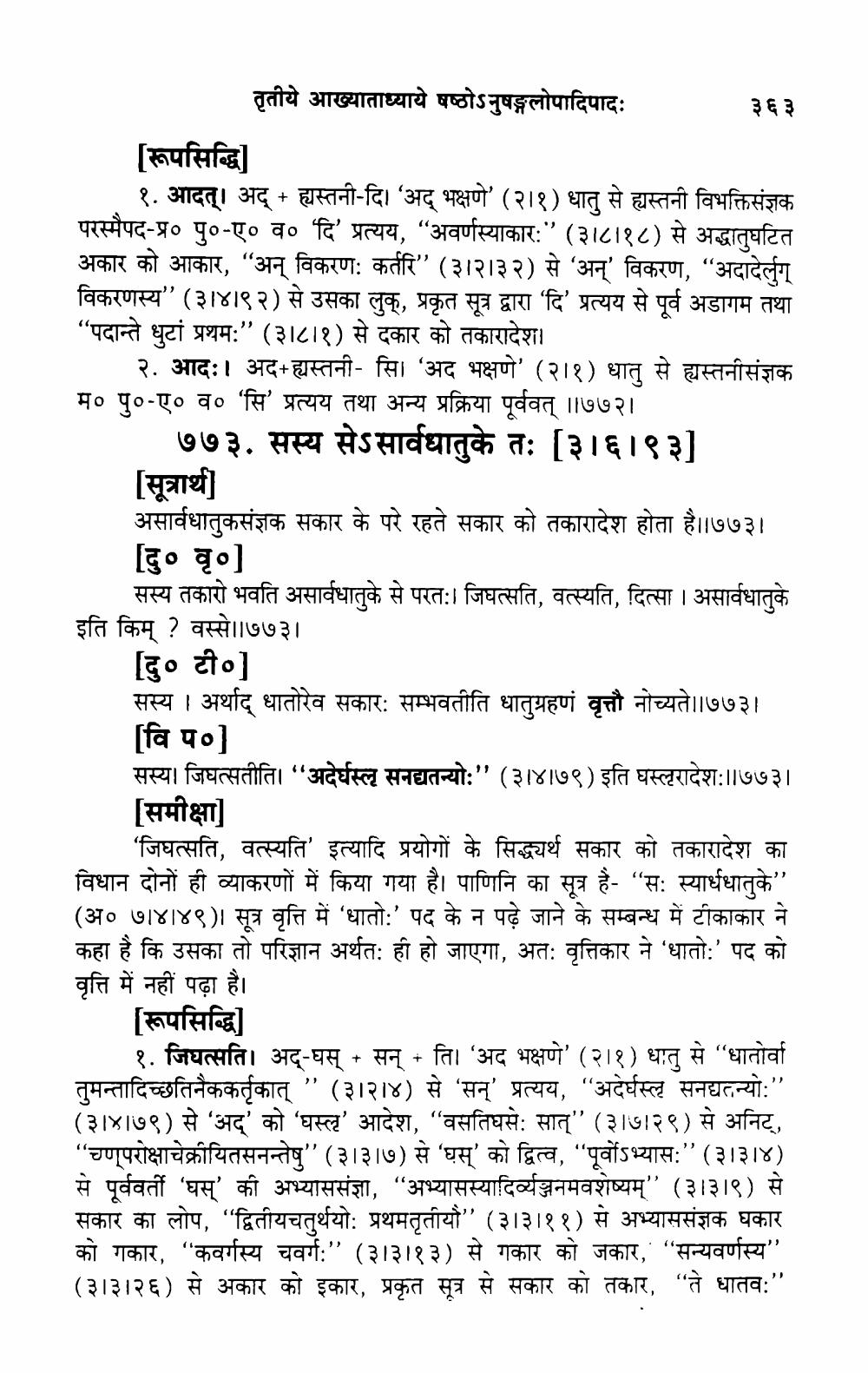________________
तृतीये आख्याताध्याये षष्ठोऽनुषङ्गलोपादिपादः
३६३ [रूपसिद्धि
१. आदत्। अद् + ह्यस्तनी-दि। ‘अद् भक्षणे' (२।१) धात् से शस्तनी विभक्तिसंज्ञक परस्मैपद-प्र० पु०-ए० व० 'दि' प्रत्यय, “अवर्णस्याकार:' (३।८।१८) से अद्धातुघटित अकार को आकार, "अन् विकरण: कर्तरि' (३।२।३२) से 'अन्' विकरण, “अदादे ग् विकरणस्य' (३।४।९२) से उसका लुक्, प्रकृत सूत्र द्वारा ‘दि' प्रत्यय से पूर्व अडागम तथा “पदान्ते धुटां प्रथमः" (३।८।१) से दकार को तकारादेश।
२. आदः। अद+शस्तनी- सि। 'अद भक्षणे' (२।१) धातु से शस्तनीसंज्ञक म० पु०-ए० व० 'सि' प्रत्यय तथा अन्य प्रक्रिया पूर्ववत् ।।७७२।
___७७३. सस्य सेऽसार्वधातुके तः [३।६।९३] [सूत्रार्थ असार्वधातुकसंज्ञक सकार के परे रहते सकार को तकारादेश होता है।।७७३। [दु० वृ०]
सस्य तकारो भवति असार्वधातुके से परत:। जिघत्सति, वत्स्यति, दित्सा । असार्वधातुके इति किम् ? वस्से।।७७३।
[दु० टी०] सस्य । अर्थाद् धातोरेव सकारः सम्भवतीति धातुग्रहणं वृत्तौ नोच्यते।।७७३। [वि प०] सस्य। जिघत्सतीति। "अदेर्घस्ल सनद्यतन्योः" (३।४।७९) इति घस्लरादेशः।।७७३। [समीक्षा
"जिघत्सति, वत्स्यति' इत्यादि प्रयोगों के सिद्धयर्थ सकार को तकारादेश का विधान दोनों ही व्याकरणों में किया गया है। पाणिनि का सत्र है- “स: स्यार्धधातके" (अ० ७।४।४९)। सूत्र वृत्ति में 'धातो:' पद के न पढ़े जाने के सम्बन्ध में टीकाकार ने कहा है कि उसका तो परिज्ञान अर्थत: ही हो जाएगा, अत: वृत्तिकार ने 'धातोः' पद को वृत्ति में नहीं पढ़ा है।
[रूपसिद्धि]
१. जिघत्सति। अद्-घस् + सन् + ति। 'अद भक्षणे' (२।१) धातु से “धातोर्वा तमन्तादिच्छतिनैककर्तकात् ' (३।२।४) से 'सन' प्रत्यय, “अदेर्घस्ल सनद्यतन्योः" (३।४।७९) से 'अद्' को 'घस्ल' आदेश, “वसतिघसे: सात्' (३।७।२९) से अनिट्, "चण्परोक्षाचेक्रीयितसनन्तेषु'' (३।३।७) से 'घस्' को द्वित्व, "पूर्वोऽभ्यासः'' (३।३।४) से पूर्ववर्ती 'घस्' की अभ्याससंज्ञा, “अभ्यासस्यादिळञ्जनमवशेष्यम्' (३।३।९) से सकार का लोप, “द्वितीयचतुर्थयोः प्रथमतृतीयौ'' (३।३।११) से अभ्याससंज्ञक घकार को गकार, "कवर्गस्य चवर्ग:' (३।३।१३) से गकार को जकार, “सन्यवर्णस्य" (३।३।२६) से अकार को इकार, प्रकृत सूत्र से सकार को तकार, “ते धातवः''