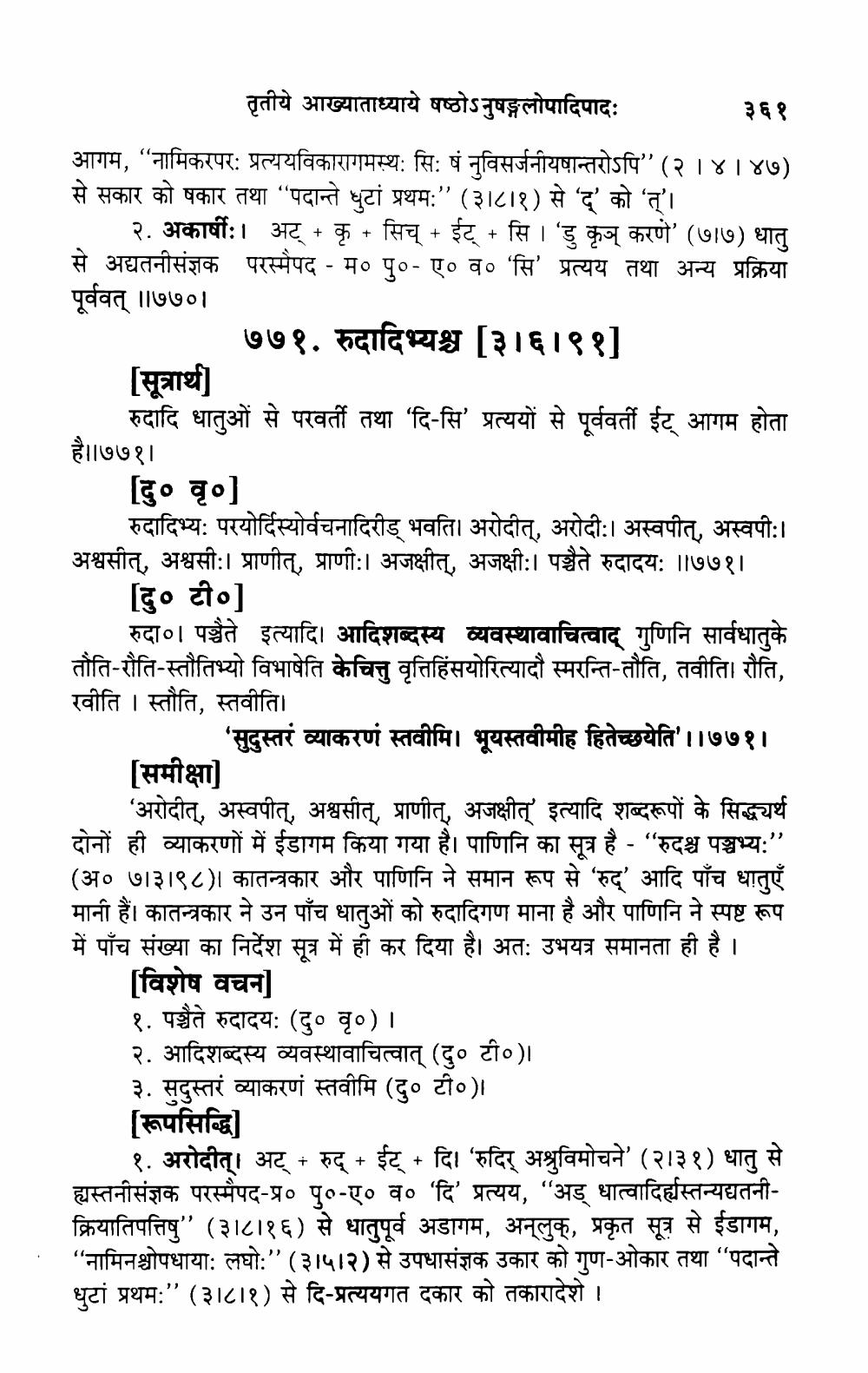________________
तृतीये आख्याताध्याये षष्ठोऽनुषङ्गलोपादिपादः ३६१ आगम, “नामिकरपरः प्रत्ययविकारागमस्थ: सि: षं नुविसर्जनीयषान्तरोऽपि' (२ । ४ । ४७) से सकार को षकार तथा “पदान्ते धुटां प्रथमः'' (३।८।१) से 'द्' को 'त्'।
२. अकार्षीः। अट् + कृ + सिच् + ईट् + सि । 'डु कृञ् करणे' (७१७) धातु से अद्यतनीसंज्ञक परस्मैपद - म० पु० - ए० व० 'सि' प्रत्यय तथा अन्य प्रक्रिया पूर्ववत् ।।७७०।
७७१. रुदादिभ्यश्च [३।६।९१] [सूत्रार्थ]
रुदादि धातुओं से परवर्ती तथा “दि-सि' प्रत्ययों से पूर्ववर्ती ईट् आगम होता है।।७७१।
[दु० वृ०]
रुदादिभ्यः परयोर्दिस्योर्वचनादिरीड् भवति। अरोदीत्, अरोदीः। अस्वपीत्, अस्वपीः। अश्वसीत्, अश्वसीः। प्राणीत्, प्राणी:। अजक्षीत्, अजक्षी:। पञ्चैते रुदादयः ॥७७१।
[दु० टी०]
रुदा०। पञ्चैते इत्यादि। आदिशब्दस्य व्यवस्थावाचित्वाद् गुणिनि सार्वधातुके तौति-रौति-स्तौतिभ्यो विभाषेति केचित्तु वृत्तिहिंसयोरित्यादौ स्मरन्ति-तौति, तवीति। रौति, रवीति । स्तौति, स्तवीति।
'सुदुस्तरं व्याकरणं स्तवीमि। भूयस्तवीमीह हितेच्छयेति' ।।७७१। [समीक्षा)
'अरोदीत, अस्वपीत, अश्वसीत. प्राणीत, अजक्षीत' इत्यादि शब्दरूपों के सिद्धयर्थ दोनों ही व्याकरणों में ईडागम किया गया है। पाणिनि का सूत्र है - "रुदश्च पञ्चभ्यः" (अ० ७।३।९८)। कातन्त्रकार और पाणिनि ने समान रूप से 'रुद्' आदि पाँच धातुएँ मानी हैं। कातन्त्रकार ने उन पाँच धातुओं को रुदादिगण माना है और पाणिनि ने स्पष्ट रूप में पाँच संख्या का निर्देश सूत्र में ही कर दिया है। अत: उभयत्र समानता ही है ।
[विशेष वचन] १. पञ्चैते रुदादयः (दु० वृ०)। २. आदिशब्दस्य व्यवस्थावाचित्वात् (दु० टी०)। ३. सदुस्तरं व्याकरणं स्तवीमि (दु० टी०)। [रूपसिद्धि]
१. अरोदीत्। अट् + रुद् + ईट् + दि। 'रुदिर अविमोचने' (२।३१) धात् से ह्यस्तनीसंज्ञक परस्मैपद-प्र० पु०-ए० व० 'दि' प्रत्यय, “अड् धात्वादिस्तिन्यद्यतनीक्रियातिपत्तिषु" (३।८।१६) से धातुपूर्व अडागम, अन्लुक्, प्रकृत सूत्र से ईडागम, "नामिनश्चोपधाया: लघो:' (३।५।२) से उपधासंज्ञक उकार को गुण-ओकार तथा “पदान्ते धुटां प्रथमः' (३।८।१) से दि-प्रत्ययगत दकार को तकारादेशे ।