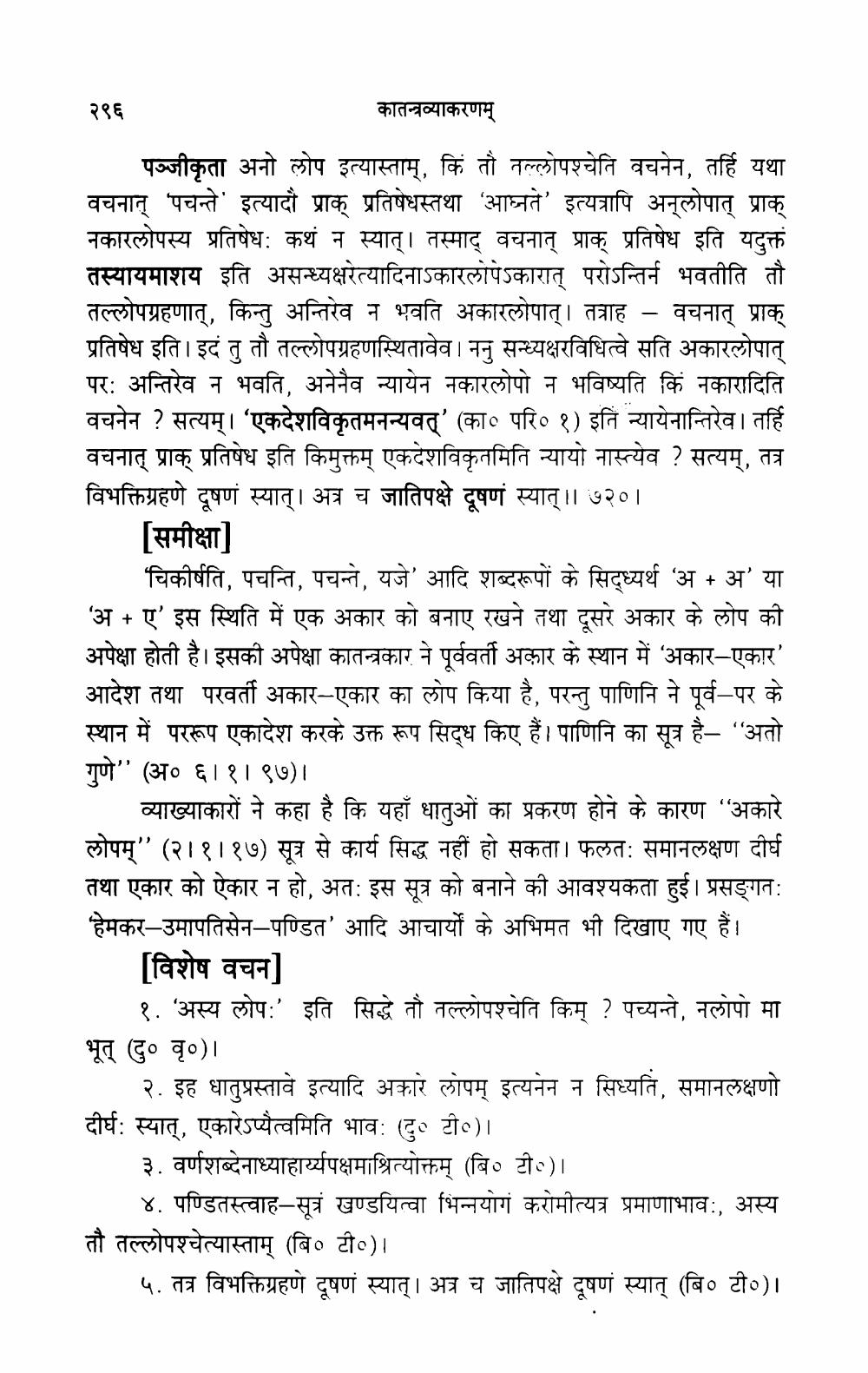________________
२९६
कातन्त्रव्याकरणम्
पञ्जीकृता अनो लोप इत्यास्ताम्, किं तो तल्लोपश्चेति वचनेन, तर्हि यथा वचनात् 'पचन्ते' इत्यादौ प्राक् प्रतिषेधस्तथा 'आनते' इत्यत्रापि अनुलोपात प्राक नकारलोपस्य प्रतिषेधः कथं न स्यात्। तस्माद् वचनात् प्राक् प्रतिषेध इति यदुक्तं तस्यायमाशय इति असन्ध्यक्षरेत्यादिनाऽकारलोपेऽकारात् परोऽन्तिर्न भवतीति तौ तल्लोपग्रहणात्, किन्तु अन्तिरेव न भवति अकारलोपात्। तत्राह - वचनात् प्राक् प्रतिषेध इति। इदं तु तौ तल्लोपग्रहणस्थितावेव। ननु सन्ध्यक्षरविधित्वे सति अकारलोपात् पर: अन्तिरेव न भवति, अनेनैव न्यायेन नकारलोपो न भविष्यति किं नकारादिति वचनेन ? सत्यम्। 'एकदेशविकृतमनन्यवत्' (काल परि० १) इति न्यायेनान्तिरेव। तर्हि वचनात् प्राक् प्रतिषेध इति किमुक्तम् एकदेशविकृतमिति न्यायो नास्त्येव ? सत्यम्, तत्र विभक्तिग्रहणे दूषणं स्यात्। अत्र च जातिपक्षे दूषणं स्यात् ।। ७२० ।
[समीक्षा]
'चिकीर्षति, पचन्ति, पचन्ते, यजे' आदि शब्दरूपों के सिद्ध्यर्थ 'अ + अ' या 'अ + ए' इस स्थिति में एक अकार को बनाए रखने तथा दूसरे अकार के लोप की अपेक्षा होती है। इसकी अपेक्षा कातन्त्रकार ने पूर्ववर्ती अकार के स्थान में 'अकार-एकार' आदेश तथा परवर्ती अकार-एकार का लोप किया है, परन्तु पाणिनि ने पूर्व–पर के स्थान में पररूप एकादेश करके उक्त रूप सिद्ध किए हैं। पाणिनि का सूत्र है- "अतो गुणे'' (अ० ६।१। ९७)।।
___ व्याख्याकारों ने कहा है कि यहाँ धातुओं का प्रकरण होने के कारण “अकारे लोपम्' (२।१ । १७) सूत्र से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। फलत: समानलक्षण दीर्घ तथा एकार को ऐकार न हो, अत: इस सूत्र को बनाने की आवश्यकता हुई। प्रसङ्गत: 'हेमकर-उमापतिसेन–पण्डित' आदि आचार्यों के अभिमत भी दिखाए गए हैं।
[विशेष वचन]
१. 'अस्य लोपः' इति सिद्धे तौ तल्लोपश्चेति किम् ? पच्यन्ते, नलोपो मा भूत् (टु० वृ०)।
२. इह धातुप्रस्तावे इत्यादि अकारे लोपम् इत्यनेन न सिध्यति, समानलक्षणो दीर्घ: स्यात्, एकारेऽप्यैत्वमिति भाव: (टु० टी०)।
३. वर्णशब्देनाध्याहार्यपक्षमाश्रित्योक्तम् (बि० टी०)।
४. पण्डितस्त्वाह-सूत्रं खण्डयित्वा भिन्नयोगं करोमीत्यत्र प्रमाणाभावः, अस्य तौ तल्लोपश्चेत्यास्ताम् (बि० टी०)।
५. तत्र विभक्तिग्रहणे दूषणं स्यात् । अत्र च जातिपक्षे दूषणं स्यात् (बि० टी०)।