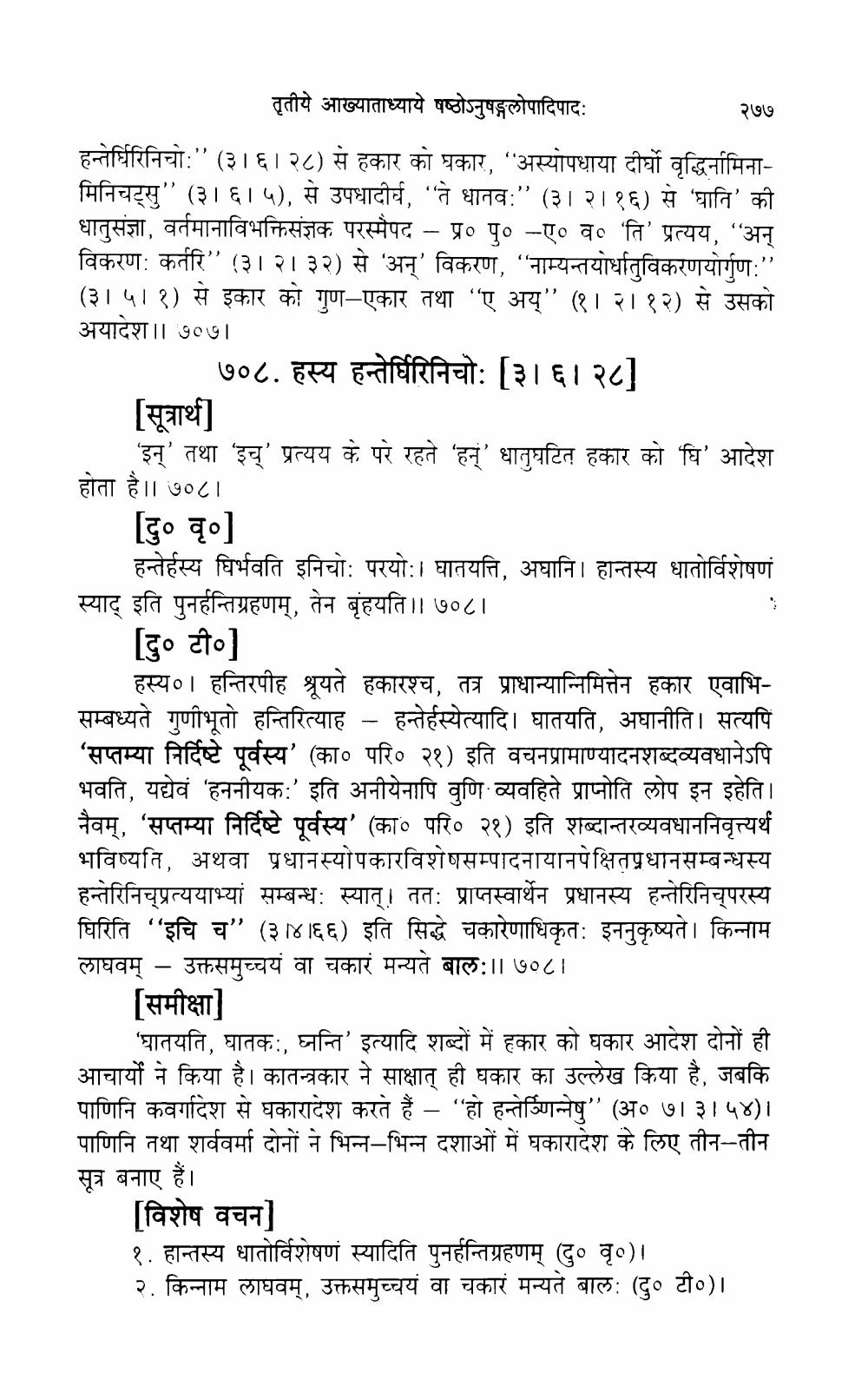________________
तृतीये आख्याताध्याये षष्ठोऽनुषङ्गलोपादिपादः
२७७ हन्तेर्घिरिनिचो:'' (३।६। २८) से हकार को घकार, "अस्योपधाया दी? वृद्धिर्नामिनामिनिचट्सु'' (३। ६। ५), से उपधादीर्च, "ते धातवः'' (३। २। १६) से 'घाति' की धातुसंज्ञा, वर्तमानाविभक्तिसंज्ञक परस्मैपद – प्र० पु० -ए० व० 'ति' प्रत्यय, “अन् विकरण: कर्तरि'' (३। २। ३२) से 'अन्' विकरण, “नाम्यन्तयोर्धातुविकरणयोर्गुणः" (३। ५। १) से इकार को गुण-एकार तथा “ए अय्'' (१। २। १२) से उसको अयादेश।। ७०७।
७०८. हस्य हन्तेपिरिनिचोः [३।६। २८] [सूत्रार्थ]
'इन्' तथा 'इच्' प्रत्यय के परे रहते ‘हन्' धातुघटित हकार को 'घि' आदेश होता है।। ७०८।
[दु० वृ०]
हन्तेर्हस्य धिर्भवति इनिचोः परयोः। घातयत्ति, अघानि। हान्तस्य धातोर्विशेषणं स्याद् इति पुनर्हन्तिग्रहणम्, तेन बृहयति।। ७०८ ।
[दु० टी०]
हस्य०। हन्तिरपीह श्रूयते हकारश्च, तत्र प्राधान्यान्निमित्तेन हकार एवाभिसम्बध्यते गणीभूतो हन्तिरित्याह – हन्तेर्हस्येत्यादि। घातयति, अघानीति। सत्यपि 'सप्तम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य' (का० परि० २१) इति वचनप्रामाण्यादनशब्दव्यवधानेऽपि भवति, यद्येवं 'हननीयकः' इति अनीयेनापि वुणि व्यवहिते प्राप्नोति लोप इन इहेति । नैवम्, 'सप्तम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य' (का० परि० २१) इति शब्दान्तरव्यवधाननिवृत्त्यर्थ भविष्यति, अथवा प्रधानस्योपकारविशेषसम्पादनायानपेक्षितप्रधानसम्बन्धस्य हन्तरिनिच्प्रत्ययाभ्यां सम्बन्ध: स्यात्। ततः प्राप्तस्वार्थेन प्रधानस्य हन्तेरिनिच्परस्य घिरिति "इचि च" (३।४।६६) इति सिद्धे चकारेणाधिकृतः इननुकृष्यते। किन्नाम लाघवम् – उक्तसमुच्चयं वा चकारं मन्यते बाल:।। ७०८ ।
[समीक्षा] _ 'घातयति, घातकः, घ्नन्ति' इत्यादि शब्दों में हकार को घकार आदेश दोनों ही आचार्यों ने किया है। कातन्त्रकार ने साक्षात् ही धकार का उल्लेख किया है, जबकि पाणिनि कवर्गादश से घकारादेश करते हैं – “हो हन्तेणिन्नेषु'' (अ० ७।३। ५४)। पाणिनि तथा शर्ववर्मा दोनों ने भिन्न-भिन्न दशाओं में घकारादेश के लिए तीन-तीन सूत्र बनाए हैं।
[विशेष वचन] १. हान्तस्य धातोर्विशेषणं स्यादिति पुनर्हन्तिग्रहणम् (दु० वृ०)। २. किन्नाम लाघवम्, उक्तसमुच्चयं वा चकारं मन्यते बाल: (दु० टी०)।