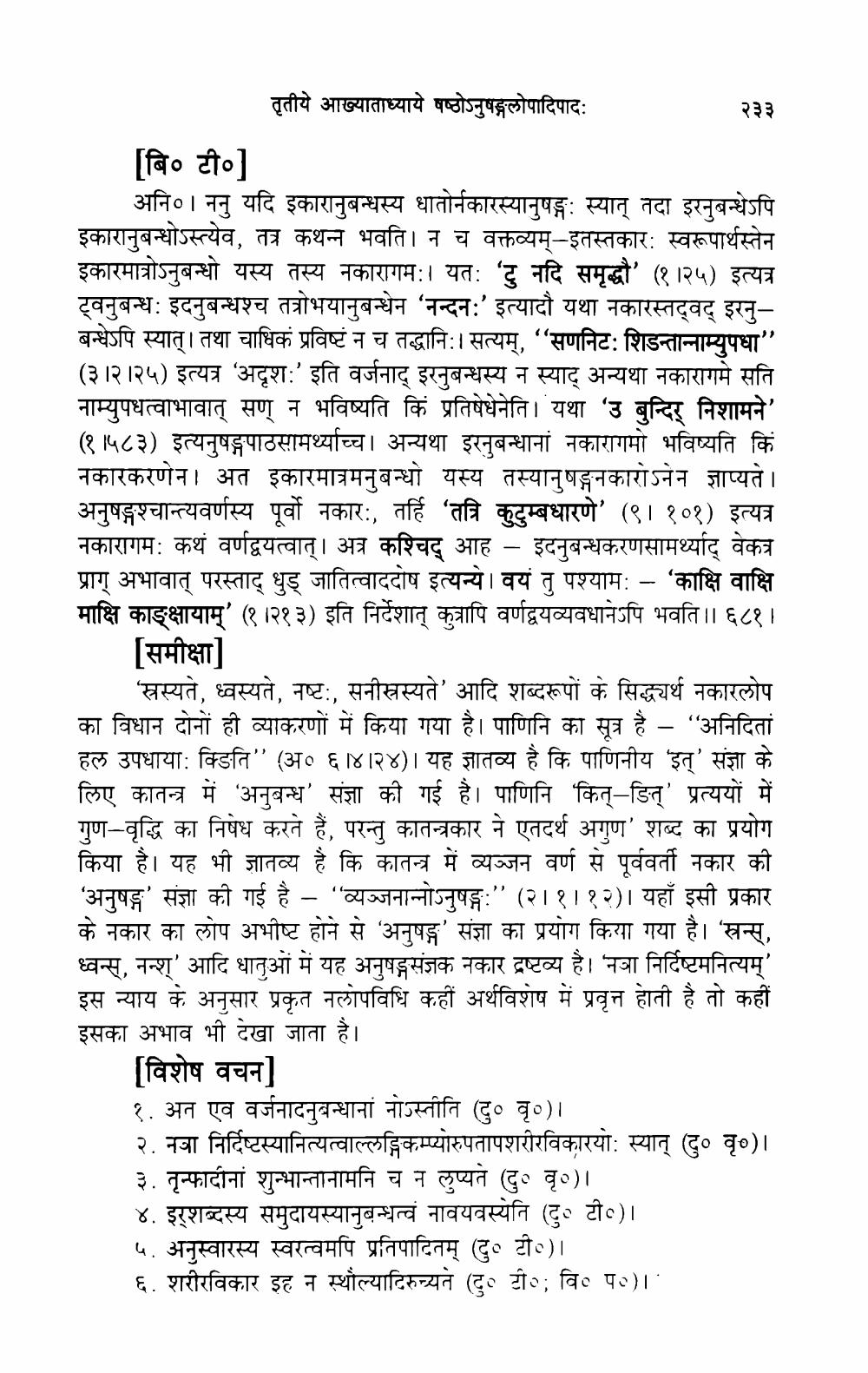________________
तृतीये आख्याताध्याये षष्ठोऽनुषङ्गलोपादिपाद:
२३३ [बि० टी०]
अनि० । ननु यदि इकारानुबन्धस्य धातोर्नकारस्यानुषङ्गः स्यात् तदा इरनुबन्धेऽपि इकारानुबन्धोऽस्त्येव, तत्र कथन्न भवति। न च वक्तव्यम्-इतस्तकार: स्वरूपार्थस्तेन इकारमात्रोऽनुबन्धो यस्य तस्य नकारागमः। यत: 'टु नदि समृद्धौ' (१।२५) इत्यत्र ट्वनुबन्ध: इदनुबन्धश्च तत्रोभयानुबन्धेन 'नन्दनः' इत्यादौ यथा नकारस्तद्वद् इरनुबन्धेऽपि स्यात्। तथा चाधिक प्रविष्टं न च तद्धानिः। सत्यम्, “सणनिट: शिडन्तान्नाम्युपधा" (३।२।२५) इत्यत्र 'अदृशः' इति वर्जनाद् इरनुबन्धस्य न स्याद् अन्यथा नकारागमे सति नाम्युपधत्वाभावात् सण न भविष्यति किं प्रतिषेधेनेति। यथा 'उ बुन्दिर निशामने' (१५८३) इत्यनुषङ्गपाठसामर्थ्याच्च। अन्यथा इरनुबन्धानां नकारागमो भविष्यति किं नकारकरणेन। अत इकारमात्रमनुबन्धो यस्य तस्यानुषङ्गनकारोऽनेन ज्ञाप्यते। अनुषङ्गश्चान्त्यवर्णस्य पूर्वो नकारः, तर्हि "तत्रि कुटुम्बधारणे' (९। १०१) इत्यत्र नकारागमः कथं वर्णद्वयत्वात्। अत्र कश्चिद् आह - इदनुबन्धकरणसामर्थ्याद् वेकत्र प्राग् अभावात् परस्ताद् धुड् जातित्वाददोष इत्यन्ये। वयं तु पश्यामः - ‘काक्षि वाक्षि माक्षि काङ्क्षायाम्' (१।२१३) इति निर्देशात् कुत्रापि वर्णद्वयव्यवधानेऽपि भवति ।। ६८१ ।
[समीक्षा] _ 'स्रस्यते, ध्वस्यते, नष्टः, सनीस्रस्यते' आदि शब्दरूपों के सिद्धयर्थ नकारलोप का विधान दोनों ही व्याकरणों में किया गया है। पाणिनि का सूत्र है – “अनिदितां हल उपधाया: क्ङिति'' (अ०६।४।२४)। यह ज्ञातव्य है कि पाणिनीय 'इत्' संज्ञा के लिए कातन्त्र में 'अनुबन्ध' संज्ञा की गई है। पाणिनि 'कित्-ङित्' प्रत्ययों में गुण-वृद्धि का निषध करते हैं, परन्तु कातन्त्रकार ने एतदर्थ अगुण' शब्द का प्रयोग किया है। यह भी ज्ञातव्य है कि कातन्त्र में व्यञ्जन वर्ण से पूर्ववर्ती नकार की 'अनुषङ्ग' संज्ञा की गई है - "व्यञ्जनान्नोऽनुषङ्गः' (२ । १ । १२)। यहाँ इसी प्रकार के नकार का लोप अभीष्ट होने से ‘अनुषङ्ग' संज्ञा का प्रयोग किया गया है। ‘स्रन्स्, ध्वन्स, नन्श्' आदि धातुओं में यह अनुषङ्गसंज्ञक नकार द्रष्टव्य है। नत्रा निर्दिष्टमनित्यम्' इस न्याय के अनुसार प्रकृत नलोपविधि कहीं अर्थविशेष में प्रवृत्त होती है तो कहीं इसका अभाव भी देखा जाता है।
[विशेष वचन] १. अत एव वर्जनादनुबन्धानां नोऽस्तीति (दु० वृ०)। २. नवा निर्दिष्टस्यानित्यत्वाल्लङ्गिकम्प्योरुपतापशरीरविकारयोः स्यात् (टु० वृ०)। ३. तृन्फादीनां शुम्भान्तानामनि च न लुप्यते (दु. वृ०)। ४. इर्शब्दस्य समुदायस्यानुबन्धत्वं नावयवस्यति (दु० टी०)। ५. अनुस्वारस्य स्वरत्वमपि प्रतिपादितम् (टु० टी०)। ६. शरीरविकार इह न स्थौल्यादिरुच्यते (टु० टी०; वि० प०)।