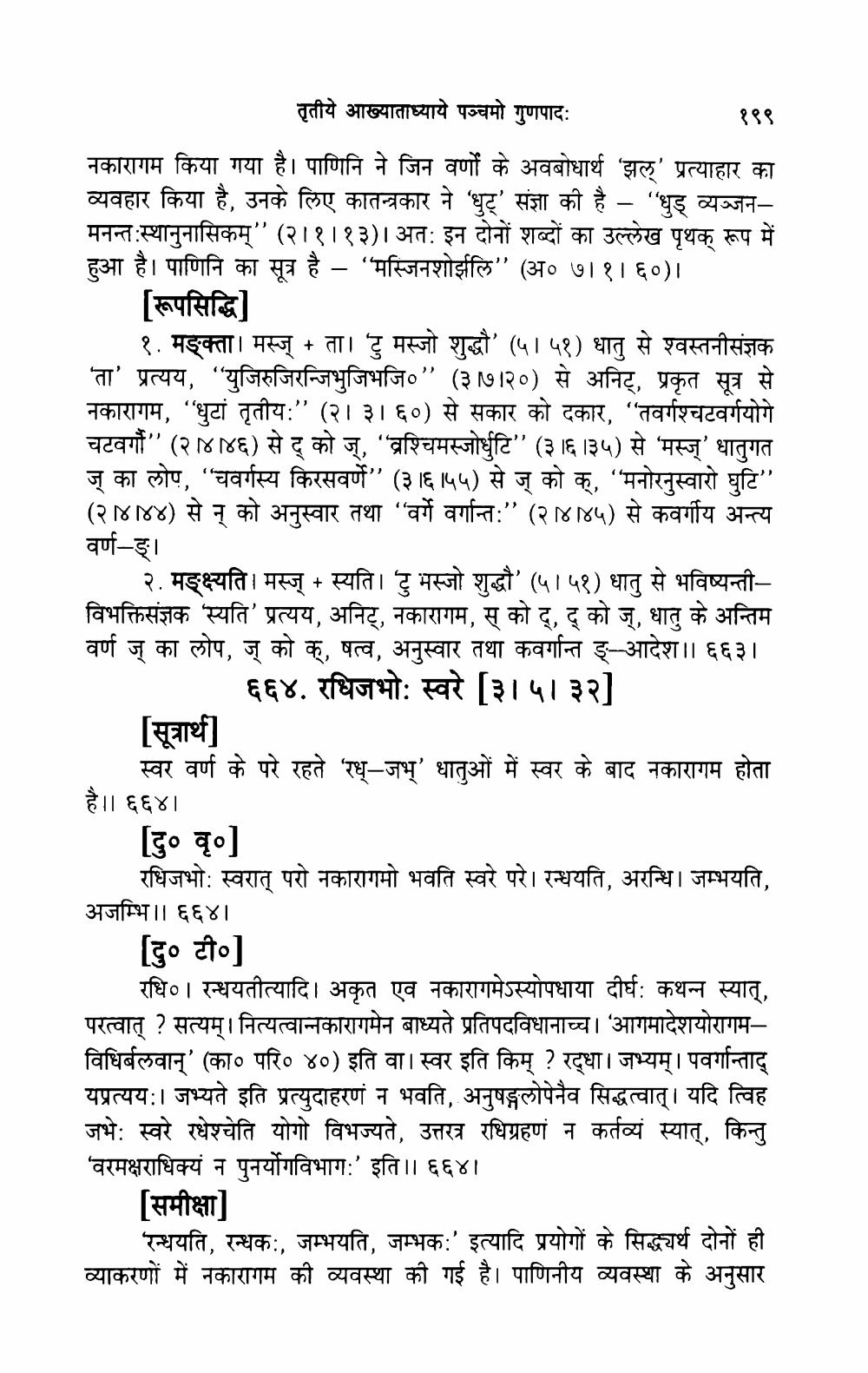________________
तृतीये आख्याताध्याये पञ्चमो गुणपाद:
१९९ नकारागम किया गया है। पाणिनि ने जिन वर्णों के अवबोधार्थ 'झल्' प्रत्याहार का व्यवहार किया है, उनके लिए कातन्त्रकार ने 'धुट्' संज्ञा की है – “धुड् व्यञ्जनमनन्त:स्थानुनासिकम्' (२।१।१३)। अत: इन दोनों शब्दों का उल्लेख पृथक् रूप में हुआ है। पाणिनि का सूत्र है – “मस्जिनशोझलि' (अ० ७।१।६०)।
[रूपसिद्धि]
१. मङ्क्ता । मस्ज् + ता। 'टु मस्जो शुद्धौ' (५। ५१) धातु से श्वस्तनीसंज्ञक 'ता' प्रत्यय, “युजिरुजिरन्जिभुजिभजि०" (३७।२०) से अनिट्, प्रकृत सूत्र से नकारागम, “धुटां तृतीयः' (२। ३। ६०) से सकार को दकार, “तवर्गश्चटवर्गयोगे चटव!'' (२।४।४६) से द् को ज्, “वृश्चिमस्जोधुटि'' (३।६।३५) से 'मस्ज्' धातुगत ज् का लोप, “चवर्गस्य किरसवर्णे' (३।६।५५) से ज् को क्, “मनोरनुस्वारो घुटि" (२।४।४४) से न् को अनुस्वार तथा “वर्गे वर्गान्तः' (२।४।४५) से कवर्गीय अन्त्य वर्ण-ङ्।
२. मक्ष्यति। मस्ज् + स्यति। टु भस्जो शुद्धौ' (५। ५१) धातु से भविष्यन्तीविभक्तिसंज्ञक 'स्यति' प्रत्यय, अनिट, नकारागम, स को द्, द् को ज, धातु के अन्तिम वर्ण ज् का लोप, ज् को क्, षत्व, अनुस्वार तथा कवर्गान्त ङ्-आदेश।। ६६३।
६६४. रधिजभोः स्वरे [३। ५। ३२] [सूत्रार्थ]
स्वर वर्ण के परे रहते ‘रध्–जभ्' धातुओं में स्वर के बाद नकारागम होता है।। ६६४।
[दु० वृ०]
रधिजभो: स्वरात् परो नकारागमो भवति स्वरे परे। रन्धयति, अरन्धि। जम्भयति, अजम्भि।। ६६४।
[दु० टी०]
रधि०। रन्धयतीत्यादि। अकृत एव नकारागमेऽस्योपधाया दीर्घः कथन्न स्यात्, परत्वात् ? सत्यम्। नित्यत्वान्नकारागमेन बाध्यते प्रतिपदविधानाच्च। आगमादेशयोरागमविधिर्बलवान्' (का० परि० ४०) इति वा। स्वर इति किम् ? रद्धा। जभ्यम् । पवर्गान्ताद् यप्रत्ययः। जभ्यते इति प्रत्युदाहरणं न भवति, अनुषङ्गलोपेनैव सिद्धत्वात्। यदि त्विह जभे: स्वरे रधेश्चेति योगो विभज्यते, उत्तरत्र रधिग्रहणं न कर्तव्यं स्यात्, किन्तु 'वरमक्षराधिक्यं न पुनर्योगविभागः' इति।। ६६४।
[समीक्षा]
'रन्धयति, रन्धकः, जम्भयति, जम्भकः' इत्यादि प्रयोगों के सिद्ध्यर्थ दोनों ही व्याकरणों में नकारागम की व्यवस्था की गई है। पाणिनीय व्यवस्था के अनुसार