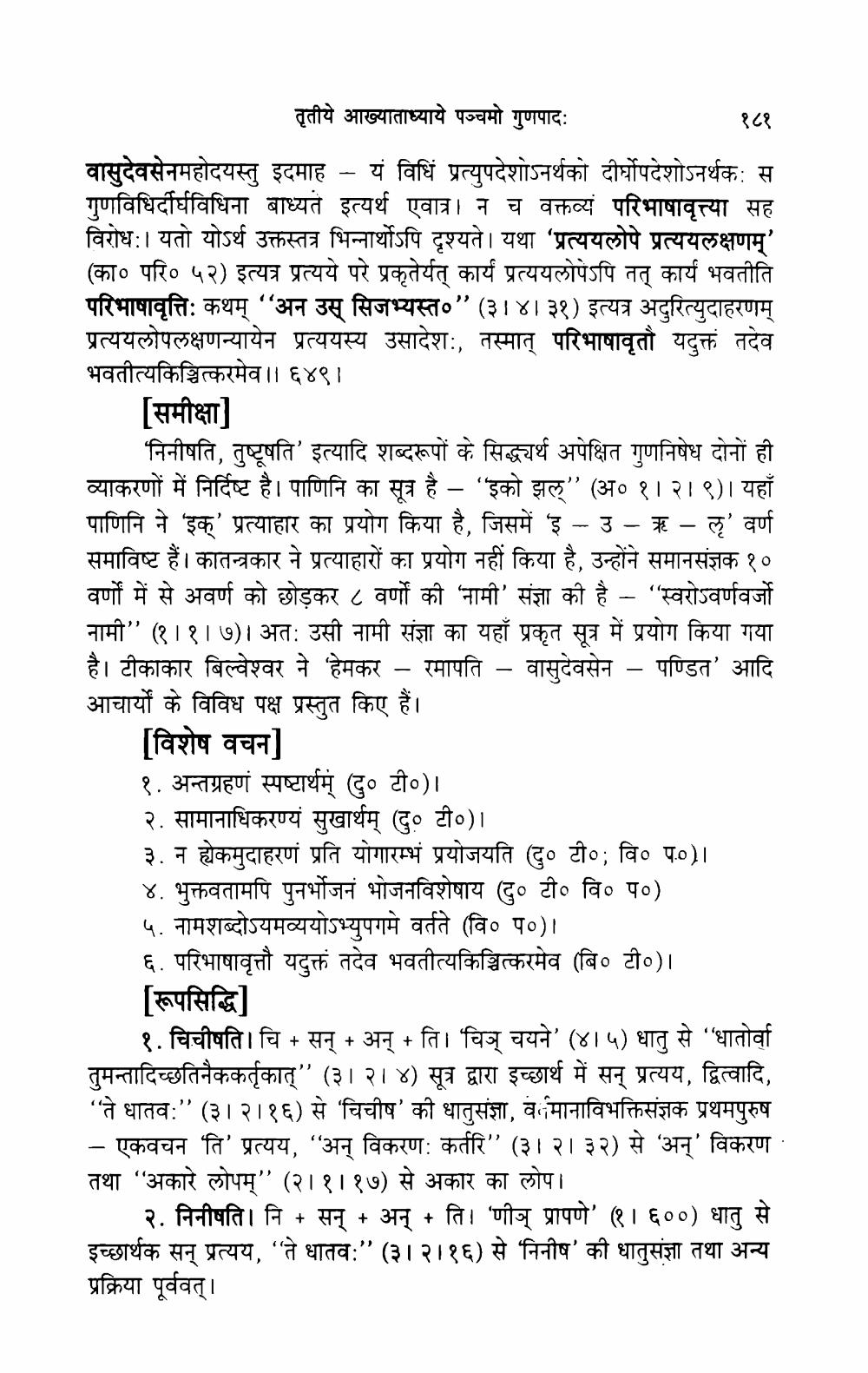________________
१८१
तृतीये आख्याताध्याये पञ्चमो गुणपादः वासुदेवसेनमहोदयस्तु इदमाह - यं विधिं प्रत्युपदेशोऽनर्थको दीर्घोपदेशोऽनर्थकः स गणविधिर्दीर्घविधिना बाध्यते इत्यर्थ एवात्र। न च वक्तव्यं परिभाषावृत्त्या सह विरोधः। यतो योऽर्थ उक्तस्तत्र भिन्नार्थोऽपि दृश्यते। यथा 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्' (का० परि० ५२) इत्यत्र प्रत्यये परे प्रकृतेर्यत् कार्य प्रत्ययलोपेऽपि तत् कार्य भवतीति परिभाषावृत्तिः कथम् “अन उस सिजभ्यस्त०" (३।४। ३१) इत्यत्र अदुरित्युदाहरणम् प्रत्ययलोपलक्षणन्यायेन प्रत्ययस्य उसादेशः, तस्मात् परिभाषावृतो यदुक्तं तदेव भवतीत्यकिञ्चित्करमेव।। ६४९ ।
[समीक्षा]
'निनीषति, तुष्टूपति' इत्यादि शब्दरूपों के सिद्धयर्थ अपेक्षित गुणनिषेध दोनों ही व्याकरणों में निर्दिष्ट है। पाणिनि का सूत्र है – “इको झल्' (अ० १। २। ९)। यहाँ पाणिनि ने 'इक्' प्रत्याहार का प्रयोग किया है, जिसमें 'इ - उ – ऋ - लु' वर्ण समाविष्ट हैं। कातन्त्रकार ने प्रत्याहारों का प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने समानसंज्ञक १० वर्गों में से अवर्ण को छोड़कर ८ वर्णों की 'नामी' संज्ञा की है - "स्वरोऽवर्णवों नामी' (१ । १। ७)। अत: उसी नामी संज्ञा का यहाँ प्रकृत सूत्र में प्रयोग किया गया है। टीकाकार बिल्वेश्वर ने हेमकर - रमापति – वासुदेवसेन – पण्डित' आदि आचार्यों के विविध पक्ष प्रस्तुत किए हैं।
[विशेष वचन] १. अन्तग्रहणं स्पष्टार्थम् (दु० टी०)। २. सामानाधिकरण्यं सुखार्थम् (दु० टी०)। ३. न ह्येकमदाहरणं प्रति योगारम्भं प्रयोजयति (८० टी०; वि० प.०)। ४. भुक्तवतामपि पुनर्भोजनं भोजनविशेषाय (दु० टी० वि० प०) ५. नामशब्दोऽयमव्ययोऽभ्युपगमे वर्तते (वि० प०)। ६. परिभाषावृत्तौ यदुक्तं तदेव भवतीत्यकिञ्चित्करमेव (बि० टी०)। [रूपसिद्धि]
१. चिचीषति। चि + सन् + अन् + ति। 'चिञ् चयने' (४। ५) धातु से 'धातोर्वा तुमन्तादिच्छतिनैककर्तृकात्'' (३। २। ४) सूत्र द्वारा इच्छार्थ में सन् प्रत्यय, द्वित्वादि, "ते धातवः'' (३।२।१६) से 'चिचीष' की धातुसंज्ञा, वर्तमानाविभक्तिसंज्ञक प्रथमपुरुष - एकवचन 'ति' प्रत्यय, “अन् विकरण: कर्तरि" (३। २। ३२) से 'अन्' विकरण तथा "अकारे लोपम्'' (२। १ । १७) से अकार का लोप।
२. निनीषति। नि + सन् + अन् + ति। ‘णीञ् प्रापणे' (१। ६००) धातु से इच्छार्थक सन् प्रत्यय, "ते धातवः' (३। २।१६) से 'निनीष' की धातुसंज्ञा तथा अन्य प्रक्रिया पूर्ववत्।