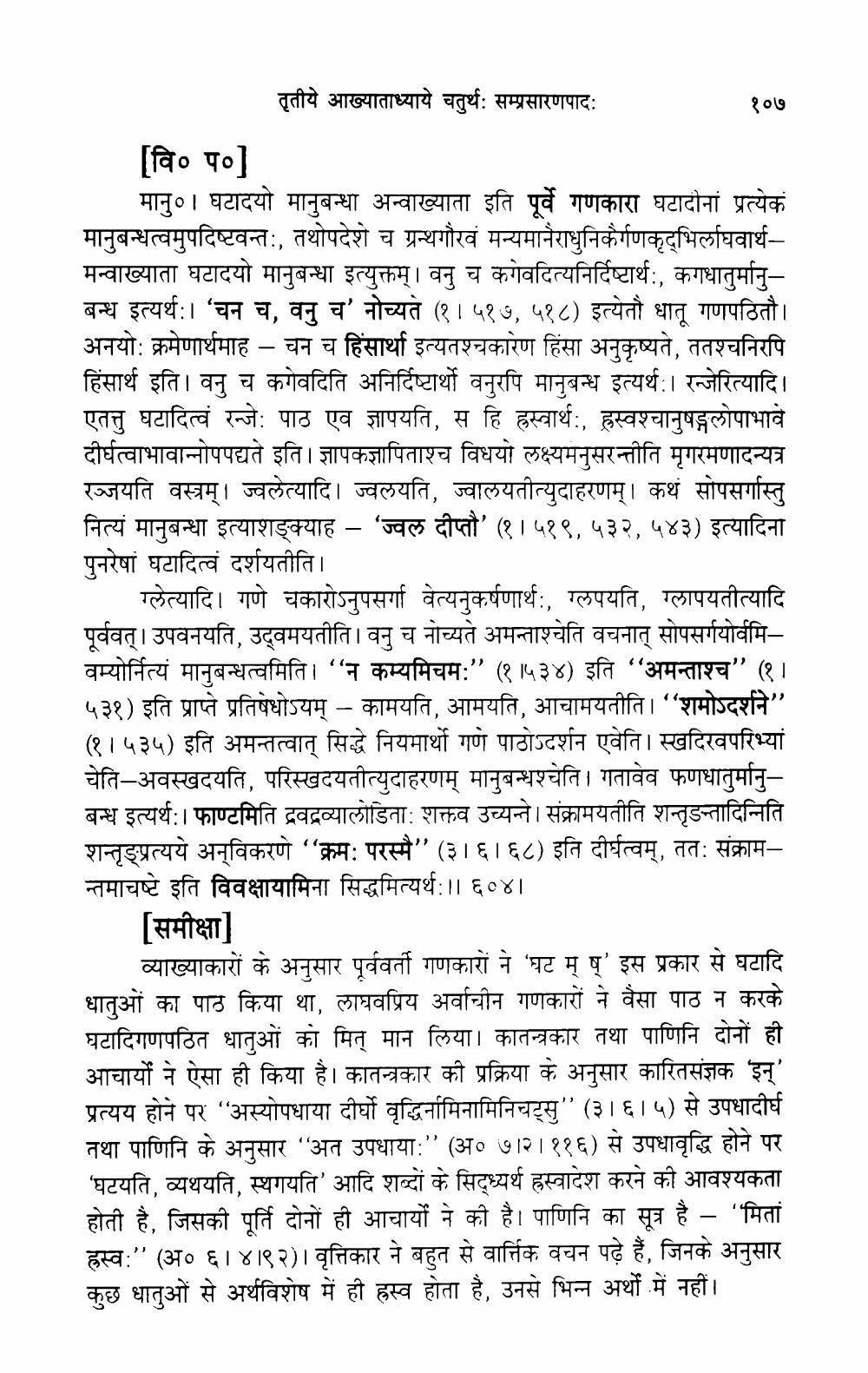________________
१०७
तृतीये आख्याताध्याये चतुर्थः सम्प्रसारणपाद:
१०७ [वि० प०]
मानु० । घटादयो मानुबन्धा अन्वाख्याता इति पूर्वे गणकारा घटादीनां प्रत्येक मानुबन्धत्वमुपदिष्टवन्तः, तथोपदेशे च ग्रन्थगौरवं मन्यमानैराधुनिकैर्गणकृद्भिर्लाघवार्थमन्वाख्याता घटादयो मानुबन्धा इत्युक्तम्। वनु च कगेवदित्यनिर्दिष्टार्थ:, कगधातुर्मानुबन्ध इत्यर्थः। 'चन च, वनु च' नोच्यते (१ । ५१७, ५१८) इत्येतो धातू गणपठितौ। अनयो: क्रमेणार्थमाह – चन च हिंसार्था इत्यतश्चकारेण हिंसा अनुकृष्यते, ततश्चनिरपि हिंसार्थ इति। वन च कगेवदिति अनिर्दिष्टार्थो वनुरपि मानबन्ध इत्यर्थः। रन्जेरित्यादि। एतत्तु घटादित्वं रन्जे: पाठ एव ज्ञापयति, स हि ह्रस्वार्थः, ह्रस्वश्चानुषगलोपाभावे दीर्घत्वाभावान्नोपपद्यते इति । ज्ञापकज्ञापिताश्च विधयो लक्ष्यमनुसरन्तीति मृगरमणादन्यत्र रञ्जयति वस्त्रम्। ज्वलेत्यादि। ज्वलयति, ज्वालयतीत्युदाहरणम्। कथं सोपसर्गास्तु नित्यं मानुबन्धा इत्याशझ्याह – 'ज्वल दीप्तौ' (१ । ५१९, ५३२, ५४३) इत्यादिना पुनरेषां घटादित्वं दर्शयतीति। __ग्लेत्यादि। गणे चकारोऽनुपसर्गा वेत्यनुकर्षणार्थ:, ग्लपयति, ग्लापयतीत्यादि पूर्ववत्। उपवनयति, उद्वमयतीति। वनु च नोच्यते अमन्ताश्चेति वचनात् सोपसर्गयोर्वमिवम्योर्नित्यं मानुबन्धत्वमिति। "न कम्यमिचमः” (१५३४) इति “अमन्ताश्च” (१ । ५३१) इति प्राप्ते प्रतिषेधोऽयम् – कामयति, आमयति, आचामयतीति। "शमोऽदर्शने" (१ । ५३५) इति अमन्तत्वात् सिद्धे नियमार्थो गणे पाठोऽदर्शन एवेति। स्खदिरवपरिभ्यां चेति-अवस्खदयति, परिस्खदयतीत्युदाहरणम् मानुबन्धश्चेति। गतावेव फणधातुर्मानुबन्ध इत्यर्थः। फाण्टमिति द्रवद्रव्यालोडिता: शक्तव उच्यन्ते। संक्रामयतीति शन्तृङन्तादिन्निति शन्तप्रत्यये अनविकरणे "क्रमः परस्मै" (३। ६ । ६८) इति दीर्घत्वम्, तत: संक्रामन्तमाचष्टे इति विवक्षायामिना सिद्धमित्यर्थः।। ६०४।
[समीक्षा]
व्याख्याकारों के अनुसार पूर्ववर्ती गणकारों ने 'घट म् ष्' इस प्रकार से घटादि धातुओं का पाठ किया था, लाघवप्रिय अर्वाचीन गणकारों ने वैसा पाठ न करके घटादिगणपठित धातुओं को मित् मान लिया। कातन्त्रकार तथा पाणिनि दोनों ही आचार्यों ने ऐसा ही किया है। कातन्त्रकार की प्रक्रिया के अनुसार कारितसंज्ञक 'इन्' प्रत्यय होने पर “अस्योपधाया दीर्घो वृद्धि मिनामिनिचट्स' (३। ६ । ५) से उपधादीर्घ तथा पाणिनि के अनुसार "अत उपधायाः' (अ० ७।२ । ११६) से उपधावृद्धि होने पर 'घटयति, व्यथयति, स्थगयति' आदि शब्दों के सिद्ध्यर्थ ह्रस्वादेश करने की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति दोनों ही आचार्यों ने की है। पाणिनि का सूत्र है – “मितां ह्रस्वः'' (अ० ६। ४।९२)। वृत्तिकार ने बहुत से वार्त्तिक वचन पढ़े हैं, जिनके अनुसार कुछ धातुओं से अर्थविशेष में ही ह्रस्व होता है, उनसे भिन्न अर्थों में नहीं।