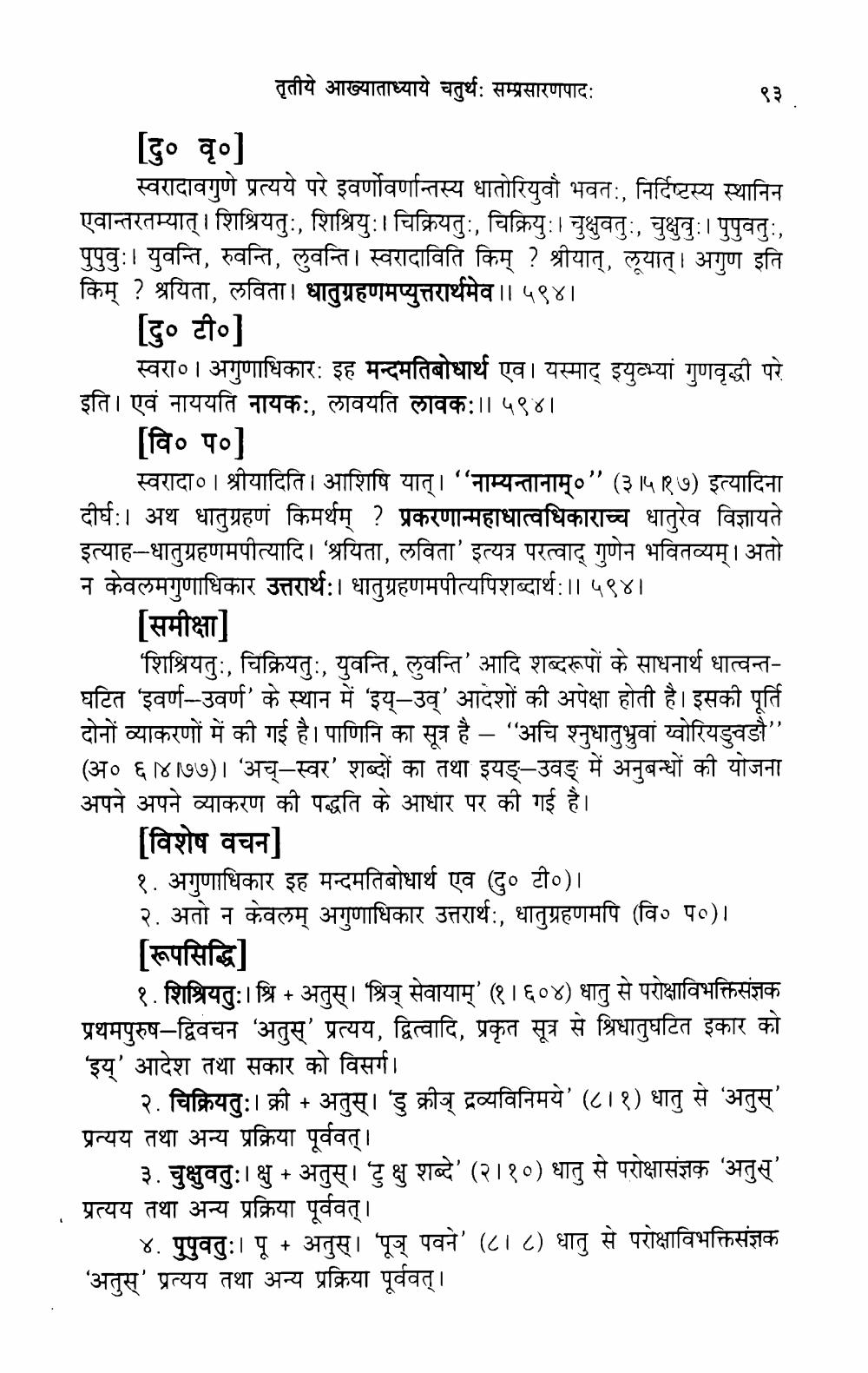________________
तृतीये आख्याताध्याये चतुर्थः सम्प्रसारणपादः [दु० वृ०]
स्वरादावगुणे प्रत्यये परे इवर्णोवर्णान्तस्य धातोरियुवो भवतः, निर्दिष्टस्य स्थानिन एवान्तरतम्यात्। शिश्रियतुः, शिश्रियुः । चिक्रियतुः, चिक्रियुः । चुक्षुवतुः, चुक्षुत्रुः । पुपुवतुः, पुपुवुः। युवन्ति, रुवन्ति, लुवन्ति। स्वरादाविति किम् ? श्रीयात्, लूयात्। अगुण इति किम् ? श्रयिता, लविता। धातुग्रहणमप्युत्तरार्थमेव ।। ५९४ ।
[दु० टी०]
स्वरा० । अगुणाधिकार: इह मन्दमतिबोधार्थ एव। यस्माद् इयुत्भ्यां गुणवृद्धी परे इति। एवं नाययति नायकः, लावयति लावकः।। ५९४।
[वि० प०]
स्वरादा० । श्रीयादिति। आशिषि यात्। “नाम्यन्तानाम्०" (३।५।१७) इत्यादिना दीर्घः। अथ धातुग्रहणं किमर्थम् ? प्रकरणान्महाधात्वधिकाराच्च धातुरेव विज्ञायते इत्याह-धातुग्रहणमपीत्यादि। 'श्रयिता, लविता' इत्यत्र परत्वाद् गुणेन भवितव्यम् । अतो न केवलमगुणाधिकार उत्तरार्थः। धातुग्रहणमपीत्यपिशब्दार्थः।। ५९४।
[समीक्षा]
'शिश्रियतुः, चिक्रियतुः, युवन्ति, लुवन्ति' आदि शब्दरूपों के साधनार्थ धात्वन्तघटित 'इवर्ण-उवर्ण' के स्थान में 'इय्-उव्' आदेशों की अपेक्षा होती है। इसकी पूर्ति दोनों व्याकरणों में की गई है। पाणिनि का सूत्र है – “अचि श्नधातुभ्रवां य्वोरियड्वडौ" (अ० ६।४७७)। 'अच्–स्वर' शब्दों का तथा इयङ्-उवङ् में अनुबन्धों की योजना अपने अपने व्याकरण की पद्धति के आधार पर की गई है।
[विशेष वचन] १. अगुणाधिकार इह मन्दमतिबोधार्थ एव (दु० टी०)। २. अतो न केवलम् अगुणाधिकार उत्तरार्थः, धातुग्रहणमपि (वि० प०)। [रूपसिद्धि
१. शिश्रियतुः। श्रि + अतुस्। श्रिज् सेवायाम्' (१ । ६०४) धातु से परोक्षाविभक्तिसंज्ञक प्रथमपुरुष-द्विवचन 'अतुस्' प्रत्यय, द्वित्वादि, प्रकृत सूत्र से श्रिधातुघटित इकार को 'इय्' आदेश तथा सकार को विसर्ग।
२. चिक्रियतुः। क्री + अतुस्। 'डु क्रीज् द्रव्यविनिमये' (८ । १) धातु से 'अतुस्' प्रत्यय तथा अन्य प्रक्रिया पूर्ववत्।
३. चुक्षुवतुः। क्षु + अतुस्। 'टु क्षु शब्दे' (२ । १०) धातु से परोक्षासंज्ञक 'अतुस्' . प्रत्यय तथा अन्य प्रक्रिया पूर्ववत्।
४. पुपुवतुः। पू + अतुस्। 'पूञ् पवने' (८। ८) धातु से परोक्षाविभक्तिसंज्ञक 'अतुस्' प्रत्यय तथा अन्य प्रक्रिया पूर्ववत् ।