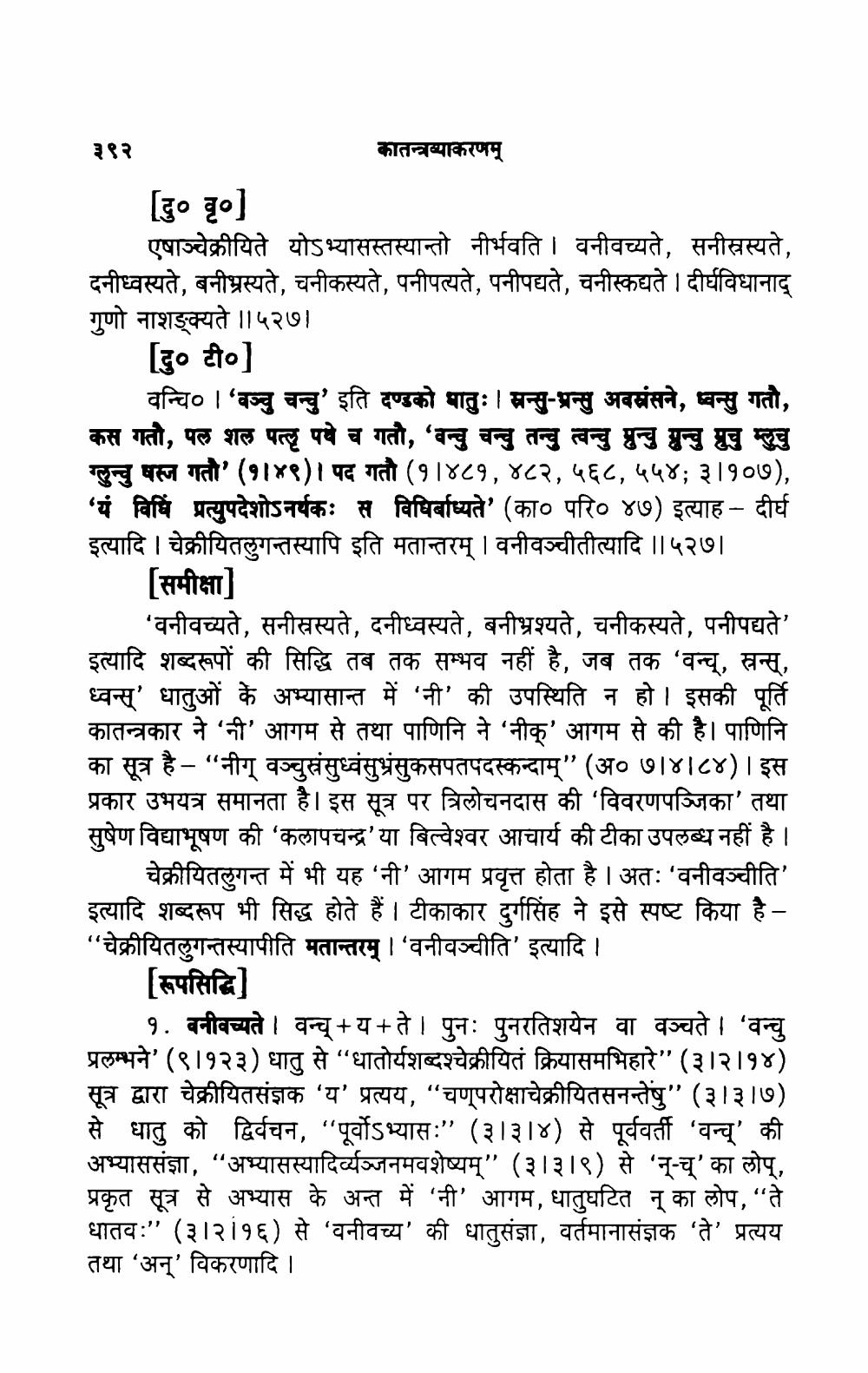________________
३९२
कातन्त्रव्याकरणम्
[दु० वृ०]
एषाञ्चेक्रीयिते योऽभ्यासस्तस्यान्तो नीर्भवति । वनीवच्यते, सनीस्रस्यते, दनीध्वस्यते, बनीभ्रस्यते, चनीकस्यते, पनीपत्यते, पनीपद्यते, चनीस्कद्यते । दीर्घविधानाद् गुणो नाशझ्यते ।। ५२७।
[दु० टी०]
वन्चि० । 'वञ्चु चन्चु' इति दण्डको धातुः । मन्सु-प्रन्सु अवलंसने, वन्सु गतो, कस गती, पल शल पत्लू पवे च गतो, 'वन्दु चन्चु तन्चु त्वन्चु मन्चु गुन्चु सूचु म्लुचु ग्लुन्चु षस्ज गती' (१।४९)। पद गतौ (१।४८१, ४८२, ५६८, ५५४; ३।१०७), 'यं विधि प्रत्युपदेशोऽनर्यकः स विधिर्बाध्यते' (का० परि० ४७) इत्याह - दीर्घ इत्यादि । चेक्रीयितलुगन्तस्यापि इति मतान्तरम् । वनीवञ्चीतीत्यादि ।। ५२७।
[समीक्षा]
'वनीवच्यते, सनीस्रस्यते, दनीध्वस्यते, बनीभ्रश्यते, चनीकस्यते, पनीपद्यते' इत्यादि शब्दरूपों की सिद्धि तब तक सम्भव नहीं है, जब तक 'वन्च, स्रन्स, ध्वन्स्' धातुओं के अभ्यासान्त में 'नी' की उपस्थिति न हो। इसकी पूर्ति कातन्त्रकार ने 'नी' आगम से तथा पाणिनि ने 'नीक्' आगम से की है। पाणिनि का सूत्र है- “नीग् वञ्चुलंसुध्वंसुभ्रंसुकसपतपदस्कन्दाम्" (अ०७।४।८४) । इस प्रकार उभयत्र समानता है। इस सूत्र पर त्रिलोचनदास की 'विवरणपञ्जिका' तथा सुषेण विद्याभूषण की 'कलापचन्द्र' या बित्वेश्वर आचार्य की टीका उपलब्ध नहीं है |
चेक्रीयितलुगन्त में भी यह 'नी' आगम प्रवृत्त होता है । अतः 'वनीवञ्चीति' इत्यादि शब्दरूप भी सिद्ध होते हैं। टीकाकार दुर्गसिंह ने इसे स्पष्ट किया है"चेक्रीयितलुगन्तस्यापीति मतान्तरम् । 'वनीवञ्चीति' इत्यादि ।
[रूपसिद्धि]
१. वनीवच्यते । वन्च् + य + ते । पुनः पुनरतिशयेन वा वञ्चते । 'वन्चु प्रलम्भने' (९।१२३) धातु से “धातोर्यशब्दश्चेक्रीयितं क्रियासमभिहारे" (३।२।१४) सूत्र द्वारा चेक्रीयितसंज्ञक 'य' प्रत्यय, “चण्परोक्षाचेक्रीयितसनन्तेषु" (३।३।७) से धातु को द्विर्वचन, "पूर्वोऽभ्यासः'' (३।३।४) से पूर्ववर्ती 'वन्च' की अभ्याससंज्ञा, "अभ्यासस्यादिळञ्जनमवशेष्यम्” (३।३।९) से 'न्-च्' का लोप्, प्रकृत सूत्र से अभ्यास के अन्त में 'नी' आगम, धातुघटित न का लोप, "ते धातवः” (३।२।१६) से 'वनीवच्य' की धातुसंज्ञा, वर्तमानासंज्ञक 'ते' प्रत्यय तथा 'अन्' विकरणादि ।