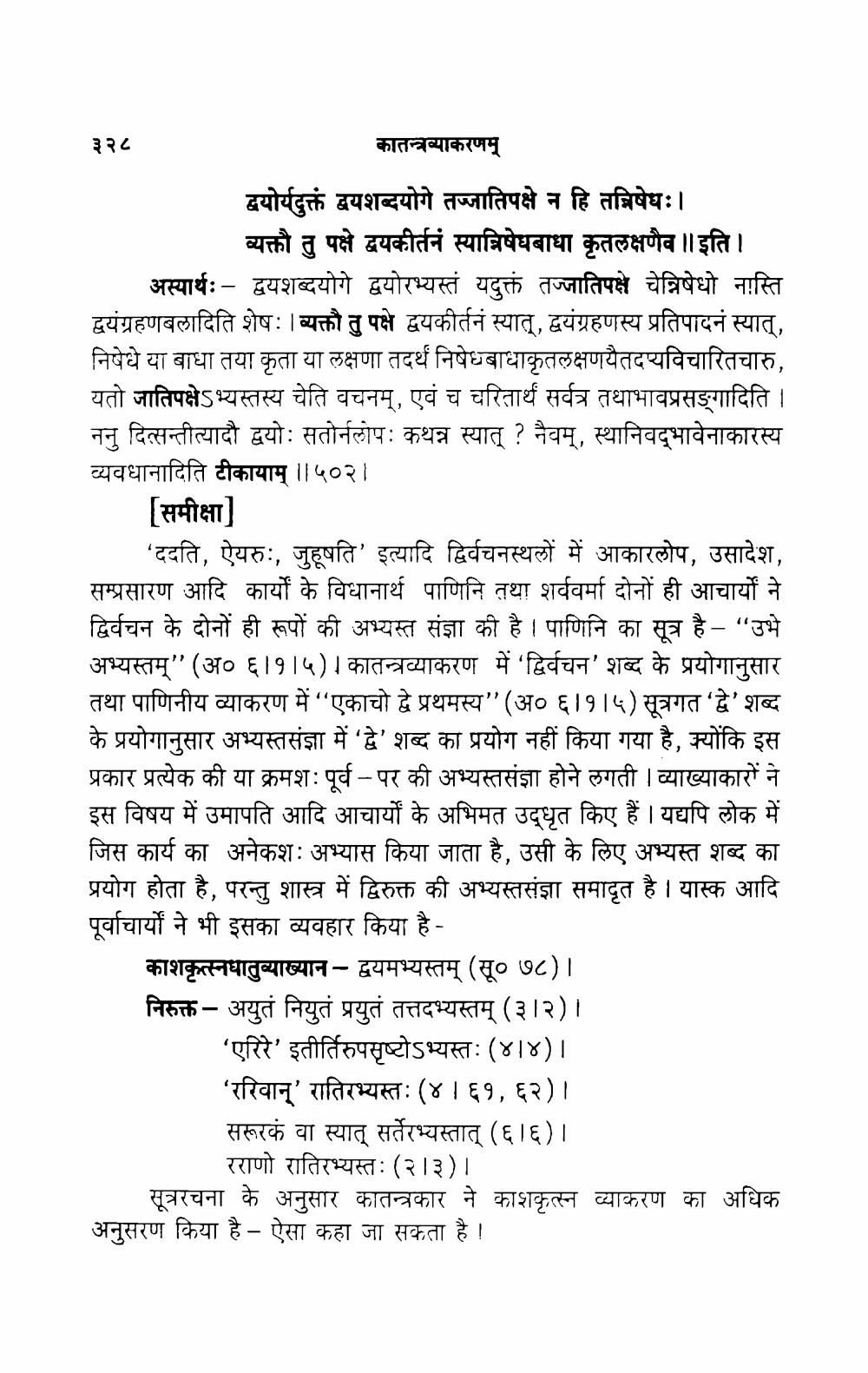________________
३२८
कातन्त्रव्याकरणम्
द्वयोर्यदुक्तं वयशब्दयोगे तज्जातिपक्षे न हि तनिषेधः।
व्यक्तौ तु पक्षे द्वयकीर्तनं स्यानिषेधबाधा कृतलक्षणैव ॥इति । अस्यार्थः- द्वयशब्दयोगे द्वयोरभ्यस्तं यदुक्तं तज्जातिपक्षे चेन्निषेधो नास्ति द्वयंग्रहणबलादिति शेषः । व्यक्तौ तु पक्षे द्वयकीर्तनं स्यात्, द्वयंग्रहणस्य प्रतिपादनं स्यात्, निषेधे या बाधा तया कृता या लक्षणा तदर्थं निषेधबाधाकृतलक्षणयैतदप्यविचारितचारु, यतो जातिपक्षेऽभ्यस्तस्य चेति वचनम्, एवं च चरितार्थं सर्वत्र तधाभावप्रसङगादिति । ननु दित्सन्तीत्यादौ द्वयोः सतोनलोपः कथन्न स्यात् ? नैवम्, स्थानिवद्भावेनाकारस्य व्यवधानादिति टीकायाम् ।। ५०२ ।
[समीक्षा]
'ददति, ऐयरुः, जुहूषति' इत्यादि द्विर्वचनस्थलों में आकारलोप, उसादेश, सम्प्रसारण आदि कार्यों के विधानार्थ पाणिनि तथा शर्ववर्मा दोनों ही आचार्यों ने द्विर्वचन के दोनों ही रूपों की अभ्यस्त संज्ञा की है । पाणिनि का सूत्र है - "उभे अभ्यस्तम्" (अ०६।१।५) । कातन्त्रव्याकरण में द्विवचन' शब्द के प्रयोगानुसार तथा पाणिनीय व्याकरण में "एकाचो द्वे प्रथमस्य' (अ०६।१।५) सूत्रगत 'द्वे' शब्द के प्रयोगानुसार अभ्यस्तसंज्ञा में 'द्वे' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि इस प्रकार प्रत्येक की या क्रमशः पूर्व- पर की अभ्यस्तसंज्ञा होने लगती | व्याख्याकारों ने इस विषय में उमापति आदि आचार्यों के अभिमत उद्धृत किए हैं । यद्यपि लोक में जिस कार्य का अनेकशः अभ्यास किया जाता है, उसी के लिए अभ्यस्त शब्द का प्रयोग होता है, परन्तु शास्त्र में द्विरुक्त की अभ्यस्तसंज्ञा समादृत है । यास्क आदि पूर्वाचार्यों ने भी इसका व्यवहार किया है -
काशकृत्स्नधातुव्याख्यान- द्वयमभ्यस्तम् (सू० ७८) । निरुक्त- अयुतं नियुतं प्रयुतं तत्तदभ्यस्तम् (३।२)।
‘एरिरे' इतीर्तिरुपसृष्टोऽभ्यस्तः (४।४) । 'ररिवान्' रातिरभ्यस्तः (४ । ६१, ६२) । सरूरकं वा स्यात् सर्तेरभ्यस्तात् (६।६)।
रराणो रातिरभ्यस्त : (२३)। सूत्ररचना के अनुसार कातन्त्रकार ने काशकृत्स्न व्याकरण का अधिक अनुसरण किया है - ऐसा कहा जा सकता है ।