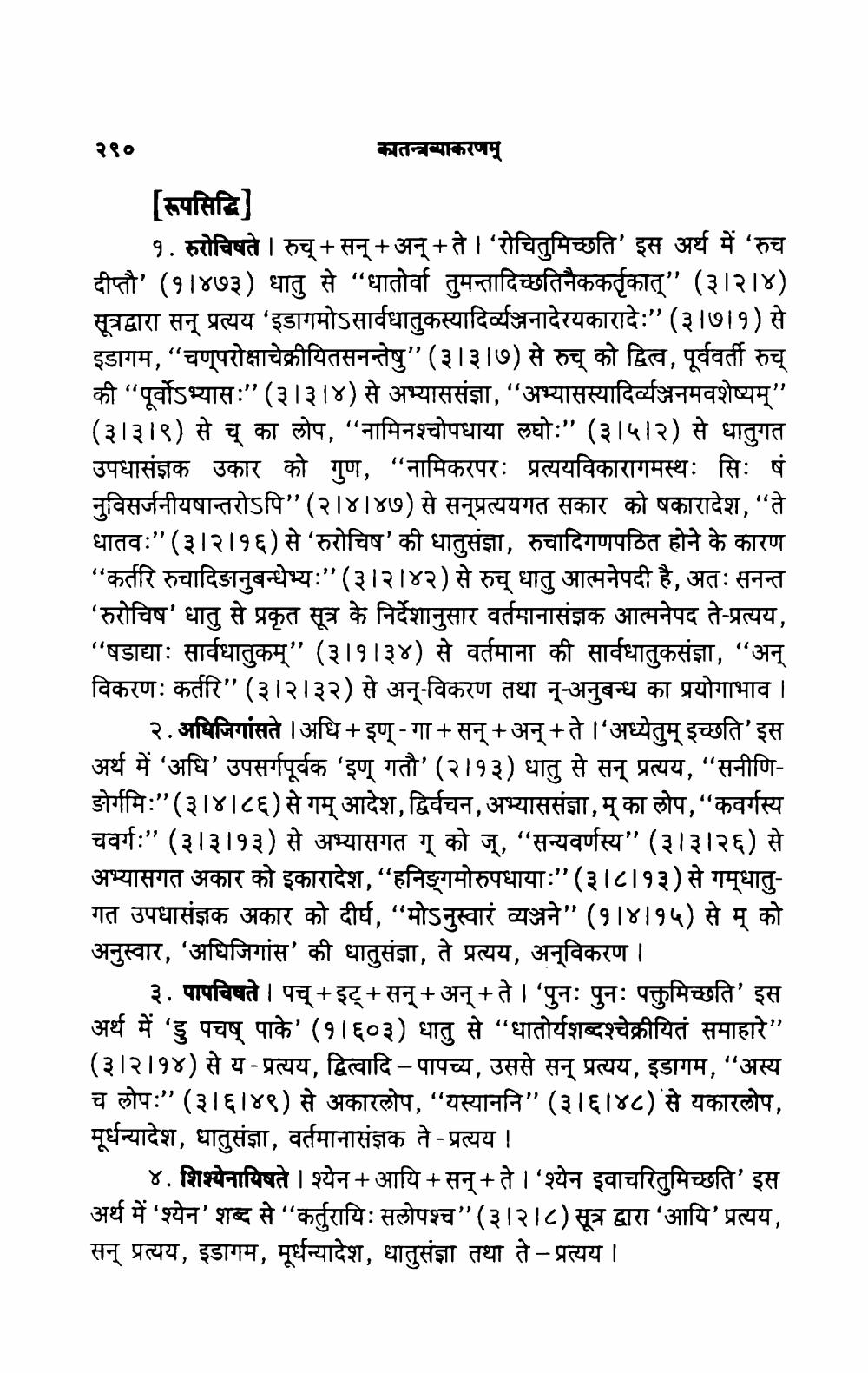________________
२९०
कातन्त्रयाकरणम्
[रूपसिद्धि
१. रुरोचिषते । रुच् + सन् + अन् + ते । ‘रोचितुमिच्छति' इस अर्थ में 'रुच दीप्तौ' (१।४७३) धातु से “धातोर्वा तुमन्तादिच्छतिनैककर्तृकात्" (३।२।४) सूत्रद्वारा सन् प्रत्यय 'इडागमोऽसार्वधातुकस्यादिळञ्जनादेरयकारादेः' (३।७।१) से इडागम, “चण्परोक्षाचेक्रीयितसनन्तेषु" (३।३।७) से रुच् को द्वित्व, पूर्ववर्ती रुच् की “पूर्वोऽभ्यासः" (३।३।४) से अभ्याससंज्ञा, “अभ्यासस्यादिर्व्यञ्जनमवशेष्यम्" (३।३।९) से च का लोप, “नामिनश्चोपधाया लघोः" (३।५।२) से धातुगत उपधासंज्ञक उकार को गुण, “नामिकरपरः प्रत्ययविकारागमस्थः सिः षं नुविसर्जनीयषान्तरोऽपि" (२।४।४७) से सन्प्रत्ययगत सकार को षकारादेश, “ते धातवः" (३।२।१६) से 'रुरोचिष' की धातुसंज्ञा, रुचादिगणपठित होने के कारण "कर्तरि रुचादिङानुबन्धेभ्यः" (३।२।४२) से रुच् धातु आत्मनेपदी है, अतः सनन्त 'रुरोचिष' धातु से प्रकृत सूत्र के निर्देशानुसार वर्तमानासंज्ञक आत्मनेपद ते-प्रत्यय, "षडाद्याः सार्वधातुकम्" (३।१।३४) से वर्तमाना की सार्वधातुकसंज्ञा, “अन् विकरणः कर्तरि" (३।२।३२) से अन्-विकरण तथा न्-अनुबन्ध का प्रयोगाभाव |
२.अधिनिगांसते । अधि + इण् - गा + सन् + अन् + ते । अध्येतुम् इच्छति' इस अर्थ में 'अधि' उपसर्गपूर्वक 'इण् गतौ' (२।१३) धातु से सन् प्रत्यय, “सनीणिङोर्गमिः" (३।४।८६) से गम् आदेश, द्विर्वचन, अभ्याससंज्ञा, म् का लोप, “कवर्गस्य चवर्ग:" (३।३।१३) से अभ्यासगत ग् को ज्, “सन्यवर्णस्य" (३।३।२६) से अभ्यासगत अकार को इकारादेश, "हनिङ्गमोरुपधायाः" (३।८।१३) से गमधातुगत उपधासंज्ञक अकार को दीर्घ, "मोऽनुस्वारं व्यञ्जने" (१।४।१५) से म् को अनुस्वार, 'अधिजिगांस' की धातुसंज्ञा, ते प्रत्यय, अविकरण।
३. पापचिषते । पच् + इट् + सन् + अन् + ते । 'पुनः पुनः पक्तुमिच्छति' इस अर्थ में 'डु पचष् पाके' (१।६०३) धातु से "धातोर्यशब्दश्चेक्रीयितं समाहारे" (३।२।१४) से य-प्रत्यय, द्वित्वादि-पापच्य, उससे सन् प्रत्यय, इडागम, “अस्य च लोपः” (३।६।४९) से अकारलोप, “यस्याननि" (३।६।४८) से यकारलोप, मूर्धन्यादेश, धातुसंज्ञा, वर्तमानासंज्ञक ते-प्रत्यय ।
४. शिश्येनायिषते । श्येन + आयि + सन् + ते । श्येन इवाचरितुमिच्छति' इस अर्थ में 'श्येन' शब्द से "कर्तुरायिः सलोपश्च" (३।२।८) सूत्र द्वारा ‘आयि' प्रत्यय, सन् प्रत्यय, इडागम, मूर्धन्यादेश, धातुसंज्ञा तथा ते- प्रत्यय ।