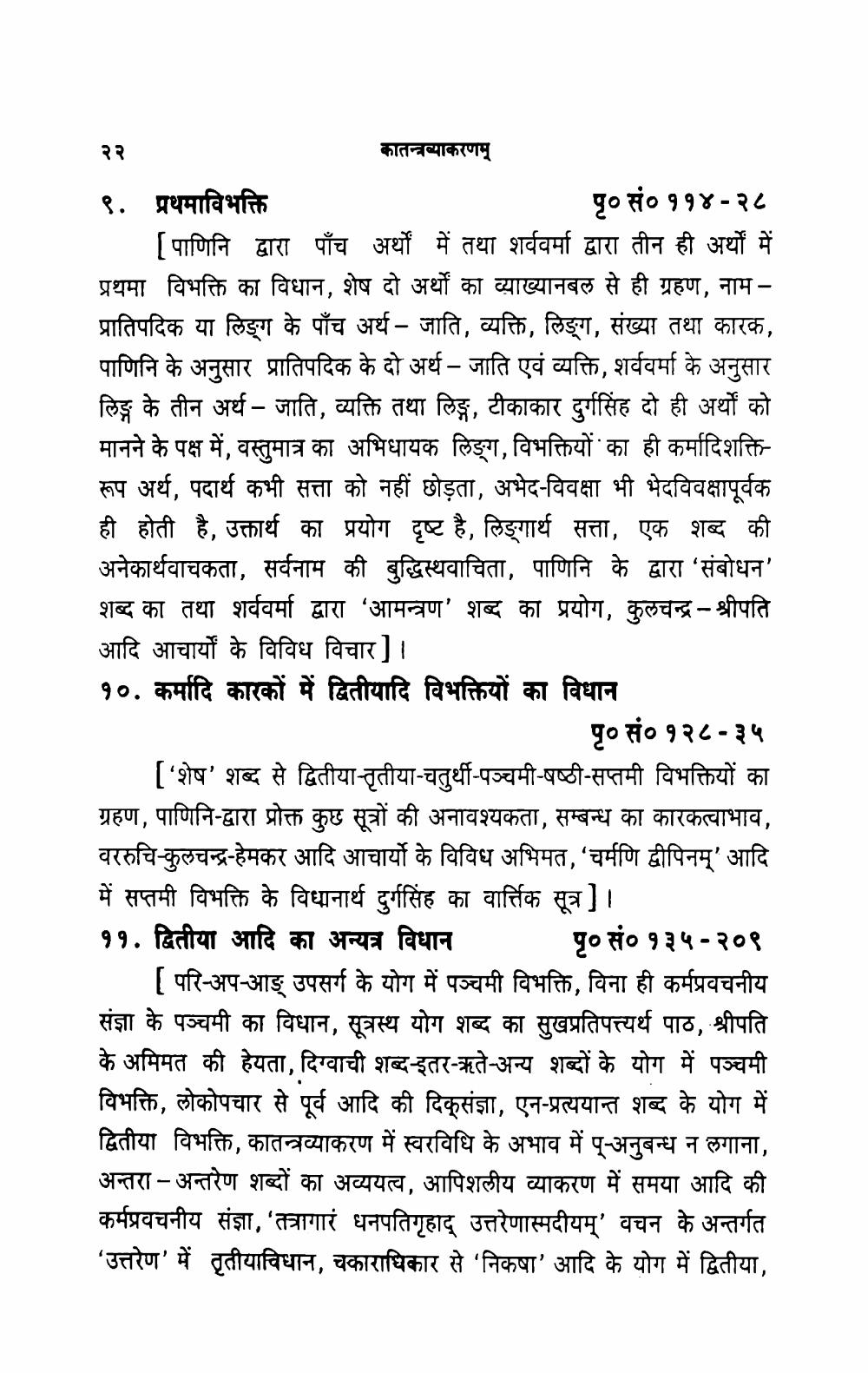________________
२२
कातन्त्रव्याकरणम्
९. प्रथमाविभक्ति
पृ० सं० ११४-२८ [पाणिनि द्वारा पाँच अर्थों में तथा शर्ववर्मा द्वारा तीन ही अर्थों में प्रथमा विभक्ति का विधान, शेष दो अर्थों का व्याख्यानबल से ही ग्रहण, नामप्रातिपदिक या लिङ्ग के पाँच अर्थ - जाति, व्यक्ति, लिङ्ग, संख्या तथा कारक, पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक के दो अर्थ - जाति एवं व्यक्ति, शर्ववर्मा के अनुसार लिङ्ग के तीन अर्थ - जाति, व्यक्ति तथा लिङ्ग, टीकाकार दुर्गसिंह दो ही अर्थों को मानने के पक्ष में, वस्तुमात्र का अभिधायक लिङ्ग, विभक्तियों का ही कर्मादिशक्ति रूप अर्थ, पदार्थ कभी सत्ता को नहीं छोड़ता, अभेद-विवक्षा भी भेदविवक्षापूर्वक ही होती है, उक्तार्थ का प्रयोग दृष्ट है, लिङ्गार्थ सत्ता, एक शब्द की अनेकार्थवाचकता, सर्वनाम की बुद्धिस्थवाचिता, पाणिनि के द्वारा ‘संबोधन' शब्द का तथा शर्ववर्मा द्वारा ‘आमन्त्रण' शब्द का प्रयोग, कुलचन्द्र - श्रीपति आदि आचार्यों के विविध विचार] | १०. कर्मादि कारकों में द्वितीयादि विभक्तियों का विधान
पृ० सं०१२८-३५ ['शेष' शब्द से द्वितीया-तृतीया-चतुर्थी-पञ्चमी-षष्ठी-सप्तमी विभक्तियों का ग्रहण, पाणिनि-द्वारा प्रोक्त कुछ सूत्रों की अनावश्यकता, सम्बन्ध का कारकत्वाभाव, वररुचि-कुलचन्द्र-हेमकर आदि आचार्यों के विविध अभिमत, 'चर्मणि द्वीपिनम्' आदि में सप्तमी विभक्ति के विधानार्थ दुर्गसिंह का वार्तिक सूत्र] । ११. द्वितीया आदि का अन्यत्र विधान पृ० सं० १३५ -२०९
[परि-अप-आङ् उपसर्ग के योग में पञ्चमी विभक्ति, विना ही कर्मप्रवचनीय संज्ञा के पञ्चमी का विधान, सूत्रस्थ योग शब्द का सुखप्रतिपत्त्यर्थ पाठ, श्रीपति के अमिमत की हेयता, दिग्वाची शब्द-इतर-ऋते-अन्य शब्दों के योग में पञ्चमी विभक्ति, लोकोपचार से पूर्व आदि की दिक्संज्ञा, एन-प्रत्ययान्त शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति, कातन्त्रव्याकरण में स्वरविधि के अभाव में प्-अनुबन्ध न लगाना, अन्तरा - अन्तरेण शब्दों का अव्ययत्व, आपिशलीय व्याकरण में समया आदि की कर्मप्रवचनीय संज्ञा, 'तत्रागारं धनपतिगृहाद् उत्तरेणास्मदीयम्' वचन के अन्तर्गत 'उत्तरेण' में तृतीयाविधान, चकाराधिकार से 'निकषा' आदि के योग में द्वितीया,