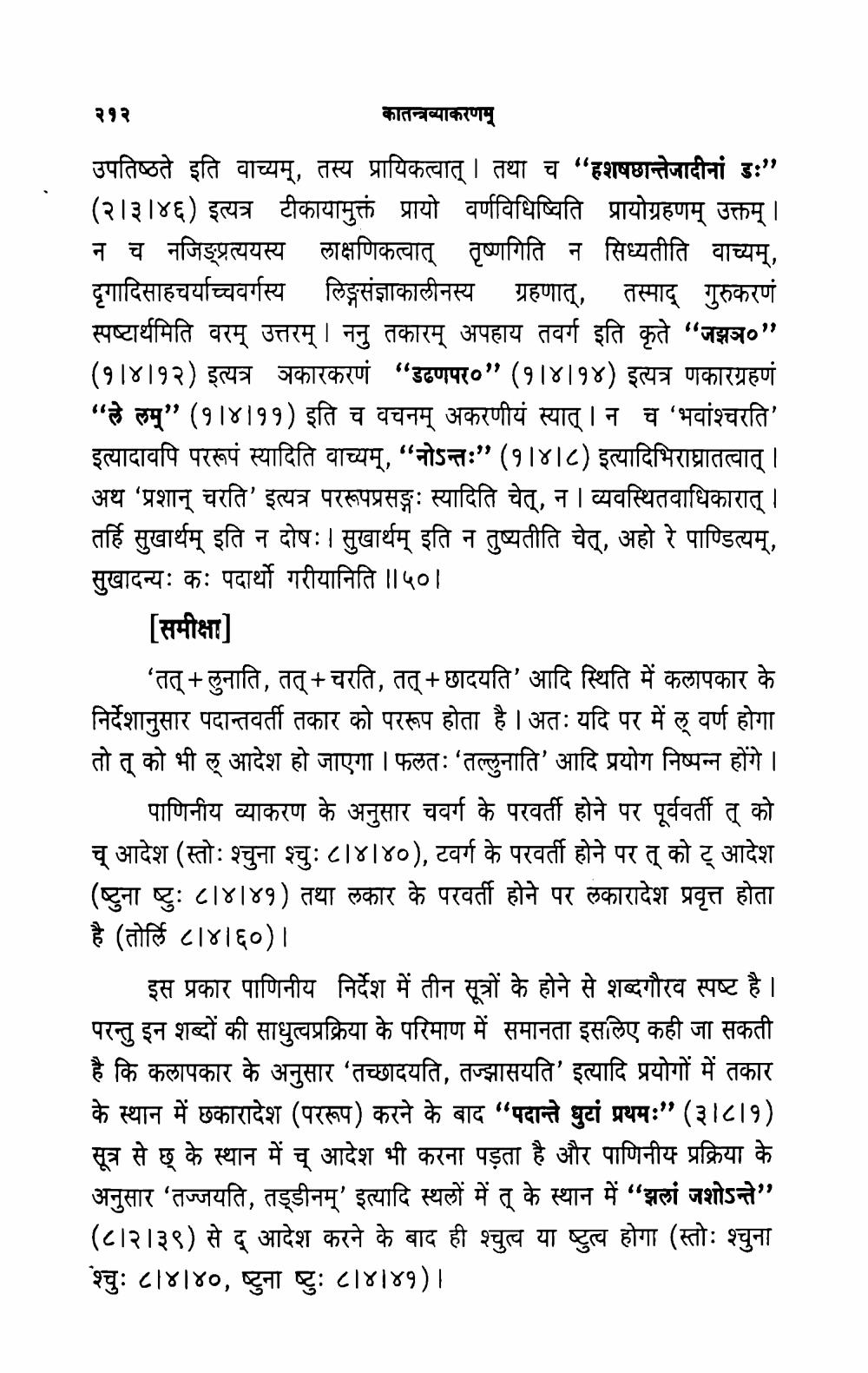________________
कातन्त्रव्याकरणम्
उपतिष्ठते इति वाच्यम्, तस्य प्रायिकत्वात् । तथा च "हशषछान्तेजादीनां ड: " (२।३।४६) इत्यत्र टीकायामुक्तं प्रायो वर्णविधिष्विति प्रायोग्रहणम् उक्तम् । न च नजिङ्प्रत्ययस्य लाक्षणिकत्वात् तृष्णगिति न सिध्यतीति वाच्यम्, दृगादिसाहचर्याच्चवर्गस्य लिङ्गसंज्ञाकालीनस्य ग्रहणात्, तस्माद् गुरुकरणं स्पष्टार्थमिति वरम् उत्तरम् । ननु तकारम् अपहाय तवर्ग इति कृते " जझञ०" (१।४।१२ ) इत्यत्र ञकारकरणं " डढणपर०" (१।४।१४ ) इत्यत्र णकारग्रहणं “ले लम्” (१।४।११) इति च वचनम् अकरणीयं स्यात् । न च 'भवांश्चरति’ इत्यादावपि पररूपं स्यादिति वाच्यम्, “नोऽन्तः " (१।४।८) इत्यादिभिराघ्रातत्वात् । अथ 'प्रशान् चरति' इत्यत्र पररूपप्रसङ्गः स्यादिति चेत्, न । व्यवस्थितवाधिकारात् । तर्हि सुखार्थम् इति न दोषः । सुखार्थम् इति न तुष्यतीति चेत्, अहो रे पाण्डित्यम्, सुखादन्यः कः पदार्थो गरीयानिति || ५० |
[समीक्षा]
‘तत् + लुनाति, तत् + चरति, तत् + छादयति' आदि स्थिति में कलापकार के निर्देशानुसार पदान्तवर्ती तकार को पररूप होता है । अतः यदि पर में ल् वर्ण होगा तो तू को भी लू आदेश हो जाएगा । फलतः 'तल्लुनाति' आदि प्रयोग निष्पन्न होंगे ।
२१२
पाणिनीय व्याकरण के अनुसार चवर्ग के परवर्ती होने पर पूर्ववर्ती तू को च् आदेश (स्तो: श्चुना श्चुः ८ । ४ । ४०), टवर्ग के परवर्ती होने पर तू को टू आदेश (ष्टुना ष्टुः ८/४/४१) तथा लकार के परवर्ती होने पर लकारादेश प्रवृत्त होता है (तोर्लि ८।४।६०) ।
इस प्रकार पाणिनीय निर्देश में तीन सूत्रों के होने से शब्दगौरव स्पष्ट है | परन्तु इन शब्दों की साधुत्वप्रक्रिया के परिमाण में समानता इसलिए कही जा सकती है कि कलापकार के अनुसार 'तच्छादयति, तज्झासयति' इत्यादि प्रयोगों में तकार के स्थान में छकारादेश (पररूप) करने के बाद “ पदान्ते घुटां प्रथमः " (३/८/१ ) सूत्र से छू से छू के स्थान में च् आदेश भी करना पड़ता है और पाणिनीय प्रक्रिया के अनुसार 'तज्जयति, तड्डीनम्' इत्यादि स्थलों में त् के स्थान में " झलां जशोऽन्ते" (८|२| ३९) से द् आदेश करने के बाद ही श्चुत्व या ष्टुत्व होगा ( स्तोः श्चुना चुः ८|४|४०, टुना ष्टुः ८ | ४ | ४१ ) ।