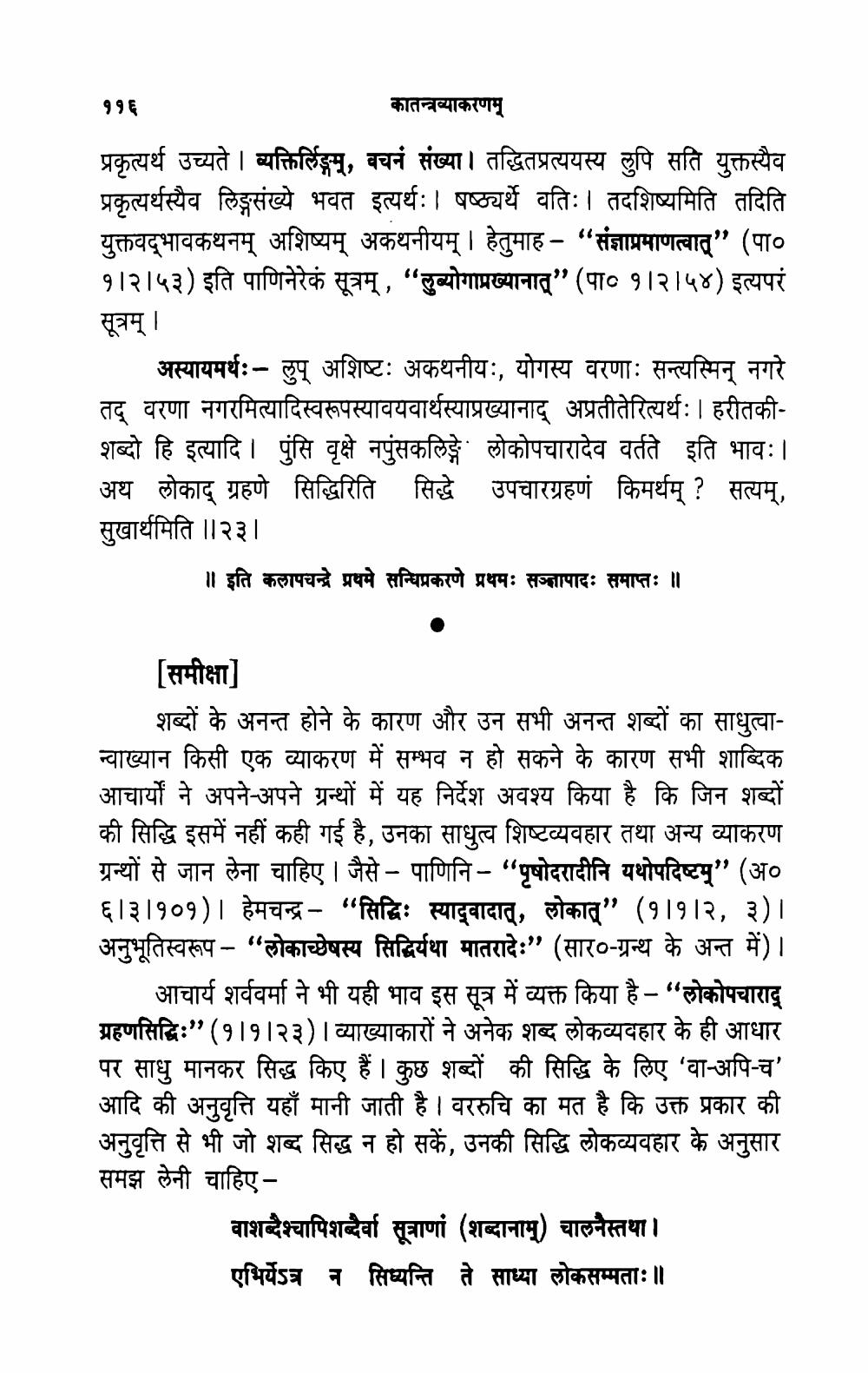________________
११६
कातन्त्रव्याकरणम् प्रकृत्यर्थ उच्यते । व्यक्तिर्लिङ्गम्, वचनं संख्या। तद्धितप्रत्ययस्य लुपि सति युक्तस्यैव प्रकृत्यर्थस्यैव लिङ्गसंख्ये भवत इत्यर्थः । षष्ठ्यर्थे वतिः। तदशिष्यमिति तदिति युक्तवद्भावकथनम् अशिष्यम् अकथनीयम् | हेतुमाह - "संज्ञाप्रमाणत्वात्" (पा० १।२।५३) इति पाणिनेरेकं सूत्रम् , "लुब्योगाप्रख्यानात्" (पा० १।२।५४) इत्यपरं सूत्रम् ।
अस्यायमर्थः- लुप् अशिष्टः अकथनीयः, योगस्य वरणाः सन्त्यस्मिन् नगरे तद् वरणा नगरमित्यादिस्वरूपस्यावयवार्थस्याप्रख्यानाद् अप्रतीतेरित्यर्थः । हरीतकीशब्दो हि इत्यादि । पुंसि वृक्षे नपुंसकलिङ्गे लोकोपचारादेव वर्तते इति भावः । अथ लोकाद् ग्रहणे सिद्धिरिति सिद्धे उपचारग्रहणं किमर्थम् ? सत्यम्, सुखार्थमिति ।।२३।
॥ इति कलापचन्द्रे प्रथमे सन्धिप्रकरणे प्रथमः सजापादः समाप्तः ॥
[समीक्षा]
शब्दों के अनन्त होने के कारण और उन सभी अनन्त शब्दों का साधुत्वान्वाख्यान किसी एक व्याकरण में सम्भव न हो सकने के कारण सभी शाब्दिक आचार्यों ने अपने-अपने ग्रन्थों में यह निर्देश अवश्य किया है कि जिन शब्दों की सिद्धि इसमें नहीं कही गई है, उनका साधुत्व शिष्टव्यवहार तथा अन्य व्याकरण ग्रन्थों से जान लेना चाहिए | जैसे - पाणिनि- "पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्" (अ० ६।३।१०१)। हेमचन्द्र- "सिद्धिः स्यादवादात, लोकात" (१1१।२, ३)। अनुभूतिस्वरूप - "लोकाच्छेषस्य सिद्धिर्यथा मातरादेः" (सार०-ग्रन्थ के अन्त में)।
आचार्य शर्ववर्मा ने भी यही भाव इस सूत्र में व्यक्त किया है - "लोकोपचाराद् ग्रहणसिद्धिः" (१1१।२३) । व्याख्याकारों ने अनेक शब्द लोकव्यवहार के ही आधार पर साधु मानकर सिद्ध किए हैं | कुछ शब्दों की सिद्धि के लिए 'वा-अपि-च' आदि की अनुवृत्ति यहाँ मानी जाती है । वररुचि का मत है कि उक्त प्रकार की अनुवृत्ति से भी जो शब्द सिद्ध न हो सकें, उनकी सिद्धि लोकव्यवहार के अनुसार समझ लेनी चाहिए
वाशब्देश्चापिशब्दैर्वा सूत्राणां (शब्दानाम्) चालनैस्तथा। एभिर्येऽत्र न सिध्यन्ति ते साध्या लोकसम्मताः॥