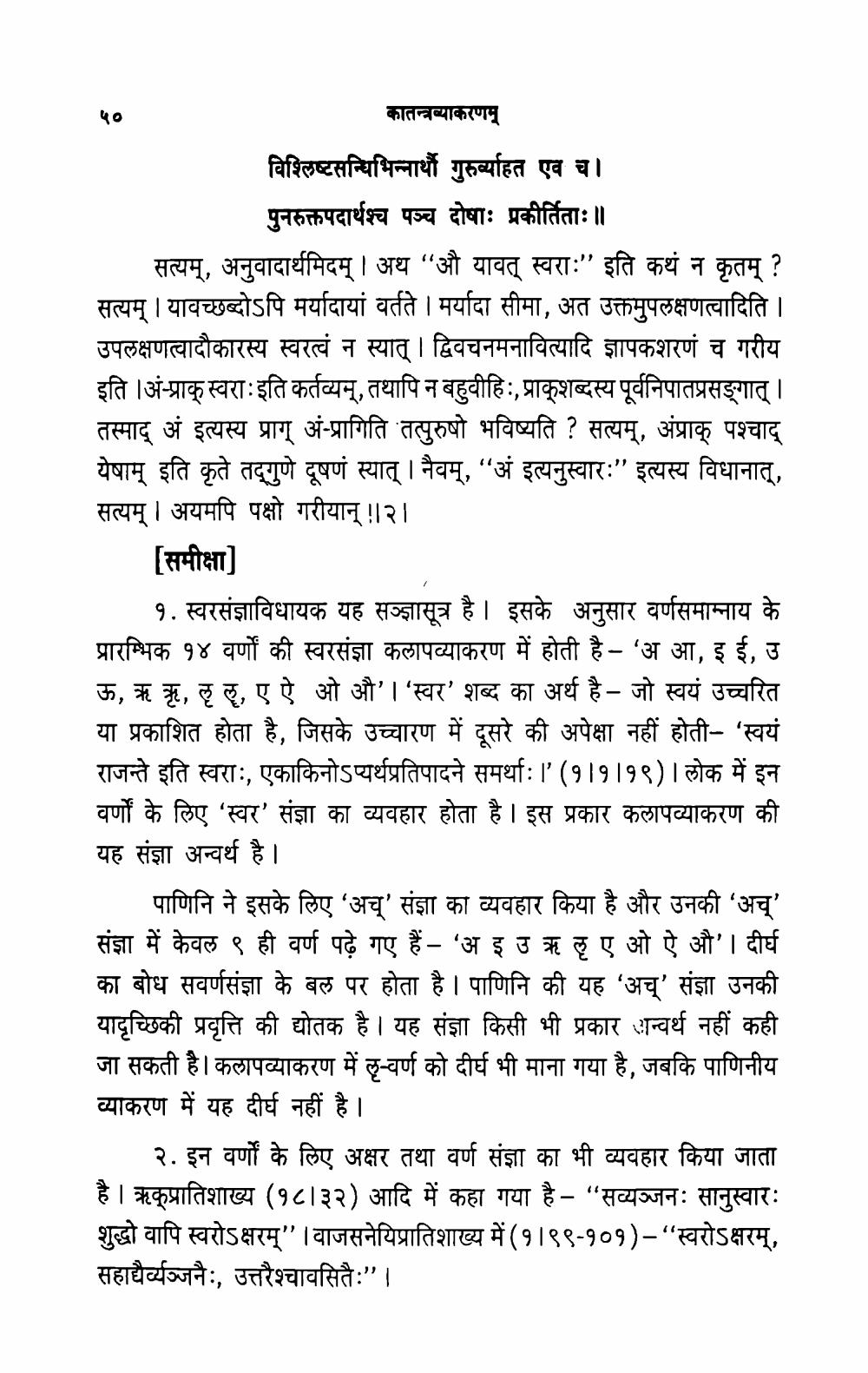________________
कातन्त्रव्याकरणम् विश्लिष्टसन्धिभिन्नार्थों गुरुाहत एव च।
पुनरुक्तपदार्थश्च पञ्च दोषाः प्रकीर्तिताः॥ सत्यम्, अनुवादार्थमिदम् । अथ "औ यावत् स्वराः' इति कथं न कृतम् ? सत्यम् । यावच्छब्दोऽपि मर्यादायां वर्तते । मर्यादा सीमा, अत उक्तमुपलक्षणत्वादिति । उपलक्षणत्वादौकारस्य स्वरत्वं न स्यात् । द्विवचनमनावित्यादि ज्ञापकशरणं च गरीय इति ।अं-प्राक् स्वराः इति कर्तव्यम्, तथापि न बहुवीहिः, प्राक्शब्दस्य पूर्वनिपातप्रसङ्गात् । तस्माद् अं इत्यस्य प्राग् अं-प्रागिति तत्पुरुषो भविष्यति ? सत्यम्, अंप्राक् पश्चाद् येषाम् इति कृते तद्गुणे दूषणं स्यात् । नैवम्, “अं इत्यनुस्वारः" इत्यस्य विधानात्, सत्यम् । अयमपि पक्षो गरीयान् !।२।
[समीक्षा]
१. स्वरसंज्ञाविधायक यह सञ्ज्ञासूत्र है। इसके अनुसार वर्णसमाम्नाय के प्रारम्भिक १४ वर्गों की स्वरसंज्ञा कलापव्याकरण में होती है - 'अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ ऋ, लू लू, ए ऐ ओ औ' । 'स्वर' शब्द का अर्थ है - जो स्वयं उच्चरित या प्रकाशित होता है, जिसके उच्चारण में दूसरे की अपेक्षा नहीं होती- 'स्वयं राजन्ते इति स्वराः, एकाकिनोऽप्यर्थप्रतिपादने समर्थाः ।' (१।१।१९)। लोक में इन वर्गों के लिए 'स्वर' संज्ञा का व्यवहार होता है । इस प्रकार कलापव्याकरण की यह संज्ञा अन्वर्थ है।
पाणिनि ने इसके लिए 'अच्' संज्ञा का व्यवहार किया है और उनकी 'अच्’ संज्ञा में केवल ९ ही वर्ण पढ़े गए हैं - 'अ इ उ ऋ लु ए ओ ऐ औ' । दीर्घ का बोध सवर्णसंज्ञा के बल पर होता है । पाणिनि की यह 'अच्' संज्ञा उनकी यादृच्छिकी प्रवृत्ति की द्योतक है । यह संज्ञा किसी भी प्रकार अन्वर्थ नहीं कही जा सकती है। कलापव्याकरण में लु-वर्ण को दीर्घ भी माना गया है, जबकि पाणिनीय व्याकरण में यह दीर्घ नहीं है।
२. इन वर्गों के लिए अक्षर तथा वर्ण संज्ञा का भी व्यवहार किया जाता है | ऋप्रातिशाख्य (१८।३२) आदि में कहा गया है - "सव्यञ्जनः सानुस्वारः शुद्धो वापि स्वरोऽक्षरम्" । वाजसनेयिप्रातिशाख्य में (१९९-१०१)- "स्वरोऽक्षरम्, सहाद्यैर्व्यञ्जनैः, उत्तरैश्चावसितैः” |