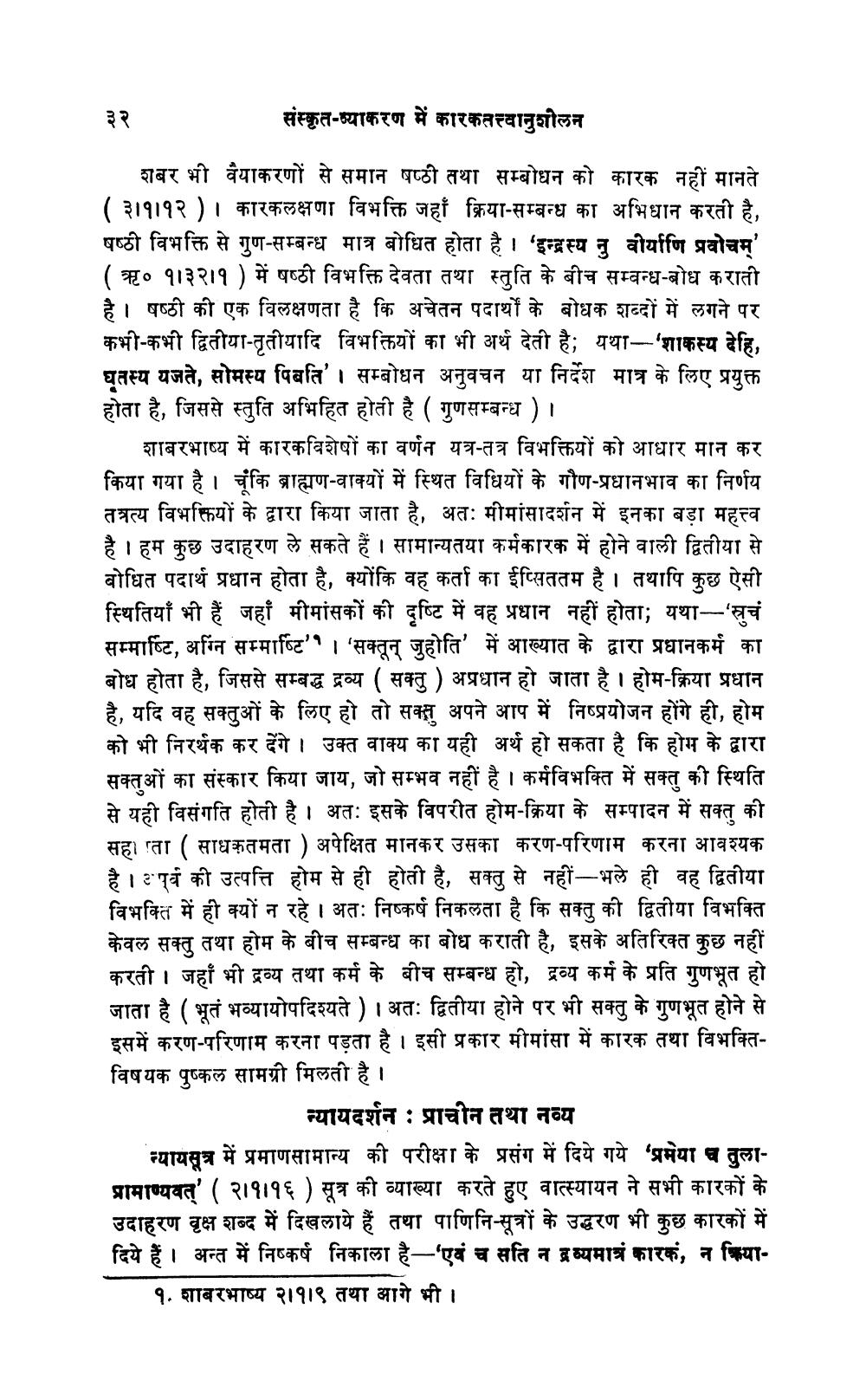________________
संस्कृत - व्याकरण में कारकतत्वानुशीलन
शबर भी वैयाकरणों से समान षष्ठी तथा सम्बोधन को कारक नहीं मानते ( ३।१।१२ ) । कारक लक्षणा विभक्ति जहाँ क्रिया-सम्बन्ध का अभिधान करती है, षष्ठी विभक्ति से गुण-सम्बन्ध मात्र बोधित होता है । 'इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्' ( ऋ० १।३२1१ ) में षष्ठी विभक्ति देवता तथा स्तुति के बीच सम्बन्ध-बोध कराती है । षष्ठी की एक विलक्षणता है कि अचेतन पदार्थों के बोधक शब्दों में लगने पर कभी-कभी द्वितीया तृतीयादि विभक्तियों का भी अर्थ देती है; यथा - 'शाकस्य देहि, घृतस्य यजते, सोमस्य पिबति' । सम्बोधन अनुवचन या निर्देश मात्र के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे स्तुति अभिहित होती है ( गुणसम्बन्ध ) |
३२
शाबरभाष्य में कारकविशेषों का वर्णन यत्र-तत्र विभक्तियों को आधार मान कर किया गया है । चूंकि ब्राह्मण वाक्यों में स्थित विधियों के गौण-प्रधानभाव का निर्णय तत्रत्य विभक्तियों के द्वारा किया जाता है, अतः मीमांसादर्शन में इनका बड़ा महत्त्व है । हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं । सामान्यतया कर्मकारक में होने वाली द्वितीया से बोधित पदार्थ प्रधान होता है, क्योंकि वह कर्ता का ईप्सिततम है । तथापि कुछ ऐसी स्थितियाँ भी हैं जहाँ मीमांसकों की दृष्टि में वह प्रधान नहीं होता; यथा - ' स्रुचं सम्माष्टि, अग्नि सम्माष्टि'" । 'सक्तून् जुहोति' में आख्यात के द्वारा प्रधानकर्म का बोध होता है, जिससे सम्बद्ध द्रव्य ( सक्तु ) अप्रधान हो जाता है । होम - क्रिया प्रधान है, यदि वह सक्तुओं के लिए हो तो सक्तु अपने आप में निष्प्रयोजन होंगे ही, होम को भी निरर्थक कर देंगे । उक्त वाक्य का यही अर्थ हो सकता है कि होम के द्वारा सक्तुओं का संस्कार किया जाय, जो सम्भव नहीं है । कर्मविभक्ति में सक्तु की स्थिति से यही विसंगति होती है । अतः इसके विपरीत होम क्रिया के सम्पादन में सक्तु की हा ( साधक मता ) अपेक्षित मानकर उसका करण परिणाम करना आवश्यक है । अपूर्व की उत्पत्ति होम से ही होती है, सक्तु से नहीं - भले ही वह द्वितीया विभक्ति में ही क्यों न रहे । अतः निष्कर्ष निकलता है कि सक्तु की द्वितीया विभक्ति केवल सक्तु तथा होम के बीच सम्बन्ध का बोध कराती है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करती । जहाँ भी द्रव्य तथा कर्म के बीच सम्बन्ध हो, द्रव्य कर्म के प्रति गुणभूत हो जाता है (भूतं भव्यायोपदिश्यते ) । अतः द्वितीया होने पर भी सक्तु के गुणभूत होने से इसमें करण - परिणाम करना पड़ता है। इसी प्रकार मीमांसा में कारक तथा विभक्तिविषयक पुष्कल सामग्री मिलती है ।
न्यायदर्शन: प्राचीन तथा नव्य
न्यायसूत्र में प्रमाणसामान्य की परीक्षा के प्रसंग में दिये गये 'प्रमेया च तुलाप्रामाण्यवत्' ( २।१।१६ ) सूत्र की व्याख्या करते हुए वात्स्यायन ने सभी कारकों के उदाहरण वृक्ष शब्द में दिखलाये हैं तथा पाणिनि-सूत्रों के उद्धरण भी कुछ कारकों में दिये हैं । अन्त में निष्कर्ष निकाला है - 'एवं च सति न द्रव्यमात्रं कारकं, न क्रिया
१. शाबर भाष्य २।१।९ तथा आगे भी ।