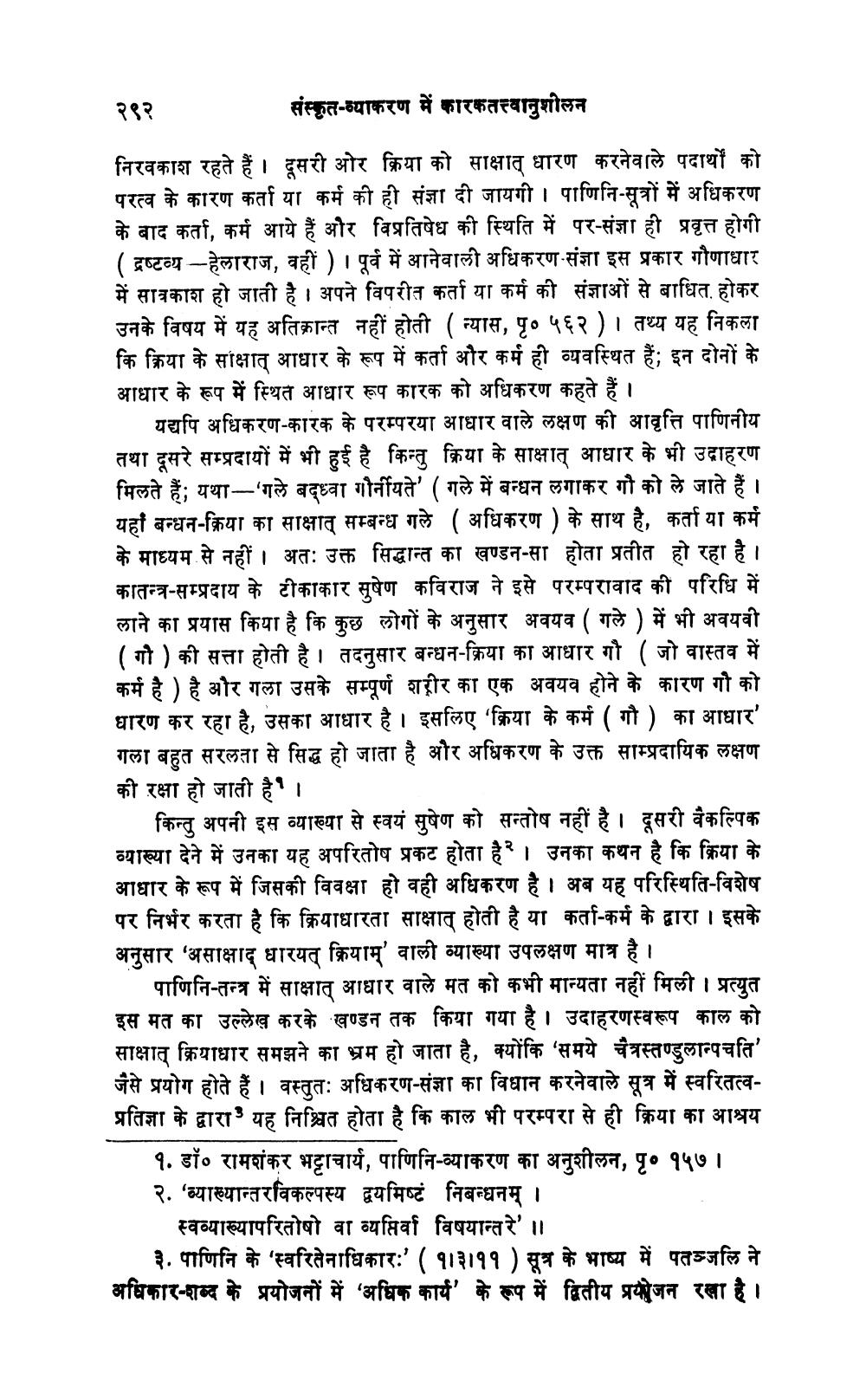________________
२९२
संस्कृत-व्याकरण में कारकतत्वानुशीलन निरवकाश रहते हैं। दूसरी ओर क्रिया को साक्षात् धारण करनेवाले पदार्थों को परत्व के कारण कर्ता या कर्म की ही संज्ञा दी जायगी। पाणिनि-सूत्रों में अधिकरण के बाद कर्ता, कर्म आये हैं और विप्रतिषेध की स्थिति में पर-संज्ञा ही प्रवृत्त होगी ( द्रष्टव्य -हेलाराज, वहीं ) । पूर्व में आनेवाली अधिकरण संज्ञा इस प्रकार गौणाधार में सावकाश हो जाती है। अपने विपरीत कर्ता या कर्म की संज्ञाओं से बाधित. होकर उनके विषय में यह अतिक्रान्त नहीं होती (न्यास, पृ० ५६२ )। तथ्य यह निकला कि क्रिया के साक्षात् आधार के रूप में कर्ता और कर्म ही व्यवस्थित हैं; इन दोनों के आधार के रूप में स्थित आधार रूप कारक को अधिकरण कहते हैं ।
यद्यपि अधिकरण-कारक के परम्परया आधार वाले लक्षण की आवृत्ति पाणिनीय तथा दूसरे सम्प्रदायों में भी हुई है किन्तु क्रिया के साक्षात् आधार के भी उदाहरण मिलते हैं; यथा- 'गले बद्ध्वा गोर्नीयते' ( गले में बन्धन लगाकर गौ को ले जाते हैं । यहां बन्धन-क्रिया का साक्षात् सम्बन्ध गले ( अधिकरण ) के साथ है, कर्ता या कर्म के माध्यम से नहीं। अतः उक्त सिद्धान्त का खण्डन-सा होता प्रतीत हो रहा है। कातन्त्र-सम्प्रदाय के टीकाकार सुषेण कविराज ने इसे परम्परावाद की परिधि में लाने का प्रयास किया है कि कुछ लोगों के अनुसार अवयव ( गले ) में भी अवयवी ( गो ) की सत्ता होती है। तदनुसार बन्धन-क्रिया का आधार गौ ( जो वास्तव में कर्म है ) है और गला उसके सम्पूर्ण शरीर का एक अवयव होने के कारण गौ को धारण कर रहा है, उसका आधार है। इसलिए 'क्रिया के कर्म (गौ ) का आधार' गला बहुत सरलता से सिद्ध हो जाता है और अधिकरण के उक्त साम्प्रदायिक लक्षण की रक्षा हो जाती है।
किन्तु अपनी इस व्याख्या से स्वयं सुषेण को सन्तोष नहीं है। दूसरी वैकल्पिक व्याख्या देने में उनका यह अपरितोष प्रकट होता है। उनका कथन है कि क्रिया के आधार के रूप में जिसकी विवक्षा हो वही अधिकरण है । अब यह परिस्थिति-विशेष पर निर्भर करता है कि क्रियाधारता साक्षात् होती है या कर्ता-कर्म के द्वारा। इसके अनुसार 'असाक्षाद् धारयत् क्रियाम्' वाली व्याख्या उपलक्षण मात्र है।
पाणिनि-तन्त्र में साक्षात् आधार वाले मत को कभी मान्यता नहीं मिली। प्रत्युत इस मत का उल्लेख करके खण्डन तक किया गया है। उदाहरणस्वरूप काल को साक्षात् क्रियाधार समझने का भ्रम हो जाता है, क्योंकि 'समये चैत्रस्तण्डुलान्पचति' जैसे प्रयोग होते हैं। वस्तुतः अधिकरण-संज्ञा का विधान करनेवाले सूत्र में स्वरितत्वप्रतिज्ञा के द्वारा यह निश्चित होता है कि काल भी परम्परा से ही क्रिया का आश्रय
१. डॉ० रामशंकर भट्टाचार्य, पाणिनि-व्याकरण का अनुशीलन, पृ० १५७ । २. 'व्याख्यान्तरविकल्पस्य द्वयमिष्टं निबन्धनम् ।
स्वव्याख्यापरितोषो वा व्यप्तिर्वा विषयान्तरे' । ३. पाणिनि के 'स्वरितेनाधिकारः' ( १३३११ ) सूत्र के भाष्य में पतञ्जलि ने अधिकार-शब्द के प्रयोजनों में 'अधिक कार्य' के रूप में द्वितीय प्रयोजन रखा है।